दिए को मशाल बनाओगे, या बुझा ही दोगे?

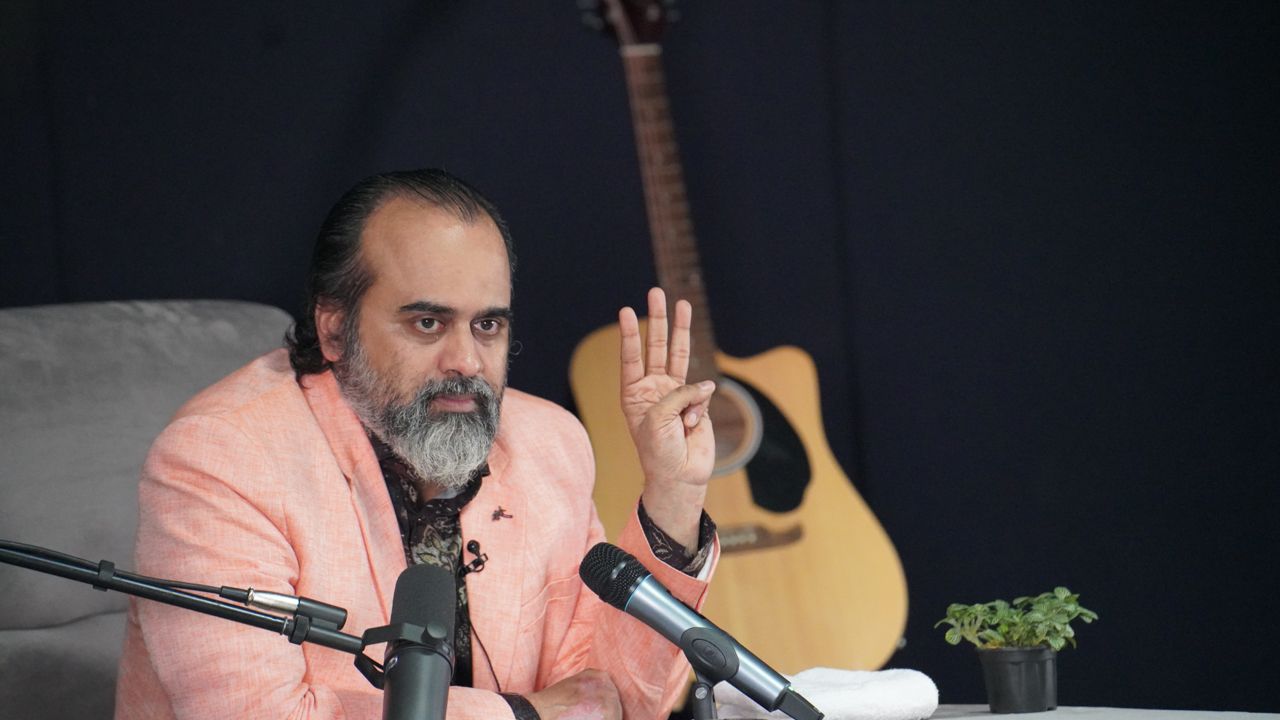
प्रश्नकर्ता: आचार्य जी जब मैं आध्यात्मिकता के बारे में किसी और से बात कर रहा होता हूँ तो एक शानदार ऊर्जा शब्दों के माध्यम से बह रही होती है। मैं दो घण्टे लगातार बिना सोचे-समझे बोल रहा होता हूँ। लेकिन जब मैं खुद को प्रतिबिम्बित करता हूँ उन्हीं शब्दों पर, तो मुझे ईमानदारी नहीं मिलती है। तो क्या मुझे बोलना बन्द कर देना चाहिए? क्योंकि एक अपराध-बोध सामने आता है। कृपया मार्गदर्शन करें।
आचार्य प्रशांत: बिलकुल, ये नहीं कहा कि “आचार्य जी, ये बताइए कि जो बोल रहा हूँ उस पर जियूँ कैसे?” वाह-री माया! तत्काल एक अनूठा विकल्प खड़ा करा अपने लिए कि “आचार्य जी, जो मैं बोलता हूँ उस पर जी तो पा नहीं रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ, बोलना ही बंद कर देता हूँ।”
और ऐसा तर्क आचार्य जी ने अब इतना सुना है - “आचार्य जी, सत्रों में आता हूँ, आप जो बात बताते हैं बिलकुल ठीक लगती हैं पर बाहर उसका पालन तो मैं करता नहीं, तो मैं सत्रों में आना ही बंद कर देता हूँ।”
"बेटा आप पिछले चार सत्रों में क्यों नहीं आए?" “जी! क्योंकि मैं उसके पिछले चार सत्रों में भी नहीं आया था।” "आप पिछले चार सत्रों में क्यों नहीं आए?" “क्योंकि मैं उसके पिछले चार सत्रों में भी नहीं आया था, तो मुझे इतनी शर्म आई कि मैं अगले चार सत्रों में भी नहीं आया।” क्या तर्क है!
व्यर्थ ही कहते हो “वारी जाऊँ मैं सद्गुरु के”, वारी तो तुम अपनी ‘बुद्धि’ के जाओ! कहाँ-कहाँ से चुनकर युक्तियाँ उछालते हो। आज नहाए क्यों नहीं? “क्योंकि कल भी नहीं नहाया था। तो बड़ी लाज लगी, इसलिए आज भी नहीं नहाया।” क्या बात है! दौड़ क्यों नहीं रहे? “क्योंकि मैं बहुत धीरे-धीरे चलता हूँ न, तो चलूँ ही क्यों?”
जीवन की अँधेरी गुफा में दिया जला है। अभी दिया मात्र है, और तुम्हारी गुफा गहन है, अँधेरी है, गहरी है, सीलन से भरी हुई है, बहुत पुरानी। तुम्हारे दिये में अभी वो शक्ति नहीं कि पूरी गुफा को ही अनुप्राणित कर दे। ज़रा सा दिये से दूर जाते हो तो पाते हो कि अँधेरा है, और सघन है, तो क्या करोगे? कहोगे कि “अरे! ऐसे दिये का फायदा ही क्या जो पूरी गुफा को ही प्रकाशित नहीं कर सकता, मैं इस दिये को ही बुझाये देता हूँ”? ये करोगे या मेहनत करोगे, युक्ति करोगे और दिये को मशाल बनाओगे? बोलो!
प्र: मशाल बनाएँगे।
आचार्य: पर क्या खूब तर्क उठते हैं! “इतना सा दिया है, सुरक्षा बहुत करनी पड़ती है, जान इसमें है नहीं और गुफा भयावह, काली-घनेरी! कौन दिये का पक्ष ले, अँधेरे से वैसे भी अपनी पुरानी यारी है। जीतते का साथ दो, अँधेरा ही जीतता दिख रहा है, उसी का साथ दे लो।"
और ये तो तयशुदा बात है कि जीतेगा तो वही जिसका साथ तुम दोगे। तुम दे लो अँधेरे का साथ, अँधेरा निश्चित जीतेगा। फिर तर्क भी मत दो कि मैंने इस वजह से अँधेरे का साथ दिया इत्यादि, इत्यादि। सीधे कह दो, हमें अँधेरा पसंद है।
हमारी हालत ऐसी है जैसे कोई मोटा आदमी, उससे कोई पूछे कि “ट्रेडमिल क्यों नहीं करते?" तो बोले, “मोटा हूँ न इसलिए।" और कोई दूसरा भी हो सकता है जिससे पूछा जाए कि “ट्रेडमिल क्यों कर रहे हो?” तो वो बोले “मोटा हूँ, इसलिए।”
तुम बता दो, तुम्हारा तर्क क्या है?
आचार्य जी से छुपते क्यों फिरते हो? “दिल में चोर है न इसलिए।” बार-बार आचार्य जी के सामने क्यों आते हो? “दिल में चोर है, इसलिए।” दोनों ही बातें कही जा सकती हैं, तुम बताओ, तुम्हारी बात क्या है?
जीतना चाहते हो अगर जिंदगी में, तो दूसरी बात पकड़ लो।
अँधेरा जितना तुम पर छाए, तुम उतना ज़्यादा दिये का पक्ष लो। भीतर का चोर जितना प्रबल होता जाए, तुम गुरु के उतने निकट आते जाओ।
तुम बिलकुल उल्टा करते हो। जब लगता है कि तुम ज़रा पाक-साफ़ हो उस समय तुम गुरु के सामने खड़े हो जाते हो; ये अहंकार की बात है। तुम गुरु से भी स्पर्धा कर रहे हो। तुम कह रहे हो, "मैं गुरु के सामने आऊँगा ही तब, जब ज़रा पाक-साफ़, नेक हूँ। उस समय गुरु मुझे डाँट ही नहीं पाएगा, उसका हक़ ही नहीं होगा डाँटने का। मैं कहूँगा 'देखो अभी तो मैं बिलकुल ठीक हूँ, अभी मुझे डाँटो मत।' और जब मुझे पता होगा कि मैंने चोरी करी है, दिल में खोट है, पाप है, अभी-अभी कीचड़ में नहा कर आया हूँ, तो गुरु के सामने आऊँगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि तब गुरु के सामने आया, तो गुरु को फिर अधिकार मिलेगा मुझे डाँट बताने का, कान खींचने का। और साहब हम ऐसे हैं कि हम पसंद नहीं करते कि कोई हमें डाँट बताए और हमारे कान खींचे।" तो गुरु के सामने भी हम सिर्फ़ तब आते हैं जब हमने कुछ तमगे हाँसिल किए होते हैं।
तुम्हारी हालत उस मरीज़ जैसी है जो डॉक्टर के सामने जाता ही तब है जब स्वस्थ हो। और ये सबका हाल है। तुम प्रकाश से ठीक तब दूर भागते हो जब अँधेरे ने तुम्हें बुरी तरह जकड़ रखा होता है। जब तुम्हें रोशनी के एक-एक किरण की सख़्त ज़रूरत होती है, ठीक तब तुम अपना दिया बुझा देते हो।
तुम्हारे जीवन में भले ही अभी सिर्फ़ शब्द ही उतरे हों पर कम-से-कम शब्द तो उतरे न। ये कोई छोटी बात है? तुम कह रहे हो तुम शब्दों का भी गला घोंट दोगे। कहीं से तो शुरुआत होनी थी, गुफा के किसी कोने में तो दिया रखा जाएगा। अचानक से सूर्य तो नहीं चमक जाएगा न। तुम कह रहे हो “दो-दो घण्टे बोल जाता हूँ जब दूसरों को सच्चाई बतानी होती है, पर वही सच्चाई अपनी ज़िंदगी में तो उतर नहीं रही", उस दो घण्टे तो उतरी!
आज से पन्द्रह-बीस बरस पहले जब मैंने पढ़ाना शुरु किया था, तो किसी ने पूछा मुझसे कि “सबकुछ छोड़-छाड़ कर पढ़ाना क्यों चाहते हो?” मैंने कहा, “सीखने का ये बड़ा अच्छा तरीका है।”
उस दो घण्टे जब तुम सच का नाम ले रहे होते हो तो दूसरा ही नहीं सुन रहा होता है तुम्हें, तुम भी तो स्वयं को सुन रहे होते हो न। स्वयं को सुन रहे होते हो, तुम्हें भी ये एहसास होता है, तुम्हें भी ये निश्चित होता है कि आत्मा है।
जो कोई सच बोल रहा है उसे भलीभाँति पता होता है की उस वक़्त वो विलुप्त हो जाता है, कोई और ही बोल रहा होता है उसके भीतर से।
कोई दूसरा तुम्हें आत्मा का प्रमाण देगा, तुम कैसे संतुष्ट हो जाओगे?
सत्य है उसका प्रमाण ही तभी मिलता है जब वो तुमसे प्रस्फुटित होता है।
स्वयं तुम्हारी हस्ती से उद्भाषित न हो सत्य, तो तुम्हें कभी भी पक्की आश्वस्ति होगी कैसे? जब तुम भौंचक्के रह जाते हो न कि “अरे! अभी मैंने ये क्या कह दिया? ये बात मुझे कहाँ से पता चल गई?” तब जानना कि तुम्हारा परिचय दूसरे ‘मैं’ से हो रहा है। तुम अभी तक सिर्फ एक ‘मैं’ की आवाज़ सुनते थे। एक ही ‘मैं’ की आवाज़ पहचानते थे।
वो दूसरा बोल उठा! और अब तुम हक्के-बक्के रह गए हो, "ये कौन बोल रहा है?"
ये मेरे साथ होता था। कॉलेज में मैं एक चुनाव में खड़ा हुआ था और एक जगह अपनी बात कहनी थी, भाषण देना था। सामने जो थे वो करीब-करीब दंगाई बने बैठे थे, वो सब मुझसे एक-एक दो-दो साल सीनियर, उन्होंने तय कर रखा था कि इसको बोलने नहीं देना है और जो भी बात बोले उसको काट देना है, शोर मचा देना है। और मेरे कॉलेज में चुनावों का ये तक इतिहास था कि जूते-चप्पल भी चल जाते थे। और मेरे लिए ये पहला मौका था, किसी चुनाव में खड़े होना, किसी भीड़ को सम्बोधित करना इत्यादि। अच्छी भरी भीड़ थी। जितना बड़ा ये कक्ष है इससे दूना बड़ा। और तब मैं कुर्ता इत्यादि कम ही पहनता था, जैसे आम लड़के होते है, मैं भी टी-शर्ट या शर्ट में रहता था। उस दिन मैंने कुर्ता पहना, और जिन लोगों ने मुझे देखा बाहर से, उन्होंने मुझसे बार-बार कहा कि “तुम बोलते जा रहे थे और ये तुम्हारे भाव थे (कुर्ते की बाँहें चढ़ाते हुए)।” बोले, “ऐसा तुम्हें पहले कभी करते नहीं देखा।” मैंने कहा, “मैंने भी आज अपने-आपको जैसा सुना, ऐसा पहले कभी नहीं सुना, मुझे खुद नहीं पता था कि ‘मैं’ बोल रहा हूँ।” और फिर मैं बाहर आया, और दोस्त था मेरा, उससे मैंने कहा “जब मैं सच बोलता हूँ, मुझे डर नहीं लगता।”
बात बहुत छोटी सी थी, बचपन से सबको सिखाई जाती है। सच बोलने में डरना मत, इत्यादि, इत्यादि। पर वही अनुभव जब स्वयं को होता है तो बात जम जाती है, पक्की हो जाती है कि;
जहाँ सच है वहाँ डर नहीं होता।
और वो दिन है, आज का दिन है, मैं सच बोलता हूँ मुझे डर नहीं लगता।
और ये बात तुम नहीं समझ पाओगे, कोई दूसरा चाहे लाख बार तुम्हारे सामने दोहराए। ये बात तुम्हें समझ में ही सिर्फ तब आएगी, जब तुम सच बोलोगे, और पाओगे “अरे! डर तो लग ही नहीं रहा। जिसके सामने बोल रहा हूँ वो बुरा मान सकता है, हानि पहुँचा सकता है, कुछ भी अंजाम हो सकता है, डर नहीं लग रहा।"
तुम कह रहे हो दो घण्टे के लिए ही बोल पाते हो, दो घण्टे तो बोलो न! दो घण्टे बहुत होते हैं। दो घण्टे अगर तुम सच्चे रह पाए तो वो दो घण्टे तुम्हारे प्रबल ध्यान के थे।
मेडिटेशन-मेडिटेशन (ध्यान) करते घूमते हो, बेख़ौफ़ होकर सच्चाई बयान करने से बड़ा मेडिटेशन कौन सा होता है?



