
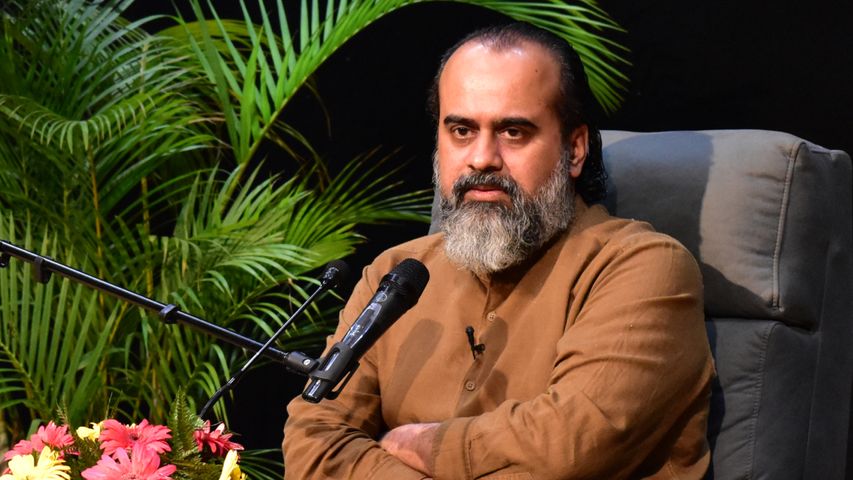
स्वात्मा हि प्रतिपादितः ~अवधूत गीता
आचार्य प्रशांत: यह सब जो दिखाई दे रहा है, यह एक ही है, जो 'मैं' हूँ।
आत्म माने ‘मैं’। इसका और मेरा तत्व एक है, अलग-अलग नहीं है।
प्रश्नकर्ता: यहाँ ‘स्व’ का प्रयोग क्यों है?
आचार्य: ‘स्व’ माने मेरा। जब ‘आत्मा’ कहा जाता है, तो कोई तो है न जो आत्मा की बात कर रहा है। अगर मात्र आत्मा है, तो उसमें ‘आत्मा’ शब्द का कोई ख़ास अर्थ ही नहीं रह जाता। ‘आत्मा’ माने ‘मैं’। अगर मात्र ‘मैं’ है, तो वो क्यों कहे ‘मैं’? किससे कहे, कैसे कहे? ‘स्व-आत्मा’ कहते ही कोई बन जाता है जो इस आत्मा पर दावा करता है।
‘प्रतिपादितः’ मतलब जो ये अलग-अलग दिखाई दे रहा है चारों तरफ़, जो प्रतिपादित है, जो विस्तीर्ण। ‘स्व’ माने ‘मैं, जो इस से अलग हूँ’। ‘अहंकार’ क्या हुआ? वो जो अपने आप को संसार से भी अलग माने, और आत्मा से भी अलग माने। वो दो-तरफा भेद में जीता है। ‘अहंकार’ माने हम, हम जैसे हैं, हम दो-तरफा अंतर, भेद करते हैं। “मैं कौन हूँ? मैं वो दरवाज़ा नहीं हूँ, ये ज़मीन नहीं हूँ, मैं मेरा पड़ोसी नहीं हूँ, मैं संसार तो नहीं हूँ।" हद-से-हद मैं ये कह देता हूँ कि, “मैं संसार में हूँ”, पर मैं ‘संसार’ तो नहीं हूँ।
दूसरी ओर अहंकार अपने आप को आत्मा से भी अलग करके देखता है। अहंकार अपने आप को जितनी उपाधियाँ देता है, वो आत्मा पर लागू ही नहीं होतीं। तो वो आत्मा से भी अपने आपको भिन्न देखता है। तो जब तुम कहते हो, “स्वात्मा हि प्रतिपादितः”, तो ‘स्वात्मा’ माने – अहंकार आत्मा की बात कर रहा है, ‘स्व’। और कह रहा है कि, “ये जो आत्मा है, यही संसार है।” अभी तक वो क्या कह रहा था? “संसार अलग, मैं अलग, और आत्मा अलग।” अब उसको दिखाई दे रहा है, “मैं, ये संसार, और आत्मा तीनों एक हैं। सब जो है, मेरा ही विस्तार है, मैं ही हूँ।”
किस अर्थ में ये सब ‘मेरा’ ही विस्तार है? दुनिया के होने का जो आधार है, कि वो दिखाई देती है, सुनाई पड़ती है, वही मेरे होने का आधार है। इस कमरे में बिस्कुट दिखाई ना पड़े, तो तुम कहोगे कि, “बिस्कुट नहीं है।” इस कमरे में गरिमा दिखाई ना पड़े, तो तुम कहोगे कि, “गरिमा नहीं है।” दोनों के होने का आधार एक ही है कि – दोनों इन्द्रियगत रूप से प्रतीत होते हैं।
तो उस तल पर संसार और तुम एक हो, और दूसरे भी तल पर तुम और संसार एक हो। दूसरा ताल क्या हुआ? कि इन्द्रियाँ ना रहें, तो संसार और तुम दोनों शून्य हो जाते हो, जैसा कि गहरे ध्यान में होता है। संसार तो हटता-ही-हटता है, उस समय तुम्हें अपनी भी सुध नहीं रह जाती। लेकिन ‘तुम’ होते हो, उसी ‘होने’ को ‘आत्मा’ कहते हैं।
अब ये ‘आत्मा’ ऐसी चीज़ नहीं है जो बाकी सब के हटने पर आ जाती है। जब कहा जाता है, “स्वात्मा हि प्रतिपादितः” का अर्थ यह होता है कि – ये ‘आत्मा’ वो तत्व है, जिसका विस्तार ‘अहंकार’ और ‘संसार’ हैं। जब विस्तार सिमट जाता है, तो सिर्फ़ ये तत्व जलता रहता है, प्रकाशित होता रहता है। और जब ये विस्तार फैल जाता है, तो विस्तार ही विस्तार दिखाई देता है, तब यह तत्व आसानी से तब प्रतीत नहीं होता।
समेट लो, तो ‘आत्मा’, फैला दो, तो ‘संसार’।
और इसका प्रमाण मात्र ‘ध्यान’ है। जो ध्यान को नहीं जानते, उनको ये बात समझ नहीं आएगी। संसार के और अहंकार के ना रहने पर भी ‘तुम’ हो, ये सिर्फ़ बात नहीं है, ये एक गहरी प्रतीति होती है। और वो अनुभव करके ही जानी जा सकती है। तो इसलिए जो लोग ध्यान को नहीं जानते, उनको ये बात ज़रा भी समझ में ना आएगी कि – “संसार भी ना रहे, मैं ना रहूँ, फिर भी मैं बचा कैसे रह गया?” उसके लिए तो ‘ध्यान’ का ही प्रमाण चलेगा। इसीलिए आप में से कई लोगों की शक्ल अभी उड़ी-उड़ी लग रही है कि, “ये क्या बात है, कुछ ना रहे, तब भी मैं रहूँगा?”
आख़िर में आकर यहीं पर अटकोगे न, क्योंकि शब्द तो सारे वहीं तक ले आ देंगे। किसी भी बात पर तुम्हें यक़ीन होगा कैसे, अगर आख़िरी प्रमाण तुम्हारे भीतर से नहीं उठ रहा। आख़िरी बात पर तो एक अंदरूनी ‘हाँ’ निकले, तो ही बात बनती है। तो अंदरूनी ‘हाँ’ निकलती नहीं, क्योंकि उस चीज़ को कभी चखा नहीं, उस चीज़ को तुम चख सकते नहीं, क्योंकि डर बहुत लगता है।
प्र२: पहले मैं चालीस-पचास मिनट ध्यान लगाती थी, फिर पढ़ा और समझ में आया कि ऐसे चालीस-पचास मिनट बैठना भी एक ढर्रा है, और लगातार ध्यान में होना ज़रूरी है, तो मेरा ध्यान करना छूट गया। अगर बात यह यह कि निरंतर ध्यानस्थ रहना चाहिए, तो उसके लिए करना क्या चाहिए?
आचार्य: अगर उस विधि का नतीजा ये निकलता है कि आप चौबीस घण्टे ध्यान में रह पाओ, तो विधि की तरह उसमें कोई बुराई नहीं है। पर उसका नतीजा अगर ये निकलता है कि चालीस मिनट का ध्यान, और फिर तेईस घण्टे की बेहोशी, तो बहुत बुराई है।
प्र२: उस विधि से एक फ़र्क ये पड़ता था, कि गुस्सा नहीं आता था।
आचार्य: दोनों बातें हो सकती हैं। वो तो चित्त की दिशा पर निर्भर करता है। एक चित्त हो सकता है जो कहे, “दिन-भर का कोटा निपटा दिया, दिन-भर की शान्ति का कोटा निपटा दिया, अब मुझे लाइसेंस मिल गया है बाकी दिन-भर उपद्रव का”, तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो गई।
कई लोग जब जिम में व्यायाम करने जाते हैं, तो वो साथ में डाइटिंग (अल्प भोजन लेना) भी शुरू कर देते हैं। और कई जब जिम जाते हैं, तो वो कहते हैं कि, “इतनी कैलोरी जला तो रहा हूँ, तो और खा सकता हूँ अब।”
तो वो तो आपके चित्त की दिशा पर है, कि क्या तर्क उठ रहा है भीतर से। एक चित्त कह सकता है, “ध्यान बड़ा शीतल था, ये अनुभूति दिन-भर चाहिए।” और एक चित्त कह सकता है, “दिन-भर की शीतलता निपटा दी न, आओ अब ज़रा जलें।”
आमतौर पर हम ऐसे ही होते हैं, कि “निपट तो गया प्रार्थना का कोटा, अब आ जा।” देखते नहीं हो? “अभी परेशान मत करना, अभी प्रार्थना कर रहा हूँ।” अभी ये क्या हुआ है? “ये कोटा पूरा हुआ है, मेरे पाँच मिनट निकल गए, अब आ जा।”
तो ध्यान और प्रार्थना का कोटा नहीं पूरा किया जाता। ध्यान और प्रार्थना में निरंतर रहा जाता है, उसमें जिया जाता है।



