
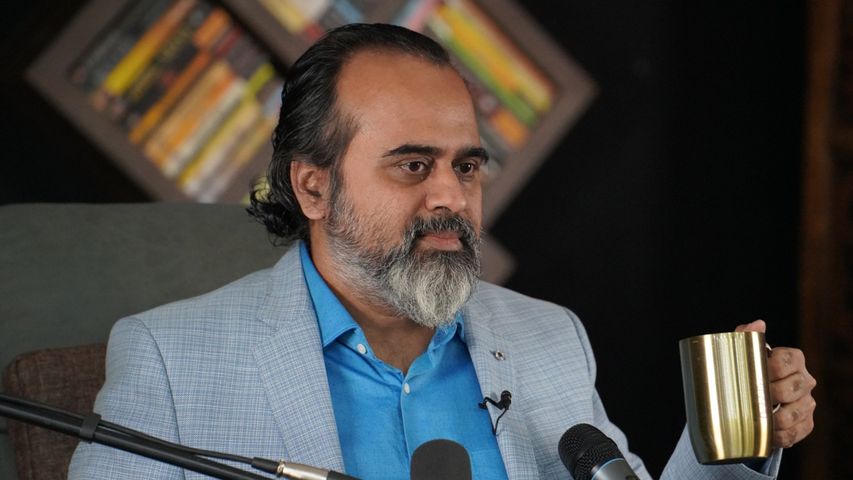
प्रश्नकर्ता: रूह और आत्मा में क्या अंतर है?
आचार्य प्रशांत: आत्मा परम सत्य है, अचल है; न जन्म लेती है, न मरती है, न आती है, न जाती है; न उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है, न कहा जा सकता है। रूह जिसको आप कहते हैं वो आदमी की कल्पना है, झूठ है, असत्य है, एक आने-जाने वाली चीज़ है। रूह और आत्मा में कोई तुलना नहीं है, कोई समानता नहीं है; और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुत लोगों को रूह और आत्मा एक ही चीज़ लगते हैं।
आत्मा का मतलब है सच्चाई। किसकी सच्चाई? आप जो बने बैठे हैं उसकी सच्चाई। और दुनिया भी चूँकि आपको ही दिखाई देती है, इसलिए जब आपकी सच्चाई की बात होगी तो उसमें दुनिया की सच्चाई भी आ गयी। दुनिया का सत्य और आपका सत्य आत्मा कहलाता है, और ये दोनों सत्य एक हैं। जगत का सत्य और आपका सत्य आत्मा कहलाता है, और वो बदलता नहीं है। चूँकि वो बदलता नहीं है क्योंकि वो कभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि शुरुआत भी एक बदलाव होती है न, और इसलिए वो कभी ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि अंत भी एक बदलाव होता है न। वो अनादि है और वो अनंत है, उसे आत्मा कहते हैं।
आत्मा किसी के शरीर में वास नहीं करती, और रूह को लेकर आपकी कल्पना है कि रूह तो शरीर में होती है और शरीर में घुस जाती है, निकल जाती है। आत्मा अनेक नहीं होती, आत्मा एक है, क्योंकि सत्य अनेक नहीं होते; और रूहें तो आपकी परिभाषा के अनुसार ही अनेक होती हैं। मैं कह रहा था कि खेद की बात है कि कुछ धार्मिक पंथ ऐसे रहे हैं जिन्होंने आत्मा को भी बिलकुल रूह के जैसा क़िस्सा बना दिया है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं कि बहुत सारी आत्माएँ होती हैं और हम सब आत्माएँ हैं। और जो–जो बातें रूहों के बारे में करी जाती हैं, वो सब बातें उन्होंने आत्मा के बारे में करनी शुरू कर दी हैं।
वास्तव में जिस तरीके से आत्मा की बात आजकल ज़्यादातर लोग करते हैं, वो आत्मा की नहीं, रूह की बात कर रहे हैं। भारतीय धार्मिक दर्शन में रूह जैसी किसी चीज़ के लिए कोई जगह ही नहीं है! रूह माने क्या? कि कोई चीज़ जो आपके भीतर रहती है तब तक जब तक आप ज़िंदा हैं, फिर जब आप मरते हैं तो रूह निकल जाती है। ऐसा कहीं नहीं है! जी हाँ, ऐसा भगवद्गीता में भी नहीं है! बहुत लोग कहते हैं, ‘पर भगवदगीता में तो श्रीकृष्ण कहते हैं कि आत्मा आती-जाती है, वगैरह-वगैरह।‘ नहीं! उन्होंने न भगवद्गीता समझी है, न कृष्ण को समझा है।
गीता अपनेआप में एक उपनिषद् कहलाती है, और औपनिषदिक दर्शन बहुत सीधा है - एक ही सत्य है जिसका नाम है आत्मा। जिसको आप परमात्मा कहते हैं, वो भी और कुछ नहीं है, आत्मा का ही एक नाम-भर है। आत्मा चूँकि परम है, इसलिए आत्मा को ही आप परमात्मा बोल देते हैं। ये वेदांत दर्शन है। और गीता वेदांत का ही ग्रंथ है, गीता वेदांत से भिन्न थोड़े ही कुछ बोल देगी भाई!
समझ में आ रही है बात?
भारत, जो आत्मा का सत्य समझता था, जो आत्मा के शिखर पर विराजमान था, उसने व्यर्थ के प्रभावों में आकर आत्मा को रूह बना डाला। और बात इतनी बिगड़ गयी है कि अब लोग आत्मा की चर्चा भी उसी तरीके से करते हैं जैसे रूह की की जाती है; कि आत्मा निकल गयी, आत्मा उड़ रही थी, आत्मा पेड़ पर बैठी थी, इसकी आत्मा निकलकर उसके शरीर में घुस गयी। ये सब बातें भारतीय या वैदिक हैं ही नहीं!
‘आत्मा’ शब्द का प्रयोग बड़े सम्मान और सावधानी से करें। आत्मा माने वो सच्चाई जो बदल नहीं सकती। आत्मा माने वो जो अनंत है, आत्मा माने वो जो अचल है। जो अचल है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाएगा! जो अनंत है वो एक छोटे-से शरीर में कैसे समा जाएगा! देखिए न, हमारे शब्दों का चयन भी कैसा हो गया है, हम कहते हैं कि भगवान फलाने की आत्मा को शांति दे। आत्मा तो सदातृप्ता है, आत्मा अशांत कैसे हो गयी कि उसे शांति दें भगवान भाई! आत्मा कहाँ से अशांत हो गयी! और लोग इस तरह से बात कर रहे होंगे, कि वो कुछ अतृप्त आत्माएँ हैं, वो फलाने पेड़ पर घूम रही थीं। आत्मा कैसे अतृप्त हो गयी!
ये सब सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि भारतीयों ने अपने धर्मग्रंथों को ही पढ़ना छोड़ दिया। अगर उपनिषद् पढ़े होते, तो इस तरह की बात नहीं कर सकते थे कि उनकी आत्मा ने उनके शरीर का त्याग कर दिया, या उनकी आत्मा अशांत होकर, अतृप्त होकर इधर-उधर भटक रही है। पर नहीं, दुनिया-भर की चीज़ें पढ़ लेंगे व्यर्थ की, बकवास, और उपनिषद् नहीं पढ़ेंगे। और कहेंगे, ‘देखिए, आपकी आत्मा और उसकी आत्मा एक-दूसरे से बड़ा प्रेम करती है,’ ‘हम सब आत्माएँ यहाँ इक्कठा हैं’ - इस तरह की बातें होंगी।
न आत्मा अतृप्त होती है, न अशांत होती है, न प्रेम करती है, न अंदर आती है, न बाहर जाती है; उसके बारे में न सोचा जा सकता है, न कहा जा सकता है। और आत्माएँ अनंत क्या, सौ–पचास क्या, दो भी नहीं होती! वास्तव में आत्मा एक भी नहीं होती क्योंकि वो अचिंत्य है। अगर ये भी कह दिया कि आत्मा एक है, तो तुमने उसके बारे में कुछ सोच डाला। जब तुम मौन हो जाते हो, तो अपने शोर से हटकर अपनी सच्चाई में पहुँच जाते हो, उसी मौन का नाम आत्मा है; और मौन में न एक होते हैं, न दो होते हैं।
आचार्य शंकर का बड़ा सुन्दर श्लोक है। जब मैंने पढ़ा था पहली बार इसे करीब बीस साल पहले, तो बड़ा प्यार हो गया था इससे। अद्वैत (संस्था) का जो हमारा पहला ब्रोशर (विवरणिका) था, उसके मुख्य-पृष्ठ पर ही मैंने इसे छपवा दिया था। उस श्लोक में आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, ‘अरे, दो कैसे हो सकते हैं, जब एक भी नहीं है!’ और मैं बहुत हँसता था। किसी ने पूछा होगा कि सत्य दो हैं कि एक। द्वैतवाद और अद्वैतवाद की बात थी न, कि दो हैं कि एक। तो उन्होंने अपनी ही शैली में उत्तर दिया, कि अरे, दो कैसे हो सकते हैं जब एक भी नहीं है, अद्वैत है; एक नहीं है, अद्वैत है।
‘दो कैसे हो सकते हैं जब एक भी नहीं है‘ - ऐसी है आत्मा! दो की बात तो छोड़ दो कि दो आत्माएँ हैं; एक भी नहीं है वो! और उस अनूठी, अद्भुत, अचिंत्य आत्मा को लेकर के हमने कैसे-कैसे बचकाने किस्से गढ़ लिये; और यही वजह है हमारे आध्यात्मिक और भौतिक, हर तरह के पतन की। यूँ ही थोड़े हुआ है कि भारत, जिसने इतनी आंतरिक ऊँचाइयाँ छुयीं, फिर अंदर और बाहर दोनों दिशाओं में पतन के गर्त में गिर गया; उसकी वजह यही थी। वो जो अंदरूनी ऊँचाइयाँ हमने हासिल करी थीं, हम उन पर कायम नहीं रह पाए। जो बातें हमें हमारे ऋषि समझा गए थे, सौंप गए थे, हमने उन बातों के अर्थ का अनर्थ कर डाला, हमने ‘आत्मा’ शब्द को खिलवाड़ बना डाला। नतीजा जो हुआ है भारत का और सनातन धर्म का, वो हमारे सामने है।
उससे बचना हो, तो अभी भी मेरा सबसे आग्रह है कि उपनिषदों की ओर बढ़िए; और कम-से-कम ‘आत्मा‘ और ‘सत्य’ और ‘ब्रह्म’ शब्द के साथ खिलवाड़ करना बिलकुल बंद करिए!



