ऊँचा उठने को तैयार हो? || आचार्य प्रशांत, वेदांत पर (2020)

Acharya Prashant
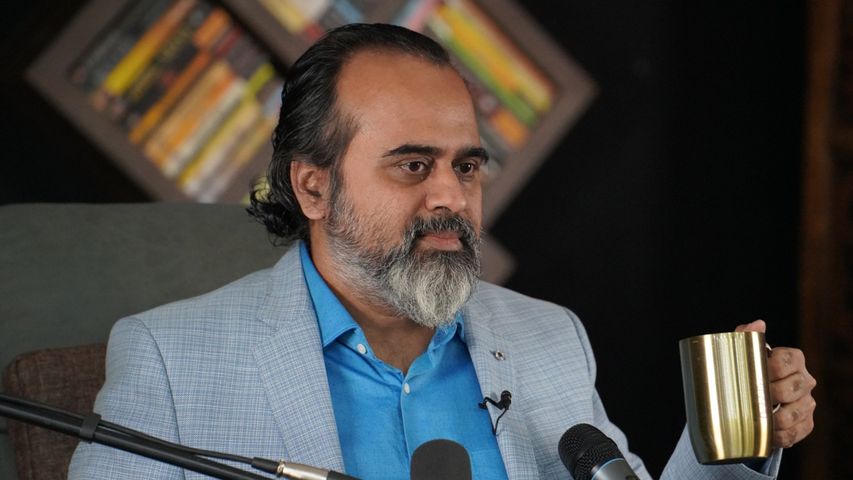
आचार्य प्रशांत: ग्रन्थों का श्लोक हो, गुरुओं का आप्त वाक्य हो, किसी ज्ञानी का आर्ष वचन हो, कभी भूलना नहीं है कि उसमें कुछ भी आपके ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए नहीं कह दिया जाता। उसमें कुछ भी इसलिए नहीं कह दिया जाता कि आपको संसार के बारे में कोई और कहानी पता चल जाए। चाहे विषय सांसारिक हो, चाहे काल्पनिक, अध्यात्म का उससे कोई केन्द्रीय सम्बन्ध नहीं हो सकता। अध्यात्म का केन्द्रीय सम्बन्ध सिर्फ़ और सिर्फ़ जो प्रार्थी है, जो शिष्य है, जो जीवात्मा है, उसके मन से है।
बहुत आगे निकल जाने पर बहुधा ये ख़तरा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से चले थे, किस भाव से चले थे। हम क्यों आये थे उपनिषद् के पास? हम इसलिए तो नहीं आये थे कि हमको पता चले कि देवों की उत्पत्ति कैसे होती है, कितने देव हैं, उनके क्या नाम हैं, वो कैसे आगे बढ़े, किन दानवों से उनका द्वन्द्व हुआ, किन क्षेत्रों का उन्होंने अधिग्रहण करा। तुम इसलिए तो नहीं आये थे न उपनिषदों के पास?
फिर से याद करो बिलकुल, उपनिषद् के पास आये ही क्यों थे? क्यों आये थे? क्योंकि हम अशान्त थे इसलिए हम उपनिषद् के पास आये। हम उपनिषदों के पास अपने सामान्य-ज्ञान अथवा अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि के लिए नहीं आये हैं। जीवन तो हमारा यूँही तमाम तरह के क़िस्सों से, धारणाओं से भरा ही हुआ है न। ये कोई बात हुई कि धर्म-ग्रन्थों के पास भी आ रहे हो और वहाँ से और कहानियाँ पकड़ लीं?
तो ये मूल सिद्धान्त कभी छोड़ना नहीं है कि मैं परेशान हूँ, मैं इसलिए धर्म-ग्रन्थ के पास आया हूँ, और उपनिषद् मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरी परेशानी शान्त हो। तो इस पूरे वक्तव्य के और इस पूरे प्रयास के केन्द्र पर मैं और मेरा आन्तरिक कोलाहल बैठा हुआ है।
तो श्लोक में फिर जो भी बात कही जाएगी, चाहे बात रुद्र की हो, चाहे देवताओं की हो, चाहे हिरण्यगर्भ की हो, ब्रह्मा की हो, हम बार-बार पूछते रहेंगे, 'इसमें मैं कहाँ हूँ? रुद्र कौन? देवता कौन है? हिरण्यगर्भ की बात क्यों हो रही है? अरे भाई! मैं तो उपनिषदों के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे चैन की नींद नहीं आती, मैं दुविधा में पड़ा रहता हूँ, भविष्य की चिन्ता है, अतीत की स्मृतियाँ कचोटती हैं, चारों तरफ़ से असुरक्षा है। मैं तो उपनिषद् के पास इसलिए आया था। मुझे ये क्यों नये-नये प्रसंग, नये-नये नाम दिये जा रहे हैं?'
आप पूछोगे न? जब आप ये प्रश्न पूछोगे तब जाकर के श्लोक आपके सामने उपयोगी तरीक़े से उद्घाटित होगा। नहीं तो बहुतों ने पढ़े हैं उपनिषद्, बहुत पुराने हैं। बहुतों ने पढ़े, लाभ बस कुछ विरलों को हुआ, क्योंकि बाक़ियों ने उपनिषदों को और तमाम अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थों को भी ज्ञान की वस्तु बना लिया। उन्होंने कहा, 'हमें पता है श्वेताश्वतरोपनिषद् के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में क्या बात हुई है।' उन्होंने कहा, 'हिरण्यगर्भ की बात हुई है, हमको पता है।'
अरे बाबा! हिरण्यगर्भ की बात करने से प्रयोजन क्या? हमें बात किसकी करनी है? उपनिषद् चिकित्सक हैं, हम रोगी हैं, तो बात किसकी होगी? रोगी की होगी न? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बात थोड़े से गुप्त तरीक़े से की गयी हो, बात थोड़े से सूक्ष्म तरीक़े से की गयी हो, बात किन्हीं ऐसे प्रतीक-चिन्हों में की गयी हो जिन्हें कोई कुंजी लगाकर के, थोड़ी बुद्धि लगाकर के खोलना पड़ता हो। ये तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता कि शिष्य के मन की बेचैनी को शान्त करने की जगह शिष्य को तमाम इधर-उधर के क़िस्से सुना दिये जाएँ। और जो लोग धर्मग्रन्थों के क़िस्सों पर ही अटक गये हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। उन किस्सों से आगे बढ़ें, ज़रा हौसले का काम करें, ज़रा साहस की बात करें। और साहस की बात ये है कि देखो कि एक-एक जो वहाँ वाक्य लिखा है, शब्द है, उसका आपके जीवन से सम्बन्ध क्या है। ठीक है? तो अब हम उसी को तलाशेंगे।
मात्र मन का ही विस्तार है आदमी का संसार, आदमी के सब शब्द, आदमी की सब कल्पनाएँ, यहाँ तक कि आदमी के देवी-देवता भी। जीव जो कुछ भी अभिव्यक्त कर सकता है अपने शब्दों में, यहाँ तक कि परम सत्य की भी जो अभिकल्पना और अभिव्यक्ति जीव कर सकता है, वो है उसके मन का ही विस्तार। हाँ, मन का विस्तार बहुत निचले तल पर भी हो सकता है, और विस्तृत होकर के, बढ़कर के मन ऊर्ध्वगमन भी कर सकता है। तो हमने कहा था कि मन के सबसे निचले तल पर बैठता है जीव, उससे उच्चतर तल पर जो बैठे हैं, जो मन का उच्चतर तल है उस तल के प्रतिनिधि हैं देवता, और मन की उच्चतम सम्भावना के प्रतिनिधि हैं महादेव या परमात्मा।
सूक्ष्म है बात, समझो। तुम कहाँ पर हो? सबसे नीचे। तुमसे ऊपर कौन हैं? देवता, माने तुम्हारी कामनाएँ, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, कि काश कल मैं ऐसा हो जाऊँ। और उच्चतम कौन है? वो जो सब कामनाओं के पार है। जब सब कामनाओं का उल्लंघन कर देते हो तो वो उच्चतम बिन्दु है। ठीक है? अब कहा जा रहा है, 'मात्र वो उच्चतम बिन्दु ही है जो सब कामनाओं को और सब संसार को समझता है', माने अपने से नीचे वाले सब तलों को समझता है, अधिपति है और सर्वज्ञाता है।
वही स्वामी भी है, वही ज्ञाता भी है। माने कहा ये जा रहा है कि सिर्फ़ वो जो उच्चतम बिन्दु है मुक्ति का, वहाँ पर ज्ञाता हो जाते हो तुम और स्वामी हो जाते हो तुम, अर्थात् उससे नीचे जब तक हो तुम, तब तक क्या हो? सेवक हो, ग़ुलाम हो, और अज्ञानी हो। किसके प्रति अज्ञानी हो तुम? अपनी ही कामनाओं के प्रति अज्ञानी हो तुम, सारे संसार के प्रति अज्ञानी हो तुम। किसके सेवक या ग़ुलाम हो तुम? अपनी ही कामनाओं के ग़ुलाम हो तुम और संसार के ग़ुलाम हो तुम। ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही?
परमात्मा को स्वामी क्यों बोलते हैं? परमात्मा को स्वामी बोलना वास्तव में परमात्मा के विषय में कुछ नहीं बताता, क्योंकि परमात्मा को अपना स्वामित्व या प्रभुत्व दिखाने के लिए कोई दूसरा सामने है ही नहीं। परमात्मा जब है तो मात्र वही है, केवली अवस्था है। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है तो वो किस पर हुक्म चलाएगा भाई? वो स्वामी किसका? अद्वैत में कौन किसका स्वामी? इसी तरीक़े से अद्वैत में ज्ञान कहाँ? जब तक ज्ञान है तब तक कम-से-कम दो चाहिए — एक ज्ञाता, दूसरा ज्ञेय। तो वो जो उच्चतम है, न तो वो अधिपति हो सकता है, न सर्वज्ञाता हो सकता है।
क्यों कहा जा रहा है उसको अधिपति और सर्वज्ञाता? ताकि तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता चले। और यही जगह है जहाँ हमें पहले सूत्र का पुनर्स्मरण कर लेना चाहिए। पहला सूत्र है, 'जो भी बात कही जा रही है वो परमात्मा के बारे में बताने के लिए नहीं कही जा रही है, देवों के बारे में बताने के लिए नहीं कही जा रही है, हमारे बारे में बताने के लिए कही जा रही है।' तो परमात्मा को सर्वज्ञ बोलकर और स्वामी बोलकर वास्तव में हमें हमारे बारे में बताया जा रहा है कि हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो स्वामी है, हम सेवक हैं। उसके नहीं सेवक हैं, इस अर्थ में सेवक नहीं हैं कि वो स्वामी है और हम उसके सेवक हैं। इस अर्थ में कि वो संसार का स्वामी है और हम संसार के सेवक हैं। वो नहीं संसार का स्वामी है, पर हम अवश्य सेवक हैं संसार के। वो संसार का स्वामी है ये बात मात्र प्रतीकात्मक तौर पर कही जा रही है, आपको ये दर्शाने के लिए कि साहब आप बहुत बड़े ग़ुलाम हो दुनिया के। ये बात समझ में आयी?
तो परमात्मा की प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं, कि तू तो सबकुछ जानता है या कि तू इस दुनिया का नियन्ता और पालनहार है। ये बात कुछ जमेगी नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। ये बात वास्तव में आपके अहंकार को असलियत बताने के लिए कही जा रही है। ये मत बोलो, 'परमात्मा! तू सबकुछ जानता है', ये बोलो कि हे जीव! तू कुछ नहीं जानता है। पर ये हम नहीं बोलते।
मूर्ति की प्रतिमा के सामने खड़े हो जाएँगे, या पूजा-आराधना करने लगेंगे और उससे बोलेंगे, 'तू सबकुछ जानता है।' (कटाक्ष करते हुए) हाँ, वो सबकुछ जानता है, और ये जानने के लिए उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ गयी कि वो सबकुछ जानता है। तुम बड़े तोप हो कि बताने आए हो उसको कि तू सबकुछ जानता है, वो तो भूल ही गया था कि वो सबकुछ जानता है। वो सबकुछ जानता है, बस इतना ही नहीं जानता कि वो सबकुछ जानता है। तो फिर तुम आये, तुम परमात्मा से कम थोड़े ही हो, हो भी तो ज़रा से कम हो, तो तुमने कहा, 'यही मौक़ा है, मदद कर दूँ उसकी और उसको बता दूँ कि ओ बाऊ! तू सबकुछ जानता है, या कि तू सबका स्वामी है।'
काहे को उसको बता रहे हो कि वो कौन है, तुम देखो तुम कौन हो। लेकिन हम आरती-प्रार्थना-कीर्तन भी ऐसे ही करते हैं, 'तू सबका स्वामी, तू ऐसा, तू वैसा।' अरे! वो कैसा है वो जानता होगा, तुम जानते हो तुम कैसे हो? नहीं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं, उसकी कोई बात ही नहीं करनी है। जबकि प्रथम सूत्र, फर्स्ट प्रिंसिपल यही है — उसकी नहीं, अपनी बात करो।
उसकी भी जब बात की जा रही है तो इस नाते की जा रही है कि तुम्हें तुम्हारी सीमाओं और क्षुद्रताओं का स्मरण आ जाए। लेकिन वो हम करेंगे नहीं, वो करने में अहंकार को चोट लगती है, हम तकलीफ़ लेना ही नहीं चाहते उतनी। तो उसको उसका बता रहे हैं, 'तू वहाँ रहता है, तू बादलों में रहता है, तू आसमान में रहता है।' वो भी अगर कुछ होता होगा हमारे जैसा, तो वो बड़ा भौंचक्का रह जाता होगा, कहता होगा, 'ये देखो, मुझे मेरे ही बारे में बताया जा रहा है। मेरा पता ये है, एड्रेस दिया जा रहा है, कि तू यहाँ है, सातवें आसमान पर रहता है, तेरा ऐसा हिसाब है, तू फ़लाने का बाप है। तुम मेरी पूजा कर रहे हो कि इल्ज़ाम लगा रहे हो?'
विरला कोई साधक या भक्त या ज्ञानी होता है जो परम-सत्ता के प्रकाश में अपना यथार्थ देखता है, अन्यथा हम अपने सीमित प्रकाश के अन्धकार में परम-सत्ता की कल्पना करते हैं। क्या मूर्खता है ये! तुम परम-सत्ता के पास इसलिए जाते हो ताकि उसके प्रकाश में तुम अपना अन्धेरा यथार्थ देख पाओ, उधर से आती सुनहरी रोशनी में तुम देख पाओ कि तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा और विकृत और गन्दा हो गया है। तुम्हारा चेहरा गन्दा है, ये अन्धेरे में पता चलेगा? तो उसका प्रकाश इसलिए नहीं है कि तुम उसको देखो और कहो, 'आहाहा! क्या सुनहरी आभा है!' उसका प्रकाश इसलिए है ताकि उसके प्रकाश में तुम अपना गन्दा चेहरा देख पाओ और सफ़ाई कर लो भाई!
हम ये नहीं करते। हम उसके प्रकाश से मुँह मोड़ लेते हैं और फिर अपने अन्धेरे जगत में, अपने अन्धेरे के माध्यम से उसकी कल्पना करते हैं। हम उसके माध्यम से स्वयं को नहीं देखते, हम अपने अन्धेरे के माध्यम से उसकी छवि का निर्माण करते हैं। यही इंसान ने धर्म के साथ करा है।
ये सब जो हमारे पूजनीय थे, परम पिता हैं सब ऋषि-मुनि, बड़ा दुख पाते होंगे। कहते होंगे, 'क्या बताया था हमने, किस नाते बताया था, और ये हमारी सन्तानों ने उसका क्या दुरुपयोग कर लिया।' ये बात बिलकुल गाँठ बाँध पा रहे हो या नहीं?
अध्यात्म इधर-उधर की बातें करने के लिए नहीं है, अपने जीवन को देखने के लिए है।
अपनी बात बता भाई, अपनी बात, अपनी बात बता। हटाओ ये सब, 'ये कैसा है? वो कैसा है? बुध ग्रह पर क्या हो रहा है? बृहस्पति का बताओ। ये है, वो है। मैं कुत्ते को देख रहा हूँ, कुत्ते का क्या होगा? मैं कुत्ता हूँ कि नहीं हूँ?' अरे हटाओ! ज़िन्दगी बताओ अपनी। 'मैं सोच रहा हूँ कि कुत्ता क्या सोच रहा होगा', ये कोई आध्यात्मिक चिन्तन नहीं है, ये अहंकार की क्रिया है ताकि उसे सही आत्म-जिज्ञासा न करनी पड़े, इसके लिए वो इधर-उधर की फ़िज़ूल बातों में उलझने की कोशिश कर रहा है।
समझ में आ रही है बात?
वो जो परमात्मा है, जैसे वो अद्वैत है वैसे वो अकर्ता भी है, वो कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता। तुम कितनी भी प्रार्थना करते रहो, वो कुछ नहीं करेगा। यही तो अन्तर है देवी-देवताओं, ईश्वर और परमात्मा में। ये देवी-देवता, ईश्वर, इनको हमने गढ़ा ही इसलिए है ताकि ये हमें इच्छित लाभ दे सकें, इन सबकी मूर्तियाँ कर्तृत्व से ओत-प्रोत हैं। पर जब ब्रह्म की या परमात्मा की या सत्य की बात आती है तो वहाँ न कुछ होता है न हुआ है न होगा, न वहाँ कर्म है न कर्ता है, न कारण है न करण है।
तो फिर उसको क्यों कहा जा रहा है, 'तुम ऐसा कर दो, तुम ऐसा कर दो', वहाँ तो कोई है ही नहीं करने वाला? क्या आशय है? पहले सिद्धान्त पर वापस लौटो, बात समझ में आ जाएगी। पहला सिद्धान्त क्या है? जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें कहीं-न-कहीं मेरा यथार्थ झलकता है। हमारा यथार्थ क्या है? हमारा यथार्थ ये है कि हमारी बुद्धि उल्टी ही चलती है, हमारा यथार्थ ये है कि हमारी बुद्धि स्वयं से मुक्ति के लिए नहीं, अहंकार की रक्षा के लिए चलती है। 'तो मेरे बूते, मेरे करे, मेरे हिसाब से तो जो मेरी बुद्धि चलती है उससे मेरा कल्याण होता दिखता नहीं', एक बार जिसने ये स्वीकार कर लिया अब उसकी बुद्धि कल्याण के मार्ग पर चलने लगेगी।
लेकिन पहले ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, कि मैं जितना अपनी भलाई करना चाहूँगा, अपनी खोपड़ी चलाकर के, मैं अपनी उतनी बुराई कर लूँगा। तो इसीलिए ऋषि बड़े विनीत भाव से अपने कल्याण का सारा दायित्व परमात्मा पर डाले दे रहे हैं, कह रहे हैं, 'मेरा कल्याण तुम देखोगे अब। तुम मेरी बुद्धि को कल्याणकारी बना दो।' हालाँकि परमात्मा बुद्धि को कल्याणकारी बनाएँगे ही नहीं। उन्होंने बुद्धि बना दी है, बुद्धि बना दी है और तुमको चुनाव का विकल्प दे दिया है। उन्होंने तुम्हें कल्याण का मार्ग भी दे दिया है, अकल्याण का मार्ग भी दे दिया है। उन्होंने तुमको विकास और विनाश दोनों का मार्ग दे दिया है, तुम चुनो। इसके आगे वो कुछ नहीं करने वाला, वो अकर्ता है, घनघोर अकर्ता।
भई! तुम्हारे निर्माण के साथ ही परमात्मा का दायित्व पूरा हो गया। तुम अपनेआप में यदि परिपूर्ण नहीं हो तो कम-से-कम परिपूर्णता की सम्भावना ज़रूर लिये हुए हो। परमात्मा तुम्हें अधिकतम जो कुछ दे सकता था उसने दे दिया है, उससे ज़्यादा की माँग करना नासमझी है। वो कुछ और अतिरिक्त तुम्हें दे ही नहीं पाएगा। तो उससे ये कहना कि तुम थोड़ा सा और दे दो, ऐसा करो, बुद्धि तो दे ही दी है, इस बुद्धि को न कल्याणकारी बना दो। परमात्मा कहेगा, 'अब वो तुम्हें ख़ुद करना है। वो तुम्हें ख़ुद करना है।'
करना तुम्हें ख़ुद ही है तो प्रार्थना परमात्मा से क्यों? इसलिए ताकि ख़ुद को ये याद रहे कि आमतौर पर मैं जैसे चलता हूँ, अपना कल्याण नहीं करता, मैं जैसा हूँ अपने अहित का ज़िम्मेदार हूँ मैं। और जिसने ये बात — ये चीज़ थोड़ी सी विरोधाभासी है, समझनी पड़ेगी — जिसने ये बात साफ़-साफ़ स्वीकार कर ली कि मैं अपना दुश्मन आप हूँ, वो अपना दोस्त हो जाता है। जिसने ये बात स्वीकार कर ली कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, उसके ज्ञान का उदय शुरू हो जाता है। जिसने ये बात स्वीकार कर ली कि वो कुछ नहीं जानता, कि वो बहुत छोटा, संकुचित, सीमित, लघु है, समझ लो उसकी चेतना विस्तार पाने लग गयी।
पर ये जो स्वीकार है वो सिर्फ़ शाब्दिक, मौखिक नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अस्तित्व से उठना चाहिए। तुम्हारे गहरे-से-गहरे आन्तरिक बिन्दु से ये स्वीकार उठना चाहिए। तुम्हें स्पष्ट दिखना चाहिए कि हाँ, मैं मूर्ख हूँ। जिसको ये दिखने लग गया कि वो मूर्ख है, उसी पल समझ लो वो मूर्खता से दूर जाने लग गया, मूर्खता से अलग उसके भीतर कोई केन्द्र विकसित होने लग गया। लेकिन जब तक मानोगे नहीं कि मूर्ख हो, जब तक तुम अपनी ही बुद्धि के क़ायल रहोगे, जब तक तुम अपनी ही चेष्टाओं के प्रशंसक रहोगे तब तक तो तुम्हें कुछ मिलने से रहा।
इसीलिए अध्यात्म सिर्फ़ उनके लिए है जो अपनेआप को टूटता हुआ देखने के लिए बिलकुल तैयार हों, जो अपनी ही नज़रों में एक तरफ़ तो गिर जाने को तैयार हों और दूसरी तरफ़ उनमें इतनी श्रद्धा हो कि बहुत गिरूँगा, बहुत गिरूँगा तो भी मुझे पता है कि मेरी नियति तो आकाश ही है। ये दोनों चीज़ें सामान्यतया एक ही व्यक्ति में पाना मुश्किल है, कि वो नीचे-से-नीचा गिरने को भी तैयार हो और नीचे-से-नीचा गिरकर भी उसके हृदय में आकाश बना रहे। ये दोनों बातें एक साथ हों ये असम्भावना हो जाती है, आमतौर पर ये नहीं होता।
हमें ऐसे लोग तो मिल जाते हैं जो कहते हैं कि मुझे कुछ बहुत ऊँचा चाहिए, लेकिन जिनको ऊँचा चाहिए वो ये भी मानते हैं साथ में कि मैं फ़िलहाल भी कुछ नीचे नहीं हूँ। तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएँगे जो अति महत्वाकांक्षी होंगे, और जिनकी महत्वाकांक्षा की इन्तहा ये होगी कि उन्हें परमात्मा भी चाहिए। वो कहेंगे, 'ज़िन्दगी में सबकुछ पा लिया, अब जो आख़िरी चीज़ है, मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन वगैरह, वो भी तो पा लूँ ।' तो वो ऊँची-से-ऊँची चीज़ चाह तो रहे हैं, वो ठीक है उतना, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं हैं कि फ़िलहाल वो बहुत गिरे हुए हैं। वो कहेंगे, 'नहीं, अभी भी मैं कुछ कमज़ोर नहीं हूँ। मैंने काफ़ी चीज़ें हासिल कर ली हैं, बस अब एक आख़िरी चीज़ हासिल करना बाक़ी है।' ऐसों का कुछ नहीं हो सकता।
दूसरी तरफ़ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानने को बिलकुल तैयार रहते हैं कि मैं उथला हूँ, मूरख हूँ, छोटा हूँ, संकुचित हूँ, धोखेबाज़ हूँ, कुटिल हूँ, कामी हूँ', पचास बातें अपने बारे में, गिरे तौर की। लेकिन जो ये ऐसी बातें बोलते हैं, उनके भीतर से ये भाव विलुप्त हो जाता है कि वो ऐसा होते हुए भी वास्तव में अपने केन्द्र पर तो उच्चतम परमात्मा ही हैं। ये दोनों बातें कैसे याद रखें? जो ये दोनों बातें याद रख गया वो जीत गया, 'मैं गिरा हुआ हूँ, लेकिन गिरे रहना मेरा यथार्थ नहीं।'
'क्या मैं गिरा हुआ हूँ?'
'निश्चित रूप से।'
'क्या यही मेरा आख़िरी सत्य है?'
'न-न-न!'
अभी ऐसा हो गया है मेरे साथ कि मैं इतना गिर गया हूँ, और मैं मान रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैं बहुत गिर गया हूँ। मैं बिलकुल बेईमानी नहीं करूँगा, मैं साफ़-साफ़ मानूँगा कि मैं बहुत गिर गया। लेकिन अगर तुम मुझे ये कहोगे कि मैं जैसा हो गया हूँ वही मेरी आख़िरी सच्चाई है तो मैं नहीं मानूँगा। आख़िरी अभी आना बाक़ी है।
आख़िरी आना बाक़ी इसलिए है क्योंकि जो आख़िरी है वो सबसे पहले हो गया था। सबसे पहले क्या हो गया था? सबसे पहले वो हो गया था जो सबसे पहले था। मैं वही हूँ जो सबसे पहले था, तो मैं गिरा हुआ कैसे हो सकता हूँ? अब ये तो मेरा कर्तृत्व है, और ये तो मेरा प्रारब्ध है, और ये तो मेरी मूर्खता है कि उच्चतम होते हुए भी मैंने अपनेआप को निम्नतम बना लिया। बना लिया है निम्नतम, हूँ नहीं। लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूँगा कि निश्चित रूप से फ़िलहाल तो मैंने अपनेआप को निम्नतम बना लिया ही है। ये दोनों बातें साथ में रखकर चलना बड़ा मुश्किल होता है।
लोग समझ नहीं पाते। अभी सवाल आया था, वो बोले, 'एक तरफ़ तो आप बोलते हैं कि इंसान से ज़्यादा कोई मूर्ख नहीं, इंसान से ज़्यादा कोई आत्मप्रवंचना में नहीं, इंसान से ज़्यादा कोई हिंसक नहीं, कुटिल नहीं। दूसरी ओर आप ये भी बोलते हैं, आपका पोस्टर देखा, "बी योर बिगेस्ट फ़ैन" ("ख़ुद के सबसे बड़े प्रशंसक बनिए")। ये भी बोलते हैं कि कितना भी अन्धेरा हो लेकिन तुम्हारे हृदय में सत्य का प्रकाश रहता है। ये क्या बात है? अगर हम इतने ही बुरे हैं तो हम कैसे अपने बिगेस्ट फ़ैन (सबसे बड़े प्रशंसक) हो सकते हैं?'
यही तो बात है। इन दोनों बातों को एक साथ रखना है, न तो ये झूठ बोल देना है कि मेरे भीतर ख़ामियाँ नहीं, तुम्हारे भीतर सौ ख़ामियाँ हों, तुम्हें एक-सौ-एक पता होनी चाहिए, और न उन ख़ामियों के प्रभाव तले आकर के अपनेआप को गिरा हुआ ही मान लेना है।
साफ़ देखना है कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ, और फिर कहना है, 'परमात्मा अभी बाक़ी है।' क्या? 'पूरी पिक्चर देख ली लेकिन परमात्मा अभी बाक़ी है। पिक्चर अभी बाक़ी नहीं है, सब पिक्चरें ख़त्म हो जानी हैं। पूरी पिक्चर ख़त्म हो गयी, एक नम्बर की घटिया पिक्चर थी। सबकुछ घटिया है इस पिक्चर में, मेरी ज़िन्दगी जैसा ही घटिया, लेकिन परमात्मा अभी फिर भी बाक़ी है।'
समझ में आ रही है बात?
ये कहना कि मेरे सामने जो खड़ा है मैं बस उसको नमन कर रहा हूँ, ये अधूरी बात है। तुम्हारे सामने जो खड़ा है, एक तरफ़ तो तुम्हें उसे नमन करना है, और दूसरी तरफ़ उसके अहंकार पर वमन करना है। वमन जानते हो? उल्टी। वो कल वाला अभिवादन याद है न? वो बिलकुल! वो पूरी चीज़ हुई, 'तुम्हारी आत्मा को नमन है, और तुम्हारे अहंकार पर वमन है।' वो पूरी बात है।
प्रश्नकर्ता: जैसा आप ने बार-बार इस सत्र में कहा कि जो परमात्मा है वो कर्ता नहीं होता, तो जो ग्रेस (अनुकम्पा) की बात होती है, कृपा की बात होती है, कि जीसस साहब ने भी कहा है कि "बढ़ते परमात्मा की ओर हज़ार हैं लेकिन सिर्फ़ दस पहुँच पाते हैं।" ये क्या है फिर?
आचार्य: और ग्रेस के बारे में ये भी कहा गया है न कि ग्रेस सदा उपलब्ध होती है। साथ-साथ चलो। क्या ग्रेस को ये कहा गया है कि ग्रेस कुछ ही लोगों को मिलती है और कभी-कभार ही मिलती है? ईश्वरीय कृपा या अनुकम्पा क्या ऐसी चीज़ है जो उसकी ओर से भेदभावपूर्ण तरीक़े से कभी किसी को मिलती हो, कभी किसी को मिलती हो? ऐसा होता है क्या? तो ग्रेस के बारे में ये जानी हुई बात है कि वो उसकी ओर से तो सबको उपलब्ध रहती है, हम चुनाव करते हैं कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो माने उसने कुछ किया क्या? तुम्हें मिली या नहीं मिली, इसकी ज़िम्मेदारी उसकी है या तुम्हारी है? उसकी ओर से तो सबको है, पर मिलती किसी-किसी को है, क्यों? उसने तो दी है, तुम्हें चाहिए क्या?
कोई चीज़ तुम्हें मिल जाए, इसके लिए एक नहीं दो शर्तें होती हैं। उसने दी हो, और साथ-ही-साथ तुम्हें चाहिए हो। उसने तो दी, तुम्हें चाहिए क्या? तो यहाँ पर भी वो अकर्ता है, उसे कोई लेना-देना नहीं, उसने तो चीज़ दे दी। उसने अभी नहीं दी है, उसने तुम्हारे प्रथम क्षण से तुम्हें ग्रेस दे रखी है, तुम लेते हो या नहीं लेते हो ये तुम्हारा निर्णय है।
क्या है ग्रेस ? तुम्हारी सामर्थ्य कि तुम अपनी उच्चतम सम्भावना को पा सको, ये ग्रेस है। और ये सामर्थ्य तुम्हें पहले से मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है, पोटेंशियल (क्षमता)? तुम उसका इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो ये तुम जानो। उसने अपनी ओर से दे रखा है, तुम्हारे माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम कहो, 'कृपा करना! तुम्हारी अनुकम्पा से ही आगे बढ़ूँगा।' न! उसने तो दे ही रखा है, उससे क्या माँग रहे हो? अपनी बात करो, कि उसकी दी हुई चीज़ को भी तुम ग्रहण करके सम्मानपूर्वक प्रयुक्त क्यों नहीं कर रहे, ये पूछो। ये न कहो कि अरे! ग्रेस नहीं मिली। ऐसा नहीं है।
ग्रेस सदा है, अनन्त है, बेशर्त है। बाधा और शर्त तुम्हारी ओर से है।
प्र: शुरू में आपने बताया कि जब भी उपनिषद् के पास आओ तो याद करो कि तुम अतृप्त चेतना हो और अपनी परेशानी से मुक्त होना चाहते हो। बहुत पहले इसी सन्दर्भ में आपने कहा था कि जब भी किसी किताब के पास जाओ तो प्रेमपूर्वक जाओ, इस इच्छा से मत जाओ कि कुछ लेना है। तो फिर इन दोनों बातों को कैसे समझें?
आचार्य: जो एक अतृप्ति की हालत में हो उसके लिए सही प्रेम उसी से है जो उसे तृप्ति दे सकता हो, यही व्याख्या है, यही परिभाषा है उचित प्रेम की, जिसकी ओर जा रहे हो वो भूसा है या कस्तूरी। प्रेम और क्या होगा।
देखो, सन्त का या मुक्त पुरुष का प्रेम इसलिए नहीं होता कि उसे मुक्ति चाहिए; अन्तर समझना। उसका प्रेम इसलिए है क्योंकि उसको कुछ ऐसा प्राप्त हो गया है भीतर-ही-भीतर जिसका स्वभाव है विस्तीर्ण होना, बँटना। तो उनकी बात अलग है। हमारे तल पर हमारा प्रेम कैसा होगा? हम बाँटने के तो क़ाबिल ही नहीं हैं, हमें तो पाना है। सवाल ये है कि हम पाने की उम्मीद किससे रख रहे हैं, भूसे से या कस्तूरी से।
समझ में आ रही है बात?
तो जब मैं कह रहा हूँ कि उपनिषदों के पास प्रेमपूर्वक जाओ, तो उससे मेरा आशय है कि ये याद रखकर जाओ कि तुम्हें जिस चीज़ की कामना है वास्तव में वो तुम्हें उपनिषद् से ही मिलेगी। जिस कस्तूरी की तुम तलाश में हो, वो उपनिषदों में ही है।
YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=UbknL33MA8Y
