क्या परिवार के साथ रहकर सच को नहीं पाया जा सकता? || आचार्य प्रशांत, बाबा बुल्लेशाह पर (2019)

Acharya Prashant
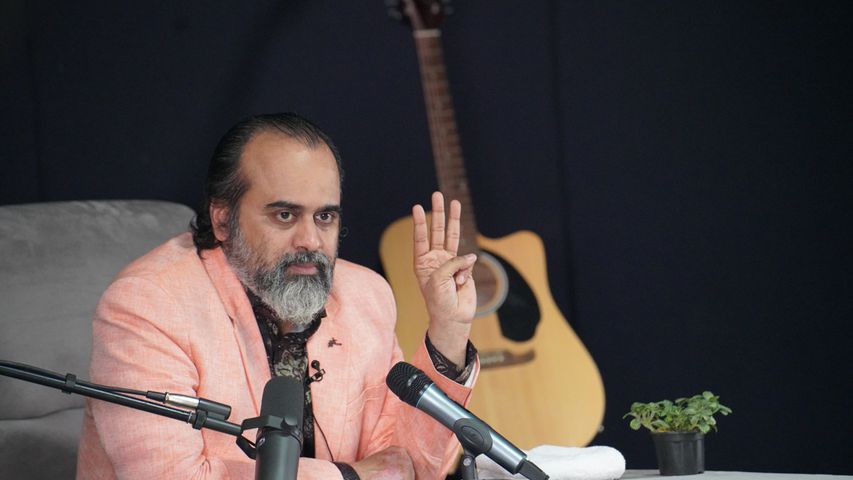
भाग 1
आचार्य प्रशांत: (पत्र पढ़ते हैं) शैलेन्द्र भास्कर हैं, कानपुर से।
मैंनूं कौन पछाणे
हादी मैंनूं सबक पढ़ाया, ओत्थे होर न आया-जाया, मुतलिक ज़ात जमाल विखाया, वहदत पाया ज़ोर नी।
गुरु ने मुझे शिक्षा दी कि यह मार्ग ऐसा है कि वहाँ कोई अन्य आता-जाता नहीं है। गुरु ने मुझे निरपेक्ष सौंदर्य का दर्शन करा दिया है और मैं उसी के रंग में ऐसी रंग गयी हूँ कि अद्वैत ज़ोर दिखाने लगा है।
~ बाबा बुल्लेशाह
नमस्कार, आचार्य जी। बुल्लेशाह जी ने अद्वैत को समझाया है। इस अद्वैत को अपने जीवन में कैसे देखूँ? मेरी समस्या यह है कि मेरी आत्मा तो बहुत तड़पती है अपने को जानने के लिए और मन करता भी है कि सब छोड़कर निकल जाऊँ लेकिन जब से जन्म लिया है तब से माता-पिता ने परवरिश की, पालन-पोषण किया। यदि उन्हें ज़रूरत के समय सहारा न दिया जाए तो यह भी एक प्रकार से प्रभु के प्रति एक अकृतज्ञता होगी। ऐसी स्थिति में क्या कोई ऐसा भी मार्ग हो सकता है कि परिवार के साथ रहते हुए भी परमात्मा का बोध कर पाऊँ? धन्यवाद आचार्य जी।
धर्म की राह पर जो चलता है, शैलेन्द्र, वो तो सबको ही सहारा देता है। स्वयं को सहारा देता है, दूसरों को भी सहारा देगा। तो माता-पिता अगर कमज़ोर हैं या वृद्ध हैं या रोगी हैं, ऐसा तो बिलकुल नहीं है कि धर्म उनकी देखभाल करने को मना करता है। वरना बड़ी विचित्र बात हो जाएगी कि धर्म कहे कि दुनियाभर में जितने असहाय लोग हैं और ज़रूरतमंद हैं उनकी तो देखभाल करो, सेवा करो, और घर में ही जो असहाय हैं उनकी उपेक्षा करो। धर्म ऐसा तो नहीं कहता। जब सबके प्रति करुणा रखनी है तो माता-पिता के प्रति भी रखनी ही है।
हाँ, धर्म भ्रम मिटाने को ज़रूर कहता है। धर्म माता से बचने को तो नहीं कहता पर माया से बचने को ज़रूर कहता है। अगर आप वास्तव में माता-पिता के काम आ रहे हैं तो काम आते भी रहिए, बल्कि जिस दिशा जा रहे हैं, और बढ़िए। माता-पिता के काम आना तो परमार्थ ही हुआ। पर क्या आप वास्तव में उनके काम आ रहे हैं? क्या आप वास्तव में ये समझते हैं कि किसी के काम आने का अर्थ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि काम आने की जगह आप उनकी अपेक्षाएँ ही पूरी कर रहे हों?
अंतर है। किसी का हित पूरा करना और किसी की इच्छाएँ पूरी करना बहुत-बहुत दूर की बातें हैं। इन दो बातों में ज़मीन-आसमान का अंतर है। आप सब भी समझिए। किसी की इच्छाएँ पूरी करना और किसी का हित पूरा करना एक ही बात नहीं है। अध्यात्म सिखाता है दूसरे के काम आओ, अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि दूसरे की इच्छाएँ पूरी करो। माँ-बाप हों, पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, यार हो, समाज हो, उनकी इच्छाएँ पूरी करना उनके हित की बात थोड़े ही है।
रोगी के हित की चीज़ है दवा और रोगी की इच्छा हो सकती है दारू की। दवा और दारू में कुछ अंतर है या नहीं है? रोगी के हित में क्या है? दवा। और वो रोगी भी लीवर का ही हो सकता है। कैसे ख़राब किया लीवर? दारू पी-पीकर के ही ख़राब किया है और वो अभी भी कह रहा है, ‘शराब लाओ, शराब लाओ’। और तुम कहो, 'देखो, अध्यात्म कहता है दूसरों के काम आओ, ये बेचारा संकट का मारा ग़रीब, अद्धा ही तो माँग रहा है। पूर्ण न दे पाएँ इसे, पूर्ण न दे पाएँ तो अद्धा तो दें।' और अद्धा देने के बाद तुम बहुत खुश हो रहे हो कि आज समाज सेवा करी। किसी बेचारे ग़रीब शराबी का गला तर किया।
हममें से अधिकांश लोग जब कहते हैं कि घरवालों के काम आना है तो वो इसी तरीक़े से काम आना चाहते हैं कि रोगी को दवा की जगह दारू दे आये। तुम दोस्त हो या दुश्मन! लेकिन तुम भी करो क्या, उसको दारू दोगे तो दुआएँ देगा और दवा दोगे तो गाली देगा, मारेगा भी। तो तुम्हें भी यही लगता है कि शायद भली बात यही है कि दारू माँगता है तो दारू ही दे दो। फिर अद्धा देना आसान है, मोहल्ला ही शराबियों का है। जगह-जगह शराबखाने खुले हुए हैं।
दवा ज़रा मेहनत की बात है। विवेक लगाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, तय करना पड़ता है कि इसके मुनासिब, इसके अनुकूल क्या दवा बैठेगी, वो दवा लेकर आनी पड़ती है। आग्रह कर-करके, विरोध झेल-झेलकर के उस दवा को खिलाना पड़ता है। उतनी झंझट कौन उठाए! इसको नारंगी चाहिए, नारंगी थमा दो। और इतनी दुआएँ देता है वो कि तुम्हें लगता है कि तीरथ कर आये।
कभी कोई तड़प रहा हो शराब के लिए, उसके हाथ में बोतल दे के देखना। थोड़ी देर में तुम्हें ही लगने लगेगा कि परमात्मा के बाद तुम्हारा ही नंबर है। (श्रोतागण हँसते हैं) इतनी दुआएँ मिलेंगी। और किसी मंझे हुए शराबी की बोतल छीन के देखना कि फिर क्या मिलता है।
दो, ख़ूब दो, अपनेआप को ही बाँट दो। पर थोड़ा विवेक तो रखो कि किसको क्या दे रहे हो। और बुरा मत मानना अगर मैंने शराबी की उपमा का प्रयोग किया। क्योंकि ये दुनिया शराबियों की ही है। यहाँ सब नशे में हैं। यहाँ सब नशे में हैं और सबके पास इच्छाएँ हैं। और सबकी एक ही इच्छा है — हमें और नशा दो। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसी की माँ है कि बाप है कि बेटी है, बेटा है, पति-पत्नी, जो भी है।
हर व्यक्ति जो माँग रहा है, वो उसके लिए विष समान है। क्या तुम उसे वही देना चाहते हो जो वो माँग रहा है? या तुम उसे वो देना चाहते हो जो वास्तव में उसके हित की चीज़ है?
अधिकांशतः किसी को भी वो चीज़ देने से बचो जो वो माँग रहा हो। नियम की तरह पालन कर लो इसका। एकाध-दो ही अपवाद हैं अन्यथा ये नियम हमेशा काम आएगा। जिस व्यक्ति की जो हसरत हो, गहरी तमन्ना हो, समझ लो वही ज़हर है उसका, दे मत देना उसको।
अपने जीवन को ही देख लो न। बड़ी गहराई से, बड़ी ललक, बड़ी शिद्दत से आज तक क्या चाहा है तुमने? ज़हर ही चाहा है न। कभी-कभार जो चाहा है वो मिला नहीं है तो रोये बहुत हो पर बच गये हो। कभी-कभार जब किस्मत फूटी थी तुम्हारी, तो जो तुमने माँगा वो मिल गया, और अब उसको झेल रहे हो, रोज़ रोते हो। जिसका भला करना है उसकी इच्छापूर्ति से बाज आओ।
अब बात आती है इस पर कि इच्छा नहीं पूरी करनी है तो फिर देना क्या है? हित कहाँ है? सबका हित, शैलेन्द्र, एक ही है। अपना हित देखो। जहाँ तुम्हारा हित है वहाँ सबका हित है। हित सबके अलग-अलग नहीं होते। मूलतः जो तुम्हें चाहिए वही सबको चाहिए। सब एक हैं।
लिखा है न तुमने, ‘मन करता है सब छोड़कर निकल जाऊँ।’ लिखा है, ‘आत्मा तो बहुत तड़पती है अपनेआप को जानने के लिए।’ तुम्हारे ही शब्द हैं, उद्धृत कर रहा हूँ। तो यही हैं हम। तड़पती हुई बेचैन चेतना हैं हम। सबके संदर्भ अलग हैं, सबके रूप-रंग-नाम अलग हैं, सबके परिवेश और परिदृश्य अलग हैं लेकिन मूलतः सबकी तड़प और बेचैनी एक ही है। तो हित भी फिर सबका एक ही है; क्या? उस तड़प को शांत किया जाए। शराबी को शराब थोड़े ही चाहिए, शराबी को मुक्ति चाहिए। शराबी को मुक्ति मिलती नहीं तो बोतल पकड़ लेता है। दे सकते हो तो मुक्ति दो। बोतल देकर के क्यों उसकी लत और गहराते हो? प्रेम है माता-पिता से तो उन्हें भी वो दो जो उनके जीवन को सार्थक करेगा।
जो चीज़ें समय की माँग हैं, संयोग की माँग हैं, वो देते चलो। रुपया-पैसा इत्यादि, ठीक है, दे दो। धर्म नहीं मना कर रहा कि माँ-बाप की आर्थिक सहायता नहीं की जानी चाहिए। आर्थिक सहायता की अगर आवश्यकता है, कर दो। पर आर्थिक सहायता भर से तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी हो जाती। प्रेम है यदि वाक़ई तो ज़िम्मेदारी बहुत दूर तक जाती है। वो ज़िम्मेदारी लेकिन तब समझोगे और तब पूरी करोगे जब अपने प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाई हो।
इस बात से तुम्हारे प्रश्न के दूसरे हिस्से पर आते हैं जहाँ पूछ रहे हो कि कैसे घर पर ही रहते हुए, परिवार-समाज में रहते हुए ही परमात्मा की ओर आगे बढ़ो। ये दोनों विरोधी बातें हैं ही नहीं। जो परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगा, वो निस्संदेह परिवार के, मोहल्ले के, समाज के, अखिल विश्व के काम का हो जाएगा। कोई विरोध नहीं है।
ऐसा नहीं है कि घर के एक कमरे में तुम बैठे हो और वहाँ तुम्हारा कोई व्यक्तिगत एनलाइटेनमेंट होगा, बाक़ी सब तो बाधा मात्र हैं। न! जो आगे बढ़ता है वो सबको साथ लेकर ही बढ़ता है, अकेले तो वैसे भी बढ़ा जा ही नहीं सकता। व्यक्तिगत मुक्ति क्या होगी! जो कुछ व्यक्तिगत है उसी से तो मुक्ति पायी जाती है। अपने लिए जानो, क्या पाने योग्य है, और अगर कोई ऊँची चीज़ है जो पाने योग्य है तो क्या उसे अकेले ही गप्प कर जाओगे? जिनसे प्यार है, उनमें बाँटोगे कि नहीं बाँटोगे?
तो यतेंद्र जी (एक श्रोता को संबोधित करते हुए) इसलिए तो अब शिमला या धर्मशाला लेकर आएँगे। मीठी चीज़ मिली है, अकेले थोड़े ही गप्प करेंगे? जिनसे प्रेम है उनमें बाँटेंगे न। ऐसे होता है। जो कुछ अनिष्टकारी मिल गया हो जीवन में, पूरी कोशिश करो कि दूसरे उससे बचे रहें। जितने काँटे मिल गये हों, उनके विरुद्ध दूसरों को आगाह करो। और जो कुछ जीवन में पाने योग्य है, वो ख़ुद भी पाओ और दूसरों को भी दिलाओ। यही अध्यात्म है।
भाग 2
प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, जैसे स्पिरिचुएलिटी (आध्यात्मिकता) कंटीन्यूअस प्रोसेस (सतत प्रक्रिया) है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक सेशन (सत्र) कर लिया या एक वीडियो देख ली और हमारी सारी प्रॉब्लम्स (समस्या) का सॉल्यूशन (समाधान) मिल जाएगा। तो मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट (विशिष्ट वातावरण) में हैं, तो माइंड (मन) उस तरीक़े से वर्क (काम) कर रहा है। या फिर जैसे मैं कितनी बार घर में अकेली हूँ या अपनी कैब में अकेली हूँ तो मेरा जो दिमाग़ है वो थोड़ा उस तरीक़े से काम करता है, मुझे लगता है कि हाँ, क्या सही है क्या ग़लत है। लेकिन जब मैं किसी और माहौल में जाती हूँ जैसे अपने ऑफिस में भी हूँ, तो वहाँ पर बहुत अलग तरीक़े के लोग होते हैं। तो कभी-कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो भी मैं यहाँ पर सीख रही हूँ, मतलब एक प्रोसेस (प्रक्रिया) में जो हूँ, वो प्रोसेस कहीं-न-कहीं फिर वहाँ पर ख़त्म सा हो जाता है। एक तरीक़े से मैं इन्फ्लूएंस (प्रभावित) हो जाती हूँ।
मैंने ये चीज़ कितनी बार अपने अन्दर महसूस करी है कि मैं फिर कहीं-न-कहीं वैसी सी बनने लग जाती हूँ। न तो पूरी तरह इस तरफ़ रहती हूँ और न ही पूरी तरह उस तरफ़ रहती हूँ, बीच में कहीं फँसी रहती हूँ। तो वो भी एक बहुत ही बेकार सिचुएशन (स्थिति) लगती है कि ये क्या है? न तो पूरी तरह उस तरफ़ हो न पूरी तरह आप इस तरफ़ हो। आप बीच में कहीं फँसे हुए हो। तो उसको कैसे हम ठीक करें?
आचार्य: बुरी लगती है वो हालत?
प्र: बुरी लगती है।
आचार्य: तो हट जाओ उस हालत से। बुरी जगह क्यों फँसे हो? ख़ुद ही कह रहे हो कि वैसे होना बुरा लगता है और ख़ुद ही वैसे रहते हो। तो अब इसमें मैं क्या करूँ? मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ग़ौर से देखो क्या अच्छा, क्या बुरा। पर जब वो मुक़ाम आ जाए कि तुम कहो कि मैंने देख लिया क्या अच्छा क्या बुरा, उसके बाद भी मैं वहीं बैठी हूँ जहाँ बुरा, तो अब मैं क्या करूँ? उसके बाद तो बात तुम्हारी तड़प की है, तुम्हारे संकल्प की है।
मैं बता सकता हूँ कि देखो एकदम बिलकुल पीठ पर ही वहाँ दीवार पर छिपकली है तुम्हारे। तुम कहो कि छिपकली यार है हमारी, तो ये तुम्हारी मर्ज़ी।
एक जगह पर आने के बाद गुरु की मर्यादा है कि आगे कुछ न करे। अन्यथा वो दूसरे की मुक्ति में दखलअंदाज़ी जैसी बात होगी। अध्यात्म का क़ायदा है कि सहायता की भी एक सीमा होनी चाहिए। गुरु को भी उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
बताओ, बताओ; समझाओ, समझाओ, समझाओ; लेकिन दूसरे का जीवन जीने मत लग जाओ। ये गुरु को निर्देश है। समझाओ, समझाओ, समझाओ, पर उसकी जगह, उसके बिहाफ़ पर तुम थोड़े ही जी सकते हो! जीना तो उसे ही पड़ेगा न। कर्म तो उसे ही करना पड़ेगा न।
हालाँकि व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ कि बड़ी इच्छा उठती है कि और भी कुछ कर दो। दूसरे के जीवन में प्रवेश ही कर जाओ। जो न चल रहा हो उसको ज़बरदस्ती चला दो। हाथ पकड़ के खींच लो। पर ये करना नहीं चाहिए। ये तो पात्र को, छात्र को, शिष्य को, स्वयं ही करना पड़ेगा। एक जगह पर आकर गुरु को रुकना ही होगा।
उस जगह के आगे का तुम मुझसे प्रश्न करोगी, तो मैं कहूँगा कि वो तो तुम्हारी मर्ज़ी की बात है। दिख रहा है कि कहीं पर हो और जहाँ हो, वहाँ ज़हर है हवा में ही, उसके बाद भी तुम वहीं पर बैठी हुई हो, तो मैं बस समझा सकता हूँ, प्रेरित कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें वहाँ से ज़बरदस्ती उठाकर नहीं ला सकता। चुनाव तुम्हें ही करना है।
प्रश्नकर्ता२: आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं तो मैं अपनेआप को थोड़ा सा टैलेंट (प्रतिभा) में कम फील (महसूस) करता हूँ। जैसे गाँव से आया हूँ और पढ़ाई-लिखाई भी ख़ास ज़्यादा नहीं है। और जैसे दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और इंग्लिश भी सब लोग बोलते हैं। और बहुत सारे मामलों में सब लोग टैलेंटेड (प्रतिभावान) ज़्यादा हैं। तो मैं अपने को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करता हूँ और कॉन्फिडेंस लेवल (आत्मविश्वास) इस मामले में कम रहता है, तो सोचता हूँ कि आगे आने वाले समय में कुछ करना चाहूँ तो आगे कैसे बढ़ूँगा?
आचार्य: क्या हुनर दिखा दिया भाई? (सब हँसते हैं) बच्चे को डरा दिया टैलेंट दिखा के। बेटा, तुम ये बात अपने मुँह से नहीं बोलते तो किसी को लगने नहीं वाली थी। कोई यहाँ नहीं है जो तुम्हारे व्यक्तित्व से या बातों से ये सोचे-समझे कि तुम गाँव से आये हो या तुममें किसी तरह की कमी है।
पहली बात तो गाँव से आना कमी कैसे हो गयी? पीछे अगर चलोगे तो हम सभी गाँव से आये हैं। एक समय पर शहर तो हुआ ही नहीं करते थे, गाँव ही थे। उससे पहले जंगल थे। तो हम सब पेड़ों से उतरे हैं। तो इसमें कमी क्या हो गयी? ये तो समय-समय की बात है कोई कभी कहीं, कोई कहीं।
दूसरे, यहाँ जिस उद्देश्य के लिए आये हो उस उद्देश्य के लिए जो पात्रता चाहिए वो तुममें है ही, वो तुम्हारे यहाँ आने से ही सिद्ध हो गयी। बैठे हो, बात कर पा रहे हो, यहाँ सम्मलित होने के लिए और कौनसा टैलेंट चाहिए! अब तुम ख़ुद ही घोषणा कर दो कि मुझमें कोई कमी है, तो अलग बात है। फिर सब पूछ लेंगे, ‘क्या कमी है?’ बता दो। नहीं तो कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। अंग्रेजी वग़ैरह ठीक है, व्यावहारिक रूप से उपयोगी बातें हैं, लेकिन जब जीवन के पूरे कैनवास को देखो तो उसमें अंग्रेज़ी में नहीं लिखा होता। आती हो अंग्रेज़ी तो अच्छी बात है; फ्रेंच आती हो, मेंडरिन आती हो, और अच्छी बात है। पर नहीं आते ये सब तो कोई गुनाह नहीं हो गया।
स्किल , कौशल सीखना बड़ी बात नहीं होती है। छ: महीना, साल, दो साल में सीखा जा सकता है। असली चीज़ कुछ और होती है। वो हो जीवन में तो जीने का मज़ा है। वो नहीं है और बहुत स्किल्ड हो, टैलेंटेड हो, क्या फ़र्क पड़ता है! एक से एक टैलेंटेड लोग ग़ुलामी का, दुख का, तनाव का, भ्रष्ट जीवन जी रहे हैं। क्या करोगे तुम प्रतिभा का!
मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्किल नहीं होनी चाहिए, बिलकुल हासिल करो। इस समय में जो कुछ ज्ञान चाहिए, मूल कौशल चाहिए जीविका वग़ैरह चलाने के लिए, वो हासिल कर लो। पर वो दूसरे नंबर की चीज़ है। उसको दूसरे नंबर का ही महत्त्व देते हैं। पहले महत्त्व की चीज़ कोई और है। उस मूल चीज़ का ध्यान रखना, बाक़ी सब अपनेआप धीरे-धीरे होगा। करते रहना।
प्रश्नकर्ता३: आचार्य जी, इसी से सम्बन्धित है एक प्रश्न। वैसे घर में पापा हैं, मम्मी हैं। पापा तो थोड़ा पढ़े-लिखे हैं, उनको तो बातें पकड़ में आ जाती हैं। बुक पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मम्मी तो बिलकुल पढ़ी-लिखी नहीं हैं। तो उन तक कैसे बात पहुँचाई जाए?
आचार्य: बहुत सारे संत थे जो पढ़े-लिखे नहीं थे। पढ़े-लिखे नहीं हैं लेकिन जीवन तो जिया है न। बस ये मत करना कि जो पढ़े-लिखे नहीं हैं उनसे तुम पढ़े-लिखों की भाषा में बात करने लग जाओ। ये ग़लती हो जाती है। जो जिस जहान का है उससे उसी भाषा में बात करो न। फिर तुम पाओगे कि उसकी समझ में कमी नहीं है। पर तुम देसी आदमी से रूसी में बात करोगे तो बात बनेगी नहीं न!
संतों ने इसीलिए तो जनभाषा में बात करी। उनमें से बहुतों को संस्कृत का ज्ञान था, जान-बूझकर नहीं बोले संस्कृत। गौतम बुद्ध, महावीर, इनमें से किसी ने संस्कृत में नहीं बात करी। क्योंकि सूत्र यही है — देसी से रूसी में बात नहीं करो।
YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=kGQsg2-g9MY
