आत्मा और जीवात्मा से जुड़ा सबसे बड़ा भ्रम || श्रीमद्भगवद्गीता पर (2020)

Acharya Prashant
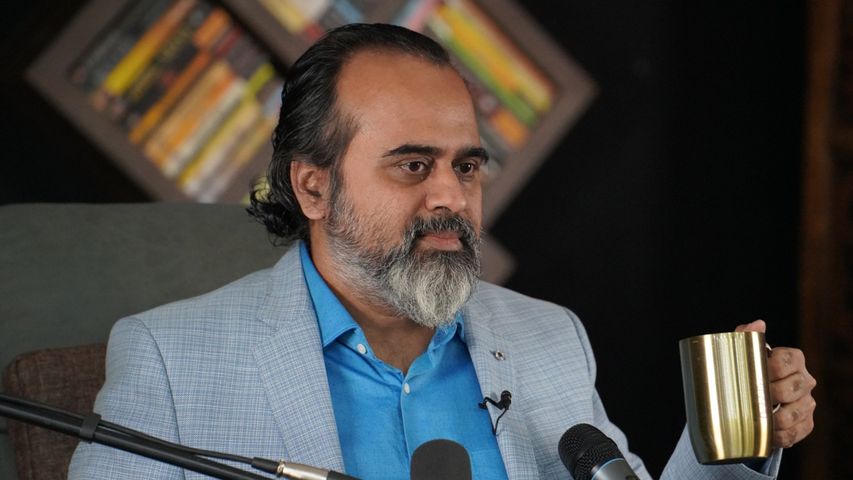
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि | तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही || २, २२ ||
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्यागकर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। —श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक २२
प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्यागकर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है।
ये जीवात्मा कौन है, सूक्ष्म शरीर है, मन है? और सूक्ष्म शरीर को अहम् वृत्ति और तादात्म्य के सम्बन्ध में कैसे समझें? कृपया मार्गदर्शन करें।
आचार्य प्रशांत: जिसे जीवात्मा कह रहे हैं कृष्ण, वो वही है जिसे जीव आत्मा समझता है। आत्मा माने 'मैं', जो तुम वास्तव में हो। तुम्हारा असली नाम, असली पहचान, उसका नाम है - आत्मा। पर जीव आत्मा में तो जीता नहीं। जीव का केंद्र क्या होता है? अहम्। तो जीव जिसे आत्मा समझे, वो हुआ जीवात्मा, अहम्।
तो आत्मा और जीवात्मा बहुत दूर-दूर की बाते हैं। आत्मा और जीवात्मा को एक मत समझ लेना। आत्मा परम सत्य है और जीवात्मा परम भ्रम है। और चूँकि जीव अहम् को ही आत्मा का नाम देता रहता है, कहता रहता है न, “मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ” तो उसने तो 'मैं' के साथ न जाने क्या-क्या जोड़ दिया — अहम् को ही आत्मा बना डाला।
तो इसीलिए फ़िर महात्मा बुद्ध को कहना पड़ा कि आत्मा झूठी बात है। वो वास्तव में यह कह रहे थे कि जिसको तुम आत्मा समझते हो, वो झूठी बात है; क्योंकि तुम तो अहम् को ही आत्मा समझते हो। तुम तो अहम् को पकड़े बैठे हो और यही सोच रहे हो कि 'यही तो आत्मा है मेरी, यही तो सच्चाई है मेरी'। तो जीवात्मा जब आत्मा बनने लग गई तो बुद्ध को कहना पड़ा ‘अनात्मा’।
दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है - जीवात्मा बनी बैठी है आत्मा।
देखा नहीं है हम किस तरह के मुहावरे, अभिव्यक्तियाँ इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं, "मेरी आत्मा रो रही है", "मैं तुमको आत्मा से प्यार करता हूँ", कोई मर जाए तो उसको कहेंगे, “उसकी आत्मा की शांति के लिए सभा रखी गई है।” आत्मा अशांत कैसे हुई, भाई? और आत्मा तो निर्वैयक्तिक है, किसी की व्यक्तिगत कैसे हो गई आत्मा, कि 'उसकी आत्मा', 'मेरी आत्मा', 'तेरी आत्मा'?
आत्मा तो एक है – न तेरी है, न मेरी है।
तो जीव ने क्या खेल चला रखा है? उसने अहम् को ही आत्मा का नाम दे रखा है। और आत्मा के साथ फ़िर वो इस तरह की बातें करता है, "मैं तुझे आत्मा से प्यार करता हूँ।" "मेरी आत्मा की आवाज़ है कि आज पकौड़े खाने ही चाहिए।" "तुम मिलते हो तो मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है।"
इन सब वाक्यों में अशुद्धि क्या है? जहाँ-जहाँ आत्मा कहा गया है, वहाँ कहना चाहिए था 'जीवात्मा', या 'मन' या 'अहम्'। पर हमने मन को समझ रखा है आत्मा, इसीलिए तो हम मन को, अहम् को इतना सम्मान देते हैं, हम बोलते हैं, “ दैट्स मी , वही तो मैं हूँ।” तुरंत बोल देते हैं, “मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ।” हमने अपने झूठ को ही सच्चाई का नाम दे दिया है, और झूठ को सच्चा बना दिया तो झूठ बड़ा सम्मानीय हो जाता है, फ़िर झूठ को हम बड़ा समर्थन देने लगते हैं।
तो इसीलिए ये जो दूसरा अध्याय है श्रीमद्भगवद्गीता का, ये बड़ा प्रासंगिक है। एक श्लोक में श्रीकृष्ण कहते हैं, “आत्मा का न जन्म है, न मृत्यु है, न तेरी है, मेरी है।” और उस श्लोक के तत्काल बाद फ़िर कहते हैं कि “ये जो जीवात्मा है, यही इधर-उधर भटकता रहता है, यही जन्मता-मरता है, यही शरीर धारण करता है।” साफ़ उन्होंने बता दिया है कि आत्मा, सच्चाई का तो जन्म ही नहीं होता, पुनर्जन्म क्या होगा। आत्मा तो सदा से अजन्मा है और अमर है; न उसका जन्म है, न उसकी मृत्यु है; जन्म-मृत्यु तो मन की होती है।
लेकिन फ़िर भी भारत में श्रीकृष्ण की बात को अधिकाँश लोगों ने समझा नहीं। अभी भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करती है। श्रीकृष्ण ने आत्मा के बारे में कहा है या जीवात्मा के बारे में कहा है?
श्रोतागण: जीवात्मा।
आचार्य: और आत्मा और जीवात्मा एक नहीं हैं, ज़मीन-आसमान का अंतर है, भाई। आत्मा के बारे में तो श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि न जन्मती है, न मरती है। जीवात्मा के बारे में कह रहे हैं कि ये इधर-उधर भटकती रहती है। हममें से बहुत लोग इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए आवश्यक है कि मैं पढ़े ही दूँ।
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् | उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते || २, १९ ||
जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही कुछ नहीं जानते क्योंकि वास्तव में आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। —श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक १९
न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूय: | अजो नित्य: शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे || २, २० ||
आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फ़िर होने वाला ही है क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। —श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक २०
फ़िर आगे कहते हैं:
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि | तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही || २, २२ ||
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्यागकर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। —श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक २२
लेकिन हमारी हठ है कि हम कहे जाएँगे कि श्रीकृष्ण ने कहा है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। फ़िर आगे आत्मा के बारे में ही कहा है बार-बार।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक: | न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: || २, २३ ||
इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। —श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक २३
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च | नित्य: सर्वगत: स्थाणुरचलोऽयं सनातन: || २, २४ ||
क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। —श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक २४
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते | तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि || २, २५ ||
यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकाररहित है। इससे हे अर्जुन! इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है अर्थात् तुझे शोक करना उचित नहीं है। —श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय २, श्लोक २५
ये सब बातें किसके बारे में कहीं? आत्मा के बारे में। और जन्म-मृत्यु किसकी बताई? जीवात्मा की। जीवात्मा माने? दोहराएँगे हम, अहम्। और मन क्या है? अहम् स्वयं को केंद्र में रखकर अपने इर्द-गिर्द जो संसार खड़ा करता है, उसका नाम है 'मन'; मन माने संसार। संसार के केंद्र में जो 'मैं' बैठा है, उसका नाम है 'अहम्'। ये अहम् है जो जीवन-मरण, जीवन-मरण का चक्र खेलता रहता है; अभी है, अभी नहीं है, अभी है, अभी बदल गया। मन बदलता रहता है न लगातार? मन के बदलाव की बात हो रही है।
मन के केंद्र में है अहम्। शरीर क्या है? मन का ही स्थूल प्रतिबिम्ब। सूक्ष्म रूप से जिसको आप मन कहते हैं, वही जब स्थूल हो जाता है तो शरीर और संसार कहलाता है; सूक्ष्म है तो मन और स्थूल है तो शरीर और संसार।
तो अगर मन बदलेगा तो मन के साथ-साथ क्या बदल जाएगा? शरीर और संसार बदल गए न? इसी बात को कृष्ण कह रहे हैं कि ये जीवात्मा बार-बार अलग-अलग शरीर ग्रहण करती है; क्योंकि जीवात्मा का काम ही है परिवर्तित होते रहना। जीवात्मा परिवर्तित होगी तो संसार तो परिवर्तित हो ही जाएगा न? जब केंद्र ही बदल गया तो वृत्त तो बदल जाएगा।
पर इसका अर्थ कुछ ऐसा लगाया है कि जब व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर से आत्मा उड़ती है और फ़िर जा करके किसी गर्भिणी के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। और इस तरह का बड़ा अंधविश्वास प्रचारित किया गया है, चित्र इत्यादि बनाए जाते हैं यह दिखाने के लिए कि पुनर्जन्म कैसे होता है। क्या बता रहे हैं श्रीकृष्ण और नासमझों ने क्या समझा उसको!
तीन हैं, तीनों को समझिएगा; आत्मा – जिसका कोई जन्म नहीं होता। प्रकृति – जिसमें अनंत जन्म और अनंत मृत्यु हैं। और व्यक्ति – जिसका एक जन्म और एक मृत्यु है। आत्मा: न जन्म, न मृत्यु, प्रकृति: अनंत जन्म, अनंत मृत्यु, और व्यक्ति, जो आप हैं, उसका एक जन्म, एक मृत्यु।
पर व्यक्ति अपनी क्षणभंगुरता के तथ्य से डरकर घोषित कर देता है कि या तो वो आत्मा है या फ़िर अपने-आप को बोल देता है कि “मैं तो प्रकृति हूँ। मेरे तो अभी बहुत जन्म और बहुत मृत्यु होंगे।” दोनों में ही उसका स्वार्थ एक ही है, अपनी एक और आखिरी मृत्यु के तथ्य से बचना, छुपना, झुठलाना। हमें इस बात से इतना खौफ़ है कि एक ही जीवन है और उसकी एक ही मृत्यु है। हम डर से बचने के लिए श्रीकृष्ण की बात को भी तोड़-मरोड़ देते हैं।
कभी हम कह देते हैं, “मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अमर हूँ। मेरी मौत होगी ही नहीं।” ये बात झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि अपना जीवन देखो। आत्मा तो विकाररहित है और तुम्हारे जीवन में विकार-ही-विकार हैं। तुम आत्मा कैसे हो गए? आत्मा तो निर्लेप है, निर्मम है, निर्मोह है और तुम्हारे जीवन में लिप्तताएँ हैं, मोह है और ममता है। तुम आत्मा कैसे हो गए? पर जीवन में तमाम तरह के दोष, विकार, मोह, ममता भरे-भरे भी हम कहते हैं, “मैं तो आत्मा हूँ और मैं अमर हूँ।” ये झूठ हुआ न?
और ये घातक झूठ है, क्योंकि जब तक ये झूठ रहेगा, तब तक आप जीवन में वृत्तियों को, विकारों को, मोह को, ममत्व को, अहंता को प्रश्रय दिए जाएँगे। आप कहेंगे कि इनको रखे-रखे ही अगर अमरता मिली जा रही है तो इनको हटाएँ काहे को?
और फ़िर दूसरा झूठ हम ये बोल देते हैं कि 'श्रीकृष्ण ने बताया है न पुनर्जन्म होता है, तो मेरा भी पुनर्जन्म होगा'। नहीं, आपका कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। अस्तित्व में बहुत पुनर्जन्म होते हैं, प्रकृति में पुनर्जन्म होते हैं; व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं होता।
अभी उस दिन मैं कह रहा था आज से कुछ वर्ष पहले भी यहाँ पर बहुत सारे खरगोश थे आश्रम में और आज भी यहाँ बहुत सारे खरगोश हैं। और कुछ वर्ष पहले का चित्र देखें खरगोशों का और आज का कोई चित्र देख लें, कोई फ़ोटो ले लें, तो वो दोनों आपको एक जैसे लगेंगे। तीन साल पहले भी सफ़ेद खरगोश थे, आज भी सफ़ेद खरगोश हैं, संख्या भी उनकी करीब-करीब उतनी ही है। प्रकृति ने पुनर्जन्म लिया है।
तथ्य यह है कि कुछ साल पहले जितने खरगोश थे, अब उनमें से एक भी बचा नहीं है, वो सब गए। उन जीवों का कोई पुनर्जन्म नहीं है, वो तो गए, लेकिन खरगोश अभी भी हैं - ये पुनर्जन्म है। खरगोश बाकी हैं, वो जो विशिष्ट खरगोश था, वो बाकी नहीं है। समझना, खरगोश बचे हैं लेकिन गोलू खरगोश नहीं बचा, वो गया।
हाँ, खरगोश आज भी है, खरगोश पाँच सौ साल पहले भी था, और खरगोश, जहाँ तक समझते हैं, अगर आदमी ने पृथ्वी ही नहीं उड़ा दी, तो पाँच सौ साल बाद भी होगा। खरगोश तब भी था, आज भी है, पाँच सौ साल बाद भी होगा। प्रकृति लगातार पुनर्जन्म ले रही है, ले रही है, ले रही है। उसके अनंत पुनर्जन्म हैं, लेकिन गोलू लौटकर नहीं आएगा, उसका एक ही था।
इन तीनों का भेद समझना बहुत आवश्यक है। आत्मा – न जन्म, न मृत्यु। जीव – एक ही जन्म और एक ही मृत्यु। और जीव का भला इसी में है कि वो उस एक जन्म का सदुपयोग कर ले पूरा-पूरा। आप जीव हैं और आपकी भलाई इसी में है कि आप याद रखें कि एक ही जन्म है—मौत निकट आ रही है लगातार—और जन्म का, समय के एक-एक पल का आप सदुपयोग कर लें।
और तीसरी प्रकृति। प्रकृति का चक्र चलता रहता है; लोग आते हैं, लोग जाते हैं। कोई आए, कोई जाए, लोग रह जाते हैं। वहाँ बहुत पुनर्जन्म हैं पर पुराना नहीं लौटकर आता; प्रकृति ही बार-बार लौटती है, कोई पुराना नहीं लौटता। वो जो व्यक्ति था, वो नहीं लौटेगा। कितने भी खरगोश पैदा होते रहें, गोलू नहीं लौटेगा। वो जो एक विशिष्ट व्यक्ति था, वो नहीं लौटेगा। हाँ, व्यक्ति बहुत सारे आते-जाते रहेंगे। अंतर स्पष्ट हो रहा है?
अब इस विषय में कभी संशय नहीं होना चाहिए। खासतौर पर गीता की आड़ ले करके अपने पूर्वाग्रह कभी प्रसारित न करें। कभी न कहें कि श्रीकृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। उन्होंने व्यक्ति के पुनर्जन्म की बात नहीं करी है, न उन्होंने आत्मा के पुनर्जन्म की बात करी है। किसका पुनर्जन्म बताया है? जीवात्मा का। और जीव कौन है? जिसने प्रकृति से साझा कर लिया है।
जब मैं कह रहा हूँ कि आप जीव हैं तो मेरा आशय क्या है? आप वो हैं जो अपने-आप को देह समझते हैं। देह माने प्रकृति। तो जीवात्मा कौन? जिसने देह से अर्थात प्रकृति से तादात्म्य कर लिया है। तो हमने क्या कहा था, पुनर्जन्म लगातार किसका होता है? प्रकृति का। और श्रीकृष्ण क्या बता रहे हैं कि कौन है जो नए-नए शरीर धारण करता है? बात समझ में आई? जीव माने वो जो प्रकृति से तादात्म्य कर चुका है, जो देहाभिमानी है; जो अपने-आप को देह समझता है सो जीव, जो अपने आप को जीवित समझता है सो जीव। शरीर को तो कहते हो न जीवित है, शरीर को ही कहते हो मर गया।
आप रहें, न रहें, जो लोग रहेंगे, वो भी इंसान ही कहलाएँगे न? ये पुनर्जन्म है। डीएनए आगे बढ़ता रहेगा, आप आगे लेकिन नहीं बढ़ेंगे। तो आप इस उम्मीद में बिलकुल मत रहिएगा कि "फ़र्क़ क्या पड़ता है, अभी तो लाखों जन्म मिलेंगे। एकाध-दो ख़राब भी कर दिए तो क्या होता है!" लाखों नहीं मिलेंगे, आपको एक ही है, उसका सदुपयोग करिए।
प्र२: सत्य और धर्म पर चलने वाले को इतने कष्ट क्यों मिलते हैं?
आचार्य: जो नहीं चल रहे धर्म पर क्या उन्हें कष्ट नहीं मिल रहे हैं? और जो चलता है धर्म के रास्ते पर, उसका इरादा क्या होता है? कष्ट से बचना या धर्म की मंज़िल को पाना?
धर्म, आपने ही कहा, एक रास्ता है। उस रास्ते की कोई मंज़िल होती है, उस मंज़िल का आकर्षण होता है, उस मंज़िल में आनंद होता है। जब उस मंज़िल में आनंद होता है तो यात्रा भी आनंदप्रद हो जाती है। धर्म का रास्ता इसलिए है कि आपको सुख मिले, कष्टों से रक्षा रहे, या वो इसलिए है कि आपको वो मंज़िल मिले जिससे आपको प्रेम है? तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो जाएँगी, कि वो ख़ास मंज़िल भी मिल जाए जो जीवन को सार्थकता देती है और सुख भी मिलता रहे?
सुख-दुःख पर इतना ध्यान है तो मंज़िल पर नज़र है भी क्या? जिनकी मंज़िल पर नज़र होती है, उन्हें यह ख्याल कहाँ रह जाता है कि सुख मिल रहा है, कि दुःख मिल रहा है। वो कहाँ ये तुलना करते हैं कि 'मैं तो धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे इतना कष्ट मिला और ये पड़ोसी पापी, अधर्मी, ये मज़े ले रहा है'? इसका मतलब आपको प्रेम मंज़िल से नहीं है, आपको प्रेम सुख से ही है। आप यह नहीं देख रहे कि आप मंज़िल के निकट पहुँचे कि नहीं पहुँचे, आप गिन रहे हैं सुख कितना मिला, “अरे, सुख कम मिला, कष्ट ज़्यादा मिला, ये रास्ता चलने में क्या लाभ है?”
उस रास्ते पर सुख-दुःख नहीं गिना जाता, उस रास्ते पर यात्रा करी जाती है मंज़िल का मुँह देख-देखकर। पाँव के नीचे काँटें भी हों तो भी नीचे नहीं देखा जाता। पथिक को ऊर्जा मिलती है गंतव्य का मुँह देखकर। तुम देख रहे हो और उधर कुछ ऐसा है जिसको देखने भर से ताक़त मिल जा रही है और तुम चलते जा रहे हो। पाँव के नीचे कंकड़ है या काँटा, पता ही नहीं चल रहा। कंकड़-काँटे का पता चल रहा है तो इसका मतलब कंकड़-काँटे ही गिन रहे हो। लक्ष्य से कुछ प्रेम ही नहीं।
फ़िर ये भूलिए नहीं कि वो कंकड़-काँटे वास्तव में क्या हैं, वो धर्म ने आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं बिछा दिए हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म की राह चलता है, मुक्ति की मंज़िल की तरफ़, तो उसको कष्ट मिलते हैं। वो कष्ट वास्तव में क्यों मिलते हैं? वो कष्ट कोई और हमें नहीं दे रहा, वो हमारे ही पुराने ढर्रे हैं जो हमें कष्ट दे रहे हैं।
बँधन माने? हमारी वृत्तियाँ, हमारे पुराने संस्कार, आदतें और ढर्रे, धारणाएँ और मान्यताएँ। वो हमारी ही चीज़ें हैं न? वो सत्य ने हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर रखी हैं, वो हमारी निजी सम्पदा है, वो हमारा ही माल है। और वो परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है तो इसमें किसी और का क्या दोष?
कोई बहुत मोटा आदमी हो। वो दौड़े और फ़िर शिकायत करे कि ये तोंद परेशान करती है, दौड़ने नहीं देती। वो तोंद किसी और ने ला करके तुममें जोड़ दी है, तुम पर आरोपित करी है, तुम्हें पहना दी है, टोपा है? या वो तुम्हारा अपना माल है, तुमने ही संचित किया है? बोलो।
तो धर्म की यात्रा ऐसे ही होती है। चलते-चलते तोंद गलानी होती है। हम तोंद हैं। तोंद माने क्या? वो सब जो अनावश्यक है पर जिसे तुमने अपने वजूद का हिस्सा बना लिया। तोंद की यही परिभाषा है न? जो अनावश्यक है पर हमारी हस्ती का अंग बन बैठी है। जो होनी नहीं चाहिए थी पर है, जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए था पर रिश्ता बन गया है, उसी का नाम वृत्ति है, उसी का नाम तोंद है। अब उसको लेकर आगे बढ़ोगे तो कष्ट तो होगा ही, पर ये कष्ट तुमको मंज़िल नहीं दे रही है, ये कष्ट तो चटोरेपन से मिला है।
जितना बढ़ते चलेंगे, तोंद उतनी कम होती चलेगी। और रुक करके उसी का रोना रोने लगे तो तोंद तो चाहती ही यही है कि कोई रुक जाए। रुक जाएँगे, “अरे, क्या बताएँ, बड़ी तकलीफ़ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे।” तभी इधर-उधर कुछ-कुछ चाट, चुरमुरे का ठेला भी दिख जाएगा, “लाओ रे, बहुत परेशान हैं।” तोंद बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ना और मुश्किल होता जाएगा।
तरीका क्या है? बस बढ़ते रहो। बढ़ते रहो, गलते रहो, बढ़ते रहो, गलते रहो। मत परवाह करो कि कष्ट मिल रहा है। ये कष्ट शुभ है। और दूसरों से तुलना तो करना नहीं कि हम ही पागल हैं जो बढ़ते जा रहे हैं और कष्ट झेले जा रहे हैं, और कितने ही लोग हैं जो घरों में बैठे हैं। उन्हें कोई यात्रा नहीं करनी, उन्हें कोई मुक्ति नहीं, कोई मंज़िल नहीं चाहिए। उन्हें कोई कष्ट ही नहीं है।
प्रेम दूसरों से तुलना कर-करके नहीं किया जाता। मंज़िल से प्यार किसको है, तुमको या दूसरों को? तुमको है न? तो मंज़िल की खातिर तकलीफ़ भी कौन झेलेगा, तुम या दूसरे?
या कभी प्रेम में आगे बढ़ते हो, किसी से मिलने जाते हो कुछ तकलीफ़ झेलकर तो शिकायत करते हो? कि सारी तकलीफ़ हम ही झेल रहे हैं। बस पकड़नी पड़ रही है, ठंड में ठिठुरना पड़ रहा है, टिकट कटाना पड़ रहा है। प्रेमिका भी तो तुम्हारी ही है। इतनी तकलीफ़ हो रही है तो अपनी जगह किसी और को भेज दो, कि “भाई, कष्ट बहुत होगा हमें जाने में। जाड़े की रात में बुलाया करती है। ऐसा कर, तू चला जा।” आउटसोर्सिंग का ज़माना है, कुछ भी चल सकता है। क्या पता! हर काम के विशेषज्ञ होते हैं, *फंक्शनल स्पेशलिस्ट्स*।
कुछ बातें पूरी तरह से निजी रखिए। उनमें तुलना इत्यादि का कोई सवाल नहीं होता। उनमें यह नहीं देखा जाता कि दूसरे को क्या मिला, कितना मिला। और प्रेम में तो तुलना बिलकुल घातक हो जाती है। जहाँ आपने यह देखना शुरू किया कि मुझे कितना मिला और दूसरे को कितना मिला, खेल ख़त्म। प्रेम टूटता ही तुलना से है। जहाँ आपने अपने सम्बन्ध को छोड़कर दूसरे के सम्बन्ध की तुलना करनी शुरू की, आप हारे, आप गए।
प्र३: ग्रन्थ पढ़ते वक़्त कई बार शब्दों के अर्थ का अनर्थ हो जाता है जिससे आस-पास के लोगों में लाभ से ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। कृपया मार्गदर्शन करें।
आचार्य: जब श्रीकृष्ण अर्जुन से गीता कह रहे हैं तो इसलिए तो उन्होंने नहीं कही थी गीता कि वो किताब बन जाए। उन्हें तो कहना था अर्जुन से और उनकी ओर से उनके कथन का प्रयोजन पूरा हो गया जिस क्षण अर्जुन के समक्ष अट्ठारवाँ अध्याय पूरा हुआ, है न? श्रीकृष्ण का ये तो नहीं इरादा था कि श्रीमद्भवद्गीता नामक एक किताब रचें, उन्हें तो अर्जुन से कुछ कहना था, उन्होंने कह दिया, उनकी बात पूरी हो गई, खेल ख़त्म।
लाभ भी तभी होता है जब सामने कोई हो और तुमको देखकर, तुमको समझकर तुम्हें उपदेश दे। पुस्तक एक सीमा तक लाभ दे सकती है, उसके आगे नहीं दे पाएगी। उसके आगे अगर लाभ तुम्हें पुस्तक से चाहिए तो तुममें बड़ी विशिष्ठ प्रतिभा होनी चाहिए या फ़िर गहरी मुमुक्षा।
कल्पना करो कि अर्जुन व्याकुल है, किंकर्तव्यविमूढ़ है और श्रीकृष्ण ला करके उसके हाथ में वेद थमा देते हैं, कहते हैं, “ले, पढ़ ले। तेरी व्याकुलता का इलाज इन ग्रंथों में है।” काम बन जाता अर्जुन का? और गीता में ऐसी तो कोई बात कृष्ण ने कही नहीं है जो वेदों ने ना कही हो। जो कुछ श्रीकृष्ण गीता में कह रहे हैं, वो सब वेदों और वेदांत में पहले से ही मौजूद है न?
तो श्रीकृष्ण ने फ़िर क्यों कष्ट उठाया बात को नए और ताज़े तरीके से कहने का? जब वो बात पहले ही उपनिषदों में मौजूद थी तो श्रीकृष्ण को इतना ही करना था कि ग्यारह प्रमुख उपनिषद् ला करके अर्जुन के हाथ में थमा देते और कहते, “युद्ध से एक दिन का विश्राम ले। जा, रातभर इनको पढ़ ले, तेरी सारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी।” अर्जुन भी कहता, “बढ़िया, ये अच्छा समाधान है। लाइए दीजिए।” वो वापस जाता, किताबों का तकिया बनाता और मस्त सोता, जैसे आप सोते हैं किताबों पर।
तो उन्हीं उपनिषदों को फ़िर श्रीकृष्ण ने गीता के रूप में अर्जुन से कहा। गीता में वास्तव में कुछ भी नया नहीं है; सत्य नया हो भी नहीं सकता। गीता को कहीं-कहीं पर एक उपनिषद् ही माना जाता है, प्रस्थानत्रयी का हिस्सा माना जाता है, उपनिषदों के समतुल्य रखा जाता है।
तो बात तो यहाँ वही है जो पहले ही वेदांत में मौजूद थी, पर जब कोई कृष्ण सामने बैठकर समझाए, समझ में तभी आती है। नहीं तो सोचो, अर्जुन चला जा रहा है ग्यारह किताबें लिए। उसकी शक्ल देखो, उसकी हालत देखो और उन किताबों को देखो। तुम्हें लग रहा है वो पढ़ेगा भी? वो तो पहले ही मन बना चुका है, कह रहा है, “लड़ाई झगड़ा बेकार की बात।”
पुस्तकों का अपना महत्व होता है, पर कोई पुस्तक किसी जीवित मार्गदर्शक का स्थान नहीं ले सकती। गहरा और असली परिवर्तन तो तुममें सत्संगति से ही आएगा।
और इसीलिए हम किताबों की ओर भागते हैं; क्योंकि परिवर्तन खतरनाक होता है और किताबों के साथ वो खतरा नहीं होता। कितने ही हैं जो कहते हैं, “आपके वीडियो देख लेंगे, आपके सामने नहीं आएँगे।” उनमें से बहुत इस वक़्त भी लाइव देख रहे होंगे। “जितनी बात हो रही है, वो साफ़-साफ़ आ तो रही है पर्दे पर। 4G का ज़माना है, 5G आने वाला है। और फ़िर वातावरण में प्रदूषण बहुत है। हम आएँ, पेट्रोल जलाएँ, उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ेगी?” पर्दे पर खतरा कम है, यहाँ है।
आप कभी गौर नहीं करते, आप जिन किताबों को पढ़ते हैं आध्यात्मिक साहित्य में, वो वास्तव में किताबें हैं ही नहीं? वो लिखी नहीं गई थीं, वो कही गई थीं। वो संवाद हैं, बातचीत हैं दो लोगों की, अधिकांशतः। तो वो जो बात है, वो किसके काम आएगी? जिससे कही गई थी। अब किसी से कही गई थी, बाद में उसको लिख भी दिया गया। अरे भाई, अगर लिखने में ही उसका सार होता तो फ़िर मूल रूप से भी उसे लिखा ही गया होता। कहा क्यों गया?
श्रीकृष्ण ने गीता लिख डाली होती, उसकी हज़ार, दो-हज़ार प्रतियाँ छपवा ली होतीं और जो कोई मिलता उलझन में, धर्मसंकट में, उसको कहते, “ये लीजिए, *न्यू यॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर*।” ऐसा कर रहे हैं क्या कृष्ण? ऐसा तो नहीं कर रहे। जब स्थिति सामने आ रही है, उस स्थिति में जो बात उपयुक्त है, अनुकूल है, वो बात ताज़ी-ताज़ी, बिलकुल मौलिक, एकदम आत्मिक, एकदम सच्ची, कह दे रहे हैं। कोई पहले से ही छपी हुई किताब नहीं तैयार है।
ताज़ी बात में जो दम होता है, वो छपी बात में कभी नहीं हो सकता। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि छपी बात बिलकुल मूल्यहीन होती है। उसकी भी एक जान होती है। पर बाग का ताज़ा आम हो और डब्बाबंद आम का रस, कुछ फ़र्क़ तो होगा न, या नहीं होगा? एक में प्राण हैं, एक में केमिकल (रसायन)। प्राण और प्रिज़र्वेटिव (परिरक्षक) में से क्या चाहिए? प्राण चाहिए न? तो ताज़ा आम खाओ।
