गलत ज़िंदगी, और गलत काम की आदत || आचार्य प्रशांत (2020)

Acharya Prashant
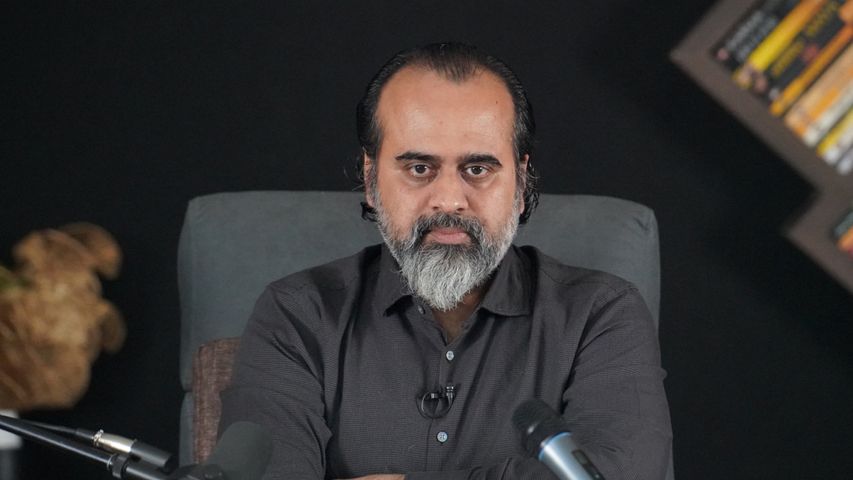
प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, प्रणाम! मैं पच्चीस वर्ष का हूँ। मार्केटिंग का कार्य करता हूँ जिसमें लोगों के मन में लालच पैदा करना मेरे लिए अनिवार्य है। यह काम करते-करते आदत ऐसी पड़ गयी है कि अब मेरा स्किल स्किल सेट (कौशल) ही यही हो गया है कि कैसे दूसरे लोगों में लालच पैदा कर सकता हूँ। तो मेरे जीवन का एक भाग यह है, दूसरा भाग वह है जो अभी यहाँ पर बैठा हुआ है। इन दोनों में सामंजस्य कैसे पैदा करूँ?
आचार्य प्रशांत: क्या बताऊँ मैं इसमें? माने (आपको) काम वही करना है जो कर रहे हैं?
प्र: जी, क्या इस प्रकार का कार्य ग़लत है?
आचार्य: अब तुम जानो न कि अगर अपनेआप से थोड़ा-सा दूर होकर के अपनेआप को देखते हो तो क्या दिखाई पड़ता है? ठीक है? मान लो जिसे देख रहे हो (वो) तुम नहीं हो, कोई और व्यक्ति है वो, ठीक है, उसकी शक़्ल भी कुछ और है। वो जिसको देख रहे हो वो तुम हो ही नहीं। और अब देखो कि वो जो व्यक्ति है कर क्या रहा है? उसकी पूरी दिनचर्या देखोगे (कि) वो क्या कर रहा है– वो किसी में डर पैदा कर रहा है, किसी को ललचा रहा है, ये सब कर के माल बेच दिया, जब माल बेचा भी तो मन में ख़याल यही आया कि सही बुद्धु बनाया।
फिर वो पैसा जेब में आया, पैसा जेब में आया भी तो भीतर से ज़रा सा तो अपराध भाव उठा ही, कि ये पैसा है तो गड़बड़ ही। फिर गये वो पैसा जिस भी चीज़ में खर्च-वर्च करना था कर आये। फिर अगले दिन गये फिर यही सब करा।
जिसको लालच दिखाकर चीज़ बेच रहे हो वो चीज़ उसके भी काम की होगी तो नहीं, नहीं तो इतना ललचाना क्यों पड़ता उसको? तो जिसको चीज़ बेच दी वो चीज़ लेकर घर पहुँचा, वो कुछ देर तक उसको देख रहा है, फिर चीज़ की हकीकत सामने आयी तो फिर वो भी तुम्हें बद्दुआ दे रहा है!
ये सब चल रहा है। अब इसमें तुम्हें मैं क्या बताऊँ कि काम सही है कि ग़लत है? सही-ग़लत तो क्या होता है, राख ही हो जाना है एक दिन तुमको। तो अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं।
आसमानों को और ग्रह-नक्षत्रों को तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है नहीं कि तुम ज़िंदगी कैसी बिता रहे हो। तुम्हारे अपने सुकून की बात है। तुम जो कर रहे हो तुम्हें ये ठीक लगता है तो करे जाओ, नहीं ठीक लगता है तो होश में आओ।
अधर्म ऐसे ही थोड़े ज़िंदा रहता है। वो कारणों से ज़िंदा रहता है और कारणों में वो बड़े-से-बड़ा कारण गिनाता है ‘मजबूरी'। वो कहता है– 'हम मजबूर हैं इसलिए हम यह सब कर रहे हैं।' और, मजबूरी वास्तव में कभी मजबूरी होती नहीं है। मजबूरी डर होती है, मजबूरी अज्ञान होती है, और मजबूरी लालच होती है। मजबूरी जैसी कोई बात ही नहीं होती न।
मजबूरी के लिए क्या शब्द है? 'विवशता' या 'परवशता’। जब आप कहते भी हो कि आप दूसरे के वश में हो, तो आप दूसरे के वश में थोड़े ही होते हो, आप अपने ही लालच के वश में होते हो।
तो विवशता तो शब्द ही झूठा है। कोई विवश कभी नहीं होता। कोई-न-कोई चीज़ होती है जिसको बचाने का लालच होता है, जिसकी ख़ातिर हम समझौता कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं मजबूरी’! तुम जो चीज़ बचाना चाहते हो उसको बचाने का मोह छोड़ दो, फिर बताओ कौन मजबूर कर सकता है तुमको?
धर्म हमेशा एक चुनाव होता है। आप किसी धार्मिक आदमी के पास जाएँ, आप पूछें उससे कि तुम धार्मिक क्यों हो? तो वो ये नहीं कहेगा कि 'मैं मजबूर हूँ, बापू ने कान उमेठ कर धार्मिक बना दिया।' ऐसे नहीं कहेगा, वो कहेगा– 'बात समझ में आ रही है, मेरी जाग्रत चेतना का चुनाव है धार्मिकता।'
ठीक है?
'मेरी जाग्रत चेतना का बुलंद चुनाव है धार्मिकता। डंके की चोट पर मैंने चुना है और, और कुछ मैं चुनना चाहता नहीं। मैं नहीं कह रहा (कि) मेरी मजबूरी है। मैं चाहता ही नहीं चुनना कुछ और।'
और जो लोग उल्टा-पुल्टा जीवन बिता रहे हों उनके पास आप जाएँ तो उनके पास सौ कहानियाँ होंगी। कहेंगे— नहीं, देखो बात तो पता है लेकिन, किन्तु, परन्तु, इफ..।
सुना लो यार क़िस्से, किसी को क्या फ़र्क पड़ना है! तुम्हारी ही ज़िंदगी है। जो भी तुम बना रहे हो दूसरे को, (वास्तव में) ख़ुद को ही बना रहे हो। बनाये जाओ उससे भी बहुत फ़र्क पड़ना नहीं है। ये क़िस्सा भी उसी दिन तक तो सुनाओगे न जिस दिन तक जी रहे हो। उसके बाद न तुम, न तुम्हारे किस्से! तो तुम कौनसा पहाड़ तोड़े दे रहे हो झूठी ज़िंदगी जी कर भी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैन में हैं एक ग़लत और घटिया जीवन जी कर भी, तो आप किसी को कितनी भी सफाई दे लें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
“मजबूरी वास्तव में कभी मजबूरी होती नहीं है। मजबूरी डर होती है, मजबूरी अज्ञान होती है, और मजबूरी लालच होती है।”
YouTube Link: https://youtu.be/QD7zNl4SIwQ