ब्रह्मलीन होने का अर्थ क्या है? || योगवासिष्ठ सार पर (2018)

Acharya Prashant
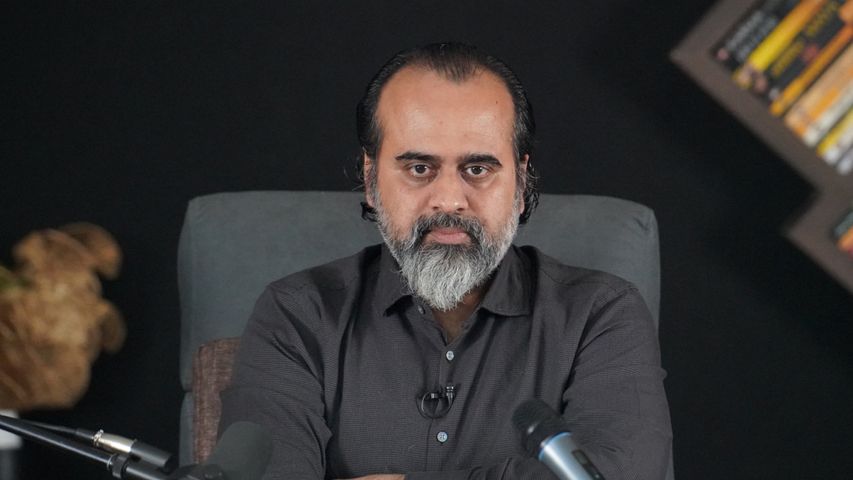
प्रश्नकर्ता: प्रणाम, आचार्य जी। आज के पाठ से अध्ययन का आनंद हुआ। कैसे हुआ, किसे हुआ, यह नहीं कह सकते, बस आनंद ही था। जब हम केवल ब्रह्म-अनुभूति में रम जाते हैं, मन अमन होता है, तब भी संसार का व्यवहार तो द्वैत में ही होगा, मान्यताएँ भी होंगी, वृत्तियाँ भी होंगी। तो मुक्त कौन होगा जब बंधन ही नहीं है?
इस संसार का भोग करते हुए, ब्रह्म में निष्ठा रखते हुए जीना सहज है व आनंदपूर्ण है। सारे ही सवाल इस एक बात पर ख़त्म हो जाते हैं कि सब ब्रह्म है। जानने वाला, क्रिया, कर्ता, भोक्ता, सब ब्रह्म ही है। कहीं भी जो कुछ हो रहा है, सब कुछ ब्रह्म ही है। अहोभाव! धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद!
आचार्य प्रशांत: सारे सवाल किसी जवाब पर नहीं ख़त्म होते। सवाल बस यूँ ही ख़त्म होते हैं। जब तक कोई जवाब शेष है, उसके बाद अगला सवाल खड़ा होना पक्का है, भले ही उस जवाब में ब्रह्म सम्मिलित हो। जवाबों को ख़त्म होना पड़ेगा, यहाँ तक कि ब्रह्म को लिए हुए जो जवाब हैं, उन्हें भी ख़त्म होना पड़ेगा।
ब्रह्म को आया, उतरा तब जानिए जब ब्रह्म स्वयं ही विलीन हो जाए। जब तक ब्रह्म की ज़रा भी धारणा है, आशा है—चाहे ब्रह्म में निष्ठा ही है—तब तक ब्रह्म से मन की एक काल्पनिक दूरी बनी हुई है।
ब्रह्म का कोई उपयोग नहीं है। ब्रह्म का आप इतना सा और यह उपयोग भी नहीं कर सकते कि ब्रह्म को किसी प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रयुक्त कर लें, वो भी संभव नहीं हो पाएगा। संभव होता दिखेगा ज़रूर क्योंकि ब्रह्म की धारणा भी बड़ी बलवती है। कितने ही सवालों का बौद्धिक समापन हो जाएगा ज्यों ही आप ब्रह्म की धारणा को प्रयुक्त करेंगे—बौद्धिक समापन; पूर्ण विसर्जन नहीं, पूर्ण अंत नहीं। ब्रह्म को भी खत्म होना होगा।
भूलिएगा नहीं कि ब्रह्म ने ‘ब्रह्म’ की कभी कोई बात नहीं करी। जब तक मनुष्य है, तब तक ‘ब्रह्म’ शब्द है। इसीलिए ऋषियों ने फ़िर दो फाड़ करके बताए: शब्द-ब्रह्म और पार-ब्रह्म। एक ब्रह्म वो जिसका होना इंसान पर निर्भर नहीं करता और एक ब्रह्म वो जो इंसान का कृतित्व है। प्यारा कृतित्व है, गहरा कृतित्व है, लेकिन है इंसान का; उसकी हस्ती कीमती है, उपयोगी है, पर उसी दिन तक है, जिस दिन तक इंसान है। जिस दिन आप चले गए, उस दिन कौन करेगा ब्रह्म-चर्चा? वास्तविक ब्रह्म का कोई उपयोग नहीं हो सकता। शब्द 'ब्रह्म' उपयोगी है।
आप कहते हैं, "इस संसार का भोग करते हुए, ब्रह्म में निष्ठा रखते हुए जीना सहज है व आनंदपूर्ण है।” हाँ, है। थोड़ा सा बस सतर्क, सावधान रहिएगा। कहीं ब्रह्म भोग का बहाना न बन जाए। हमारा तो कुछ ऐसा है कि हम अपनी निष्ठाएँ भी अपनी सुविधा के अनुसार चुन लेते हैं। ब्रह्म ज़रा अनुकूल लगा तो निष्ठा रख लेंगे। अच्छा है कि ब्रह्म में निष्ठा हो, अच्छा है कि संसार की अपेक्षा ब्रह्म में निष्ठा हो, और अच्छा है यदि आप निष्ठाहीन ही हो जाएँ, किसी में न बचे निष्ठा।
मन के पास पकड़ने के लिए कुछ ऐसा ही होता है सदा जो मानसिक हो। मन मन का कुछ पकड़ सकता है। मन में जो कुछ आया होगा, या तो वो प्राकृतिक होगा या मनुष्य का कृतित्व होगा, अन्यथा क्या आएगा मन में? तो मन में यदि ब्रह्म के प्रति निष्ठा आ रही है तो ऐसी निष्ठा के प्रति थोड़ा सावधान रहिएगा।
वास्तविक निष्ठा में निष्ठा का ख़याल नहीं करना पड़ता। आप ब्रह्मनिष्ठ हुए, ऐसा तब जानिए जब ‘निष्ठा’ शब्द आपके व्याकरण में ज़रा कहीं नीचे दब जाए। जब ज़रूरत पड़े तो मेहनत करके उसको खोद के निकालना पड़े। भूल जाएँ सब कुछ, “कौन ब्रह्म? कैसी निष्ठा? कुछ याद नहीं। सामने जो है, वो याद है; सामने चाय का प्याला रखा है तो याद है; सामने कुछ नोट रखे हैं तो याद है; सामने कोई आदमी है तो उसकी स्मृति है। तात्कालिक जो कर रहे हैं सो याद हैं, जो करना बाकी है सो याद है, और ये सब छोटी-छोटी बातें हैं जो याद हैं। इनसे कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा, ऐसा हमें कुछ याद नहीं।” ब्रह्म बहुत बड़ा है।
मन की एक बात समझ लीजिए। मन में जो कुछ होता है, वो मन में मौजूद बाकी सामग्री से अन्तर्सम्बन्धित हो जाता है। प्रयोग करके देखिएगा, आप ऐसा कर नहीं पाएँगे कि आप कोई नई वस्तु देखें और उसका सम्बन्ध पुरानी देखी हुई वस्तुओं से न बैठाएँ। आप ऐसा कर नहीं पाएँगे कि आपके सामने कोई तथाकथित नया विचार, या नई धारणा या नया दर्शन लाया जाए और आप उसका सम्बन्ध पुराने पढ़े-लिखे, देखे से न बैठाएँ। आप बैठा लेंगे, मन की आदत है।
मन चाहता है कि नए को पुराने की दृष्टि से देखे। कुछ नया सा आता है तो उसको पुराने के सन्दर्भ में परिभाषित कर देता है, ये आदत है मन की। आप ब्रह्म को मन में लेकर आएँगे, देखिए क्या हो जाएगा। बहुत बड़े को मन छोटे के सन्दर्भ में परिभाषित कर देगा। और छोटे को आधार बनाकर जिसकी परिभाषा हो सकती है, वो कितना बड़ा होगा? छोटे की तुलना में बड़ा हो सकता है, अपेक्षतया बड़ा हो सकता है, वास्तव में नहीं बड़ा हो सकता।
ब्रह्म को मन में लाएँ ही नहीं। आप उसे मन में लाए नहीं कि बहुत छोटा हो गया, कि जैसे हाथी चूहेदानी में आ गया। छोटा तो हो ही गया, बाकी चूहों से उसकी जात भी मिल गई। मन की चूहेदानी में बहुत सारे छोटे-छोटे चूहे थे और ले आए आप हाथी को भी चूहेदानी में। मन तुरंत इस तथाकथित नए हाथी की जात मिला देगा पुराने चूहे-चुहियों से। बेचारा ब्रह्म, फँस गया!
तो ब्रह्म को ब्रह्म रहने दें। आप अनादित हैं, इतना काफी है, उसी को ब्रह्म जानिए। आनंद है न? बस बहुत है। क्या करना ब्रह्म का? जिस दिन आनंद पर बादल पड़ता दिखे, जिस दिन आनंद डूबता सा दिखे, उस दिन ब्रह्म को याद कीजिएगा। जब तब आप आनंदित हैं, तब तक ब्रह्म याद में नहीं आएगा; क्योंकि ब्रह्म है। ब्रह्म भेजे में, स्मृति में नहीं आएगा क्योंकि ब्रह्म ह्रदय में है। जिस दिन आपका आनंद क्षीण पड़ने लगे, उस दिन लौटिएगा ब्रह्म के पास क्योंकि उस दिन लौटने की ज़रूरत होगी। जब हो आनंदित, तब ब्रह्म की बात करें तो आनंद पर जैसे बट्टा लगता है।
हाँ, आपने ठीक कहा कि ब्रह्म में रम जाते हैं। ब्रह्म-अनुभूति में नहीं रमते, ब्रह्म में रमते हैं। हाँ, ब्रह्म में रमना संभव है, ब्रह्म में रमना स्वभाव है, वो बिलकुल हो सकता है। आपने कहा कि तब भी संसार का व्यवहार तो द्वैत में ही होगा, मान्यताएँ भी होंगी, वृत्तियाँ भी होंगी—सब होता है बस बात ज़रा बदल जाती है।
आप क्रोध में होते हैं, आवेश में होते हैं, आवाज़ तो तब भी होती है, कर्म तो तब भी होते हैं, दुनिया तो तब भी होती है। आप प्रेम में, आनंद में होते हैं, आवाज़ तो आपके पास तब भी होती है, कर्म तब भी होते हैं, दुनिया तब भी होती है—पर सब बदल जाता है, कुछ महीन सा बदल जाता है।
भूखे आदमी की आँखों में और तृप्त आदमी की आँखों में कुछ तो अंतर होता है न? कुछ बदल जाता है। देखती वो दोनों आँखें संसार को ही हैं पर देखने में कुछ बदल जाता है। ब्रह्म में रमे हुए आदमी की आँखें जिस दुनिया को देखती हैं, वो दुनिया अलग होती है—दिखती ही भर नहीं है अलग, अलग हो ही जाती है। और ब्रह्म से विलग, भूखे आदमी की आँखें जिस दुनिया को देखती हैं, वो दुनिया अलग होती है।
जो दृश्य है, वो तो द्वैतात्मक ही है, कोई इसमें संदेह नहीं। अलग-अलग वस्तुएँ दिख रही हैं, संसार दिख रहा है; कुछ चलायमान है, कुछ अचल है, लोग, जानवर, सड़कें, यही सब दिख रहे हैं, पर फ़िर भी कुछ बदल जाता है। तो आप कहें यदि कि ब्रह्म में रमने के बाद भी संसार का व्यवहार वैसा ही चलेगा आपके लिए जैसा कि पूर्व में चलता था, तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बदल जाता है।
मेरे पास एक सज्जन थे, बात हो रही थी उनसे। तो उन्होंने एक ज़ेन कहानी का हवाला दिया। वो बोले कि वो कहानी एक आलोकित, सम्बुद्ध भिक्षु के बारे में है। उससे पूछा गया कि ज्ञान से पहले, निर्वाण से पहले तुम क्या करते थे? कैसा रहता था तुम्हारा दिन? तो कहता है, “क्या करता था? सुबह उठता था, नित्य कर्म से निवृत होता था, फ़िर लकड़ी काटने जाता था, लकड़ी को बाज़ार में बेच देता था, फ़िर जो पैसा मिलता था, उससे खाना खरीदता था, खाता था और आकर सो जाता था।”
"अच्छा, तो मतलब साधारण सा जीवन था तुम्हारा। और ज्ञान के बाद अब जीवन कैसा है? अब रोशनी जल गई है, अब तो सब बदल गया होगा?"
तो वो भिक्षु लकड़हारा बोला, "हाँ, सब कुछ बदल गया है।" नहीं, वो नहीं बोला। कहानी यह बात इतनी स्पष्ट, स्थूल रूप से कहती नहीं। वो लकड़हारा सिर्फ इतना बोला, "अब सुबह उठता हूँ, नित्य क्रिया से निवृत्त होता हूँ, कुल्हाड़ी उठाता हूँ, जंगल जाता हूँ, लकड़ी लाता हूँ, फ़िर बाज़ार जाता हूँ, बेचता हूँ, भोजन खरीदता हूँ, खाता हूँ और सो जाता हूँ।” कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।
तो जिनसे मेरी बात होती थी, वो बोले कि देखिए कि इससे यही तो सिद्ध होता है न कि ज्ञान के पूर्व और ज्ञान के पश्चात आप जैसा जीवन जी रहे होते हो, उसमें कोई अंतर थोड़े ही आता है? वो और कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपने न बदलने के पक्ष में दलील तैयार कर रहे थे। वो मुझसे वास्तव में कह रहे थे कि “मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ, बोध पश्चात भी ऐसा ही जियूँ तो भी आप मुझे बुद्ध मानना।”
अभी उनके जीवन में कई तरह के दूषण थे। उनका धंधा ही ऐसा था कि जिसमें तमाम तरह की छुपी हुई हिंसा थी और लालच था, कदम-कदम पर भय था, लेकिन मुनाफा खूब था। अब मुनाफा वो छोड़ना नहीं चाहते थे और बुद्धत्व भी प्यारा लगता था, तो उन्होंने इस कहानी को सहारा बनाया था। ये कहानी उन्हें बड़ी प्यारी लगी क्योंकि यह कहानी कह रही थी कि बुद्धत्व के उपरान्त भी तुम वैसा ही जीवन जी सकते हो जैसा तुम पूर्व में जीते थे।
तो उन्होंने कहा, “ठीक है, इसका मतलब मैं बुद्ध भी हो सकता हूँ और ये जो मुनाफा बनाता हूँ मैं अपने भ्रष्ट तरीकों से, ये मुनाफा भी कायम रह सकता है।” उन्होंने कहानी को दलील की तरह पेश किया मेरे सामने।
मैंने कहा, “देखिए, ये कहानी ऊपर-ऊपर की बात बता रही है और ऊपर-ऊपर की बात बिलकुल ठीक बता रही है। अंदर-अंदर सब कुछ बदल जाता है, और ऊपर-ऊपर भी बदलता है। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं बदला जाता।”
बोध से पहले वाल्मीकि अगर लुटेरे थे तो क्या बोध के बाद भी लुटेरे रहेंगे? हुआ था क्या ऐसा? राम से पहले तुलसीदास यदि एक साधारण, वासनाग्रस्त पति थे, तो क्या राम के बाद भी वो वैसे ही साधारण, वासनाग्रस्त पति रहेंगे? ऐसा हुआ था? बुद्ध से पहले अंगुलिमाल जैसा था, क्या बुद्ध के पश्चात भी वो वैसा ही रहेगा? तो ऊपर-ऊपर भी काफी कुछ कई बार बदल जाता है। कहानी का ध्येय बस यह बताना है कि ज़बरदस्ती मत बदलिए, बदल जाएगा ही। और अंदर-अंदर तो सदा सब बदलता ही है।
लकड़ी आप पहले भी लेकर आते थे जंगल से, लकड़ी आप अभी भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन लकड़ी लाने के तरीके में बड़ा अंतर आ जाएगा। अब आप नहीं चाहेंगे पेड़ों को कष्ट देना, अब आप नहीं चाहेंगे हरे पेड़ों को काट देना। पहले आपकी कुल्हाड़ी बेझिझक हिंसा करती होगी, अब आपकी कुल्हाड़ी किसी हरियाते पेड़ के प्राण नहीं ले पाएगी। अब आप देखेंगे कि कहीं कुछ सूखा सा पड़ा हुआ है, ख़त्म है, निर्जीव है, उसकी लकड़ी ले लेता हूँ।
तो आपने बस इतना पढ़ा कि जंगल गया और लकड़ी लेकर आ गया। कैसे लेकर आ गया? लकड़ी को अब वो कैसे छूता है, पहले कैसे छूता था? अब छूने में, अब उसके स्पर्श में प्रेम होगा। पहले उसके स्पर्श में छीना-झपटी थी, चीर-फाड़ थी ज्यों बलात्कार था। बड़ा अंतर आ गया है। फ़िर लकड़ी लेकर जाता है वो बाज़ार बेचने। आप कभी बाज़ार गए होंगे तो आपने विक्रेताओं में ज़मीन-आसमान का अंतर देखा होगा।
कबीर भी जुलाहे हैं, अपना कपडा रोज़ बाज़ार लेकर जाते हैं, बेचते हैं। आपको क्या लगता है, वो अन्य जुलाहों की तरह ही बेचते होंगे? कबीर बेचने में भी ज़रा कबिराई तो होगी न? कबीर यदि कपड़ों के विक्रेता हैं, तो उसमें भी कबीर की सुगंध तो होगी न? कितने श्लोक तो कबीर ने हाट में ही बोल दिए होंगे। ऐसा अन्य जुलाहे तो नहीं करते। कबीर जिसको कपड़ा देते होंगे, यकीन जानिए, उसको कपड़े के साथ-साथ राम भी दे देते होंगे। यह हो नहीं सकता कि कबीर किसी से मिलें और उस तक राम न पहुँचें। तो कबीर यदि कपड़ा भी किसी को देते हैं तो कपड़ा बहाना है, कपड़े के रेशे-रेशे में वो राम को छुपाकर दे रहे हैं। बड़ा फर्क है। सब बदल जाता है।
हाँ, ज़बरदस्ती का बनावटी बदलाव किसी काम का नहीं होता। बनावटी बदलाव के विरुद्ध वह कहानी कही गई जिसका अभी मैंने ज़िक्र किया। बनावटी बदलाव खतरनाक है, लेकिन बदलाव का बिलकुल ही न आना और भी खतरनाक है। आप मंदिर में जाने से पहले जैसे हैं, मंदिर में वैसे ही रह गए, गड़बड़ बात है। और आप मंदिर जाने से पहले जैसे हैं, मंदिर पश्चात भी वैसे ही रहे तो भी गड़बड़ बात है। सब बदलना चाहिए। गुरु से पहले जैसे थे आप, गुरु के बाद भी वैसे ही रह गए तो यह कोई उपलब्धि नहीं है। कायाकल्प तो होना है।
आपने कहा कि द्वैत रहेगा, धारणाएँ रहेंगी, वृत्तियाँ रहेंगी। न, उनका परिमार्जन हो जाता है। जैसे रसोई वही हो, पहले उसमें माँस पकता था, अब नहीं पकता; किसी ने रसोई को मंदिर बना दिया है। वृत्ति अभी भी है। पहले भी आपको सामाजिक संसर्ग अच्छा लगता था, लोगों से बात करना भला लगता था। अभी भी आपको लोगों से बात करना, सामाजिकता पसंद है, पर सब बदल जाएगा। पहले क्या बात करते थे? अब क्या बात करते हैं? पहले किससे बात करते थे? और अब किससे बात करते है? पहले कौन सा समाज खड़ा कर रखा था? अब कौन सा समाज खड़ा कर दिया? वृत्ति रहते हुए भी पूरी तरह बदल जाएगी।
द्वैत रहेगा? हाँ, रहेगा। आपने ठीक कहा कि द्वैत रहेगा। द्वैत का मतलब होता है 'मैं' और संसार, वो रहेगा। आप हैं, संसार है, बिलकुल है। पर संसार कभी पूरा तो आप देख नहीं पाते। अनंत विश्व है, कभी उसका पूरा पता नहीं। संसार का अपने मुताबिक एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हो, गौर करिएगा, अपने मुताबिक। तो ये होता है आपका द्वैतात्मक संसार, कि आप जैसे हो, उसी के अनुसार कुछ उठा लेते हो, वही आपको दिखाई पड़ता है।
भूखे थे आप, बाज़ार से गुज़रते थे। जो आपको बाज़ार में दिखाई दे रहा है, जहाँ-जहाँ आपकी नज़र रूकती है, जहाँ-जहाँ मन आपका जाकर बैठे, वही आपका संसार है। तो भूखे अगर आप और संसार से गुज़र रहे हो, तो क्या हुआ आपका संसार? कहाँ जाकर आपकी नज़र रुकेगी बार-बार? जितनी खाने-पीने की दुकानें होंगी, उन्हीं पर जाकर आपकी नज़र बार-बार रुकेगी।
द्वैत है, पर उसके द्वैत के केंद्र में, भूलना नहीं, कि तुम हो। तुम बदल गए तो द्वैत रहते हुए भी बदल जाता है। दृष्टि बदल गई तो जो दिखाई दे रहा है, वो बदल जाएगा; क्योंकि तुम बदल गए हो। और फ़िर तुम संतृप्त हो, अब पुनः बाज़ार से निकले, पेट भरा हुआ है, ह्रदय पूरा है, अब तुम्हें कुछ और दिखाई देगा। दिखाई जो देगा, द्वैत उसमें अभी भी शामिल है, पर तुम पूरे हो इसीलिए जो दिख रहा है, वो नया होगा; वो पहले नहीं था। द्वैत रहते हुए भी जीवन बदल गया न?
संसार तो कबीर को भी दिखाई देता है और साधारण संसारी को भी दिखाई देता है। तुम्हें क्या लगता है, दोनों को एक ही चीज़ दिखाई देती है? लेकिन संसार दिखाई दे रहा है तो द्वैत की प्रक्रिया तो घट रही है। देखने के लिए दृश्य और दृष्टा में ज़रा दूरी चाहिए, तो द्वैत तो है। कबीर देखें तो भी द्वैत है, आप देखो तो भी द्वैत है, लेकिन देखो कबीर को क्या दिखता है और आपको क्या दिखता है; क्योंकि देखने वाला परिष्कृत हो गया अब, देखने वाले का शोधन हो गया।
तो आपने द्वैत की बात की, बढ़िया किया। धारणाओं की बात की, बढ़िया किया। पर सतर्क रहिएगा कहीं ये बातें न बदलने का, वृत्तियों के, ढर्रों के कायम रहने का बहाना न बन जाएँ।
आपने कहा है धारणा। हाँ, धारणा रहती है। ‘मैं देह हूँ’, ‘मैं भूखा हूँ’, ‘मैं हिंसक हूँ', ये सब धारणाएँ हैं और सनातन धर्म अपना लें आप, तो वो भी धारणा है। धर्म की परिभाषा ही ये है – जो धारण किया सो धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य सो धर्म। तो धारणा तो है ही। आप हाथों में बन्दूक भी धारण कर सकते हैं और कठोपनिषद भी धारण कर सकते हैं। धारणा तो है, पर क्या धारण किया? अंततः सारी धारणाएँ हटानी हैं। बन्दूक हटानी है और एक तल पर जाकर कठोपनिषद को भी हट जाना है। तो बात ठीक है कि धारणाएँ तो सारी हटनी चाहिए, पर धारणा धारणा में भी अंतर होता है।
कोई तन पर यज्ञोपवीत धारण किए हुए है और कोई गोलियों का पट्टा। चमड़े का पट्टा देखा है कैसे धारण किया जाता है? उसमें गोलियाँ-ही-गोलियाँ रहती है। एक ही जगह धारण किए जाते हैं दोनों, पर धारणा धारणा में कितना अंतर है? किसी ने मुखौटा धारण किया, किसी ने संन्यास। संन्यास भी एक धारणा ही है, पर धारणा धारणा में बड़ा अंतर है।
तो जब ब्रह्म में रत हो जाते हो तो वृत्तियाँ रहते हुए भी बदल जाती हैं, जैसे कि बंदा ऊपर-ऊपर से वही दिखता हो और अंदर-अंदर से पूरा बदल गया हो, ऊपर-ऊपर से वैसा ही दिखेगा।
बुद्ध के पश्चात भी अंगुलिमाल का कद तो नहीं बढ़ गया होगा, पीठ तो पीठ जैसी ही होगी। ऊपर-ऊपर से तो वैसा ही दिखता होगा जैसा पहले दिखता था, पर अंदर-अंदर से जैसे सब बदल गया, जैसे किसी ने उसकी आँतें, जिगर, यकृत, मस्तिष्क सब बाहर निकाल लिया हो और सब नया लगा दिया हो, जैसे गाड़ी की चेसिस छोड़कर भीतर के सारे कलपुर्ज़े बदल दिए गए हों।
ज़बरदस्ती मत बदलिएगा और बदलाव का विरोध भी मत करिएगा यह कहकर कि द्वैत को तो बने ही रहना है। बदलाव आएगा, पूरा आएगा, ऐसा बदलाव आएगा कि द्वैत में अद्वैत खड़ा हो जाएगा।
दो तरह के होते हैं द्वैत: एक जो सिर्फ द्वैत होता है और द्वैत ऐसा भी होता है जिसके ऊपर अद्वैत का आशीर्वाद होता है। उपनिषद् कहते हैं: “ब्रह्म विश्व की पूँछ की तरह है, ऐसी पूँछ जो विश्व को सहारा देती है, विश्व को बने रहने में मदद करती है, स्टेबिलिटी (स्थिरता) देती है।” तो एक द्वैत ऐसा भी होता है जिसकी पूँछ की तरह अद्वैत पीछे-पीछे चला आए।
अभी मुझसे बात कर रहे हो, ये घटना द्वैत में ही घट रही है न? एक वक्त, एक श्रोता, तो हो गया द्वैत, हो गया कि नहीं? पर ये ऐसा द्वैत है जिसकी पूँछ में अद्वैत लगा हुआ है। तुम भीतर तो घुसने देते हो द्वैत को, कि एक वक्ता होगा, एक श्रोता होगा; एक गुरु होगा, एक चेला होगा। तुम सोचते हो कि दूजापन कायम रहेगा?
दो रहेंगे, शुरुआत तो जब होती है तो दो रहते ही हैं। पर तुमने जिस जीव को प्रविष्टि दी है, वो अपनी पूँछ साथ लेकर आएगा न? या ऐसा होता है कि कुत्ते को आना देते हो और वो पूँछ अपनी छोड़ आता है? तुम तो उसका मुँह भर देखते हो, कहते हो, “अच्छा मुँह है, सुन्दर है, मोहक। आ जा।” पीछे-पीछे क्या आ गई? पूँछ। ऐसा ही एक द्वैत होता है। गुरु के साथ बैठते हो, शुरुआत द्वैत से होती है लेकिन पूँछ की तरह क्या आ गया चुपके से? अद्वैत।
ऐसे ही वृत्तियाँ भी होती हैं। वृत्ति भी ऐसी हो सकती है कि निवृत्ति का द्वार बन जाए। ग्रंथों से प्रेम हो गया, ये भी वृत्ति ही है। गुरु से लगाव लग गया, ये भी वृत्ति ही है। पर ये ऐसी वृत्ति है जो निवृत कर देगी। दुनिया से मन जोड़ बैठोगे अगर तो दुनिया तुम्हारा मन पकड़े ही रहेगी, एक जगह जोड़ोगे, सौ जगह जुड़वाएगी। और कोई ऐसा भी होता है जिससे मन जोड़ा अगर तो वो बाकी सब जगह से तो मन को छुड़वा ही देगा, अपने पास भी लगने नहीं देगा; ऐसा जुड़ाव जो निवृत्ति का साधन बन गया।
द्वैत की पूँछ अद्वैत हो सकता है। वृत्ति की पूँछ निवृत्ति हो सकती है। ग्रन्थ कितना बोलते हैं: जपो माला रे, लगे रहो, अभ्यास करो। कृष्ण कितना समझा रहे थे न अभ्यास, याद है? अब अभ्यास क्या है? देखोगे गौर से तो उसमें भी वृत्ति सम्मिलित है, पर करोगे अभ्यास तो निवृत हो जाओगे। तो बदलेगा, सब बदलेगा, वृत्तियों का पूरा प्रारूप बदल जाएगा।
संतों की भी आदतें होती हैं, जानते हो? आदत और वृत्ति एक ही कोटि की चीज़ें हैं। पर उनकी वृत्तियाँ ऐसी होती हैं कि उनसे संसार को लाभ मिलता है। एक सूफी फ़कीर था, उसकी वृत्ति थी कि जब तक दो मील-चार मील में जितने भूखें हैं, वो खा नहीं लेंगे, तब तक मुझे पचेगा ही नहीं। और उसने ये रोज़ का कार्यक्रम बना रखा है। अभ्यास ही है एक तरह का, पर देखो कैसी वृत्ति है? और एक वृत्ति ये होती है कि जब तक दो मील-चार मील में किसी-न-किसी को दुःख न दे दूँ, तब तक मुझे खाना पचेगा नहीं। वृत्तियाँ तो दोनों हैं न? पर एक वृत्ति तुम्हें भी निवृत कर देगी और संसार को भी और दूसरी फँसाए रखेगी।
कबीर भी ऐसे ही करें। उनके घर कोई आए तो उसका खाकर जाना पक्का है। फ़िर उसी बात को लेकर आगे कहानी है कि खाना नहीं था, ताने पड़े। तो कमाल को लेकर निकले तो किसी ने पूछा कहाँ जाते हो? तो बोले, “चोरी करने,” बड़ी बेतकल्लुफ़ी से। फँस गए, फ़िर जादू। संतों की वृत्तियाँ हैं मीठी। उनकी कथाएँ भी मीठी, बड़ा रस देती हैं।
यह कुतर्क मत कीजिएगा कि आदत, आदत एक बराबर और क्रोध, क्रोध एक बराबर। न, आदत, आदत में बड़ा अंतर होता है। फ़िर कह रहा हूँ, संतों की, सूफियों की, ऋषियों की कहानियाँ पढ़िए, उन सबकी भी व्यक्तिगत खूबियाँ मिलेंगी, उन सब में भी व्यक्तिगत गुण अभी विद्यमान थे। प्रकृति से तीनों गुणों से हट नहीं गए थे वो। दुर्वासा का गुस्सा देखा है? परशुराम का गुस्सा देखा है?
बुल्लेशाह की तड़प देखी है? उनको निकाल दिया गया आश्रम से क्योंकि गुरु नाराज़ हो गए थे। अब वो तड़पे जाएँ। जानते हो क्या किए? सड़क पर स्त्रियों के कपड़े पहनकर नाचने लगे। कुछ तो करना है न कि गुरु को लुभाया जाए। तर्क जितने दे सकते थे, दे लिए, क्षमा जितनी माँग सकते थे, माँग ली, लेकिन इनायत शाह मानते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि यही तरीका बचा है, अब यही तरीका आया उनकी बुद्धि में, और कोई तरीका वास्तव में बचा भी नहीं था। तो स्त्रियों के कपड़े लिए, पहन लिए और भेष बदलकर आश्रम में घुस गए। वैसे मनाही कर दी गई थी कि ये घुसे न अब, इसकी शक्ल न दिखाई दे। औरत बनकर घुस गए, फ़िर वहाँ लगे नाचने। इतना नाचे, इतना नाचे कि माफ़ी पा गए। अब इसमें दिल में कसक तो उठी होगी, दर्द भी हुआ होगा, रोए भी होंगे।
मन है, अमन नहीं हो गया। संत के पास भी मन होता है। बहुत रोता है वो, अमन नहीं हो गया। इस चक्कर में मत फँस जाइएगा। उसे भी चोट लगती है, वो भी प्रफुल्लित होता है, वो भी उदास होता है।
मन में यह चित्र न बैठा लीजिएगा कि दो हो अवस्थाएँ है: या तो सब शून्य हो जाए या फ़िर ज़िन्दगी वैसी ही चलती रहे जैसी चल रही थी। नहीं, नहीं, नहीं, इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी अवस्था भी है कि सब शून्य है नहीं, लेकिन शून्य से अभिप्रेरित है, कि अभी ऐसा भी नहीं हुआ है कि वृत्तियाँ हट गईं, जल गईं, निर्जरा हो गईं; वृत्तियाँ हैं, लेकिन उनमें एक खुशबू आ गई है। कि जैसे रामकृष्ण पूछते हों, “रसोई में क्या है?” अब ये क्या है? भजन के मध्य, दैनिक कार्यक्रम के मध्य एक महासंत, एक परमहंस रसोई की ओर चल पड़ता है। पर मिठास है, कुछ बात है।
अब मीरा को नाचना है और तुम कह दो, “तू बैठ जा महावीर की तरह।” न, अरे है उसमें स्त्रैण वृत्ति, भाई। वो उसी वृत्ति को कृष्णमय किए दे रही है। वृत्ति हट नहीं गई, पर वृत्ति कृष्णमय हो गई है। स्त्री हैं मीरा और उसका स्त्रीत्व साफ़ दिखाई देता है। आप मीरा के कथन देखें, आप बुद्ध के वक्तव्य देखें, पता चल जाएगा कि पुरुष का कौन सा है और स्त्री का कौन सा है। लेकिन मीरा ने अपने स्त्रीत्व को कृष्ण के रंग में रंग दिया है। अब वो पवित्र हो गया, अब वो धुल गया, अब उसमें कोई रज नहीं बचा।
तुम गुरु गोबिंद सिंह की वाणी सुनो। वहाँ तोपें गरज रही हैं, वहाँ तलवारों की खनक है, लेकिन फ़िर भी कितनी भक्ति है, कैसी श्रद्धा है! देवी को पूजते थे, निराकार के भी उपासक थे। पर जैसा वो जीवन जी रहे हैं योद्धा का, वो भी उनकी वाणी में साफ़ दिखाई देता है। तुम परमहंस को यह कहता नहीं पाओगे कि सवा लख से एक लड़ाऊँ, गुरु गोबिंद सिंह कहेंगे।
यह तर्क भी खूब चलता है। एक सज्जन आए, बोले, “देखिए, कृष्णमूर्ति ने हमें समझाया है कि आदत, आदत एक बराबर, डर, डर एक बराबर। हमें बताया गया है कि किसी भी प्रकार का डर गड़बड़ है।” मैंने कहा कि नहीं, कृष्णमूर्ति यदि होते यहाँ पर तो वो तुमको बताते कि यह नहीं कहा उन्होंने। जाकर पूछो कबीर से जो तुमसे बार-बार कहते हैं कि एक भय ज़रूर रखना। जाकर पूछो तुलसी से, वो भी यही कहते हैं कि एक भय ज़रूर रखना। जाकर पूछो कुरआन से जो तुमसे कहती है, “अल्लाह से डरो।”
डर, डर बराबर नहीं होते; आदत, आदत बराबर नहीं होते; वृत्ति, वृत्ति बराबर नहीं होती; क्रोध, क्रोध बराबर नहीं होता; धारणा, धारणा बराबर नहीं होती।
दीवाली की रात घुघ्घू सिंह जुआ खेलने गए। अब घुघ्घू सिंह तो घुघ्घू सिंह हैं, वो जुआ भी घुघ्घू की तरह ही खेलते हैं, तो हार गए। चूँकि घुघुआते हुए गए तो जेब में ज़्यादा पैसा नहीं था। जितना हारे, उतना अदा करने के लिए, पूरा करने के लिए पॉकेट (जेब) खाली। तो जिनके साथ खेल रहे थे, उनसे एक चांटा पाए, पटाक। फ़िर घुघ्घू सिंह चांटा खाके, गाल सुजाए घर वापस आए। वहाँ बापराम तैयार खड़े थे, बोले, “तू था कहाँ?” पकड़ ली गर्दन घुघ्घू सिंह की तो घुघ्घू घुघुआने लगे। सारी बात उलीच दी तो बापराम ने दबाकर एक थप्पड़ दिया दूसरे गाल पर। अब इधर वाला गाल भी पाँच उँगलियों का निशान लिए हुए और इधर वाला भी, दायाँ-बाँया दोनों। थप्पड़ थप्पड़ में अंतर होता है।
संसार तुम्हें खूब सजा देता है। “ये संसार काटन की बाड़ी, उलझ-उलझ मर जाना है।” संसार खूब सज़ा देता है, थप्पड़-ही-थप्पड़, और गुरु भी सज़ा देता है। पर जुए वाले यार और बापराम के थप्पड़ में अंतर होता है।
इस चक्कर में मत पड़ जाना कि जो प्रेमी है, वो थप्पड़ कैसे मारेगा? हमें तो बताया गया है हिंसा, हिंसा एक बराबर होती है। फ़िर तुम हिंसा का अर्थ ही नहीं समझे; फ़िर तुम हिंसा का बड़ा सतही अर्थ जानते हो। सूजा दायाँ गाल भी है और बाँया भी, पर सूजन, सूजन में फ़र्क है। दवाई शायद दोनों पर एक ही लगे, पर सूजन, सूजन में फर्क है, है कि नहीं है? अब तुम घुग्घूमल होगे तो नहीं समझ पाओगे इस बात को, पर बापराम का थप्पड़ काम कर गया होगा तो समझ जाओगे।