न धैर्य न विवेक न निर्भयता || आचार्य प्रशांत, ऋषि अष्टावक्र पर (2014)

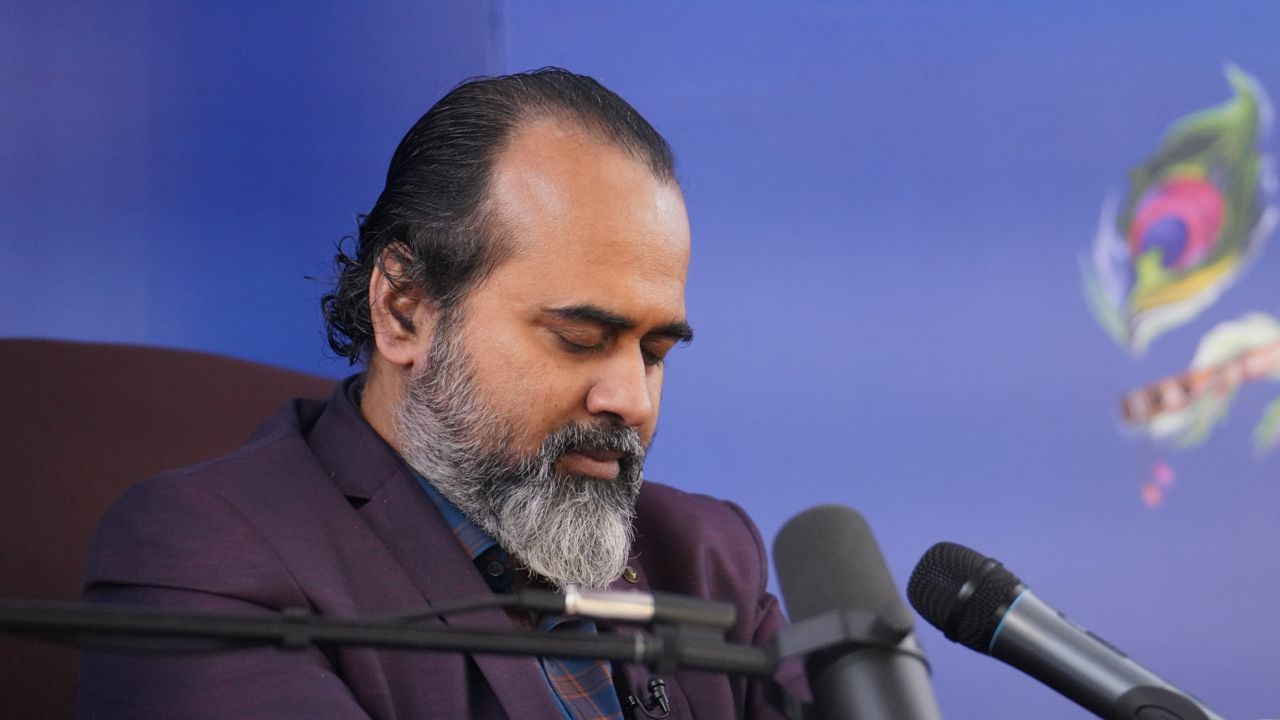
क्व धैर्यं क्व विवेकित्वं क्व निरांकतापि वा |
अनिर्वाच्यस्वभावस्य नि:स्वभावस्य योगिनः ||
(अष्टावक्र गीता अध्याय १८ , श्लोक ७९)
वक्ता: कुछ बड़े अद्भुत शब्द हैं जिनका प्रयोग किया गया है, लिख लेते हैं उन शब्दों को जिनके बारे में अष्टावक्र बात कर रहे हैं:
धैर्य
विवेक
निर्भयता
अनिर्वाच्य स्वभाव
निःस्वभाव
जो पहले तीन शब्द हैं, जो पहले तीन गुण हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं कि योगी उनसे सर्वथा मुक्त होता है। क्या करेगा धीरज का योगी? धीरज तो तब धरा जाता है जब कामना हो, कामना के उठने और कामना के पूरे होने में जो अंतराल होता है उसमें मन की जो अवस्था होती है उसका नाम होता है धीरज। कुछ भी नहीं धर्ता उसका मन, तो धैर्य क्या धरेगा? धर्य का अर्थ ही है कुछ धरना। कुछ रखना, कुछ लिए हुए बैठना, कुछ बोझ होना। कुछ नहीं धरना, कोई धैर्य नहीं। लेकिन बड़ी दिक्कत है, हमें यूँ संस्कृत किया गया है कि धीरज बड़ा अच्छा गुण है। धैर्य का हमें बड़ा मूल्य बताया गया है। और योगी के विषय में क्या कहते हैं अष्टावक्र, कि धीरज जैसी कोई चीज़ उस पर लागू ही नहीं होती। क्यों धरे वह धीरज, जो है सो अभी है, जो नहीं है तो नहीं है? भविष्य उसके लिए है ही नहीं तो, धीरज का प्रश्न कहाँ उठता है?
श्रोता १: धीरज वहाँ भी तो आता है कि आपने मुझसे कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, या तो मैं जवाब दूँ, या मैं चुप करूँ, अगर मैं चुप कर गयी तो पास वाले कहेंगे कि इसने धैर्य दिखाया।
वक्ता: हमने धीरज का अर्थ यही कहा कि कामना है और अभी से लेकर कामना की पूर्ती तक में जो अंतराल है वहाँ पर मन की अवस्था का नाम धीरज है। आप अब ही न पलटकर वार करो पर धीरज का अर्थ ही यही है कि इच्छा मन में बैठी हुई है। अभी नहीं करोगे तो कभी और करोगे, कर के रहोगे। इच्छाओं को काटता, इच्छाओं का विगलन तो सिर्फ बोध करता है। धीरज तो इच्छा को सिर्फ बैठा देता है, ‘अभी बैठ, कभी और उठना’। इच्छा कहीं चली नहीं गयी है धीरज से, इच्छा पर प्रकाश नहीं पड़ गया है कि वह तिरोहित हो जाए। क्या हुआ है इच्छा के साथ? वह बैठा दी गयी है, स्थगन हो गया है उसका, एक तरह का पोस्टपोंमेंट है वह। तो इसलिए धीरज को बड़ा मूल्य मत दे देना, कष्ट है धीरज। कौन धीरज में आनंदमय हो सकता है? कष्ट है वो।
श्रोता २: श्रद्धा में धीरज नहीं है?
वक्ता: श्रद्धा में तो यह भाव है कि ‘है ही’, इंतज़ार नहीं है। धीरज में तो प्रतीक्षा है, समय है। श्रद्धा में समय नहीं है, श्रद्धा में ‘है ही, अभी’, होगा नहीं ‘है’। श्रद्धा ‘होगा’ की बात नहीं करती है, मन ‘होगा’ की बात करता है। जहाँ होगा है वहाँ पड़ेगी ज़रुरत धीरज की। अब हमने मूल्य की बात की थी कि किस तरीके से जब मूल्य गड़बड़ाते हैं तो मन पूरा गड़बड़ा जाता है। धीरज को लेकर के जो हमें पट्टी पढ़ाई जाती है वह अच्छा उदाहरण है इस बात का, कि किस तरह से गलत मूल्य हमारे भीतर बैठा दिए गए हैं। धीरज में कुछ नहीं रखा है।
श्रोता १: यह कैसे कह सकते हैं कि गलत मूल्य बैठा दिए गए हैं?
वक्ता: जो भी कुछ समय में होगा और आप उसे मूल्यवान समझने लगोगे, वहीँ आप उस से दूर हो जाओगे जो समयातीत है, जो समय का स्रोत ही है। समय तो माया है और ज्यों ही आप धीरज को मूल्य देते हो, आपने समय को मूल्य देना शुरू कर दिया। ज्यों ही आपने समय को मूल्य दिया, त्यों ही आपने माया को मूल्य दे दिया, अब आप समय में भटकोगे। धीरज का अर्थ है समय में भटकना। अब आप वहाँ प्रतिष्ठित नहीं हो जो समय का स्रोत है।
श्रोता १: तो धीरज, समय को मूल्य देना है।
वक्ता: बिल्कुल! जहाँ धीरज को मूल्य दिया गया वहाँ समय को मूल्य दिया गया, वहाँ कामना को मूल्य दिया गया।
श्रोता २: और यह धार्मिक नहीं है।
वक्ता: दूसरा शब्द है, जो योगी के सन्दर्भ में प्रयुक्त है, वह है विवेक। अब तो बड़ी दिक्कत हो गयी। शंकराचार्य तक कहते हैं कि जो साधक हो उसमें विवेक का गुण ज़रूर होना चाहिए, और कहते हैं कि जो नित्य-अनित्य का भेद कर पाए उसमें ही विवेक है। और यहाँ अष्टवक्र कह रहे हैं, कैसा विवेक? करना क्या है विवेक का? अरे नित्य-अनित्य में भेद है ही नहीं। अनित्य, नित्य से ही तो उपजा है। जो कृष्ण कह रहे हैं, ‘मम् माया’, ‘क्या करूँगा मैं भेद करके, मेरी भेद बुद्धि ही ख़त्म ही गयी, मुझे कुछ अलग-अलग अब दिखता ही नहीं। कैसा विवेक? विवेक का तो अर्थ ही है अलग-अलग करना, विवेक का अर्थ ही है एक को न देख पाना, विवेक का अर्थ है टुकड़े करना, बांट देना, अंतर देखना, अरे हमें अब दिखता ही नहीं तो विवेक का क्या करेंगे, जहाँ देखते हैं तू ही नज़र आता है। विवेक तो छांटता है कि यह सत्य है और यह असत्य, हमारे लिए कोई असत्य अभी रहा ही नहीं, तुम असत्य कहते हो, हमें उसमें कारगुजारी सत्य की दिखाई देती है। जिसे तुम माया कहते हो हमें उसमें ब्रह्म दिखाई देता है, जिसे तुम नकली कहते हो, हमें उसमें भी असली दिखाई देता है, तो हम विवेक का क्या करेंगे? जित देखूं तित तू, अब यहाँ क्या करना है विवेक का?’
विवेक क्यों काट रहे हैं अष्टावक्र, क्योंकि विवेक का अर्थ है कि दो हैं; सत्य और असत्य। अष्टावक्र विवेक तो काट करके आपको संदेश दे रहे हैं कि दो नहीं हैं, एक है, अद्वैत है। जो जब उन्होंने धीरज को काटा तो क्या कहा? समय नहीं है।
और जब विवेक को काट रहे हैं, तो कह रहे हैं दो नहीं हैं, झूठ है। विवेक का तो अर्थ ही है कि झूठ को सच से अलग करो। और अष्टवक्र कह रहे हैं कि झूठ होता ही नहीं, सिर्फ सत्य की सत्ता है, तो विवेक कैसा? ‘जब तू ही तू पसरा हुआ है चारों ओर तो हम किसको कहें कि तू नहीं और कहाँ कदम रखें, कैसी सावधानी रखें, जहाँ ही चल दिए, जहाँ लेट गए, तू ही है। विवेक तो तेरा अपमान होगा, विवेक तो इस बात की घोषणा है कि जैसे तू अनुपलब्ध हो, जैसे तू अनुपस्थित हो। तू कहीं है ही नहीं अनुपस्थित।
अगला शब्द है, निर्भयता
निर्भयता तो तब प्रासंगिक होती है जब कहीं भय हो। यदि भय की कहीं छाया ही ना हो, तो निर्भयता शब्द ही अर्थहीन है। जब भय ही कुछ नहीं है, तो निर्भयता कैसे कुछ हो सकती है। निर्भयता तो बस इस बात की घोषणा है कि भय नहीं, भय झूठा, कि भय के पार भी कुछ है, तब निर्भयता के केंद्र में भय ही बैठा है। और यदि भय ही न हो तो?
देखिए होता क्या है। एक पायदान होता है जहाँ सब काट कर एक की सत्ता स्थापित की जाती है। एक सीढ़ी वह होती है, जहाँ शब्द झूठा है, उसको काट कर एक परम सत्य को स्थापित किया जाता है, मूलमंत्र वहाँ तक जाता है। भगवत गीता भी वहाँ तक जाती है, कृष्ण अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। वहाँ पर नानक उस अकाल को स्थापित कर रहे हैं। उसकी ज़रुरत तब पड़ती है जब आपने उस सबको काटा हो, उस सबको ठुकराया हो जो नकली है। जब बहुत कुछ जो नकली था उसे काटा जाता है तो किसी एक को, सच्चे को, स्थापित करना पड़ता है। पर जब आप उस सच्चे में ही बैठ जाते हो,वो सब जो नकली था वो है ही नहीं, तो अब आप उसे एक भी कैसे बोलोगे। एक की सत्ता प्रतिस्थापित करनी पड़ती है अनेक के विरुद्ध। जो मन अनेकों में भटका हुआ है, उसे सत्य की तरफ ले जाने के लिए ‘एक’ कहना बड़ा ज़रूरी है, ‘अद्वैत’ कहना बड़ा ज़रूरी है, ‘एक ओंकार’ कहना बड़ा ज़रूरी है। भला है कि एक ओंकार कहा गया। लेकिन, जब उस ओंकार में ही आप बैठ गए, अब और कुछ बचा ही नहीं, तो एक भी कैसे बोलोगे। एक बोलने के लिए दूसरा होना ज़रूरी है। ओंकार ही रह गया, तो एक भी नहीं, क्योंकि ओंकार अपने आप में एक नहीं है, ओंकार कुछ नहीं है। तो अष्टावक्र वहाँ से बोल रहे हैं, वह उस ओंकार में बैठकर ही बोल रहे हैं, उनका आसन है वहाँ पर, तो इस कारण वह कहते हैं, कि मुझे दूसरा दिखाई ही नहीं देता। कैसा विवेक? कैसी निर्भयता?
गुरुओं ने, शास्त्रों ने, कृष्ण ने, बड़ा काम किया जो भटकते हुए मन को ‘एक’ तक लेकर आये, पर जो मन एक में बैठ गया उसको अब एक जैसा बचता नहीं, क्योंकि एक भी क्या है, संख्या है। कैसी संख्या, कौन सी संख्या? संख्याएँ तो आकाश में होती हैं। सबसे छोटी संख्या है एक, पर है तो संख्या ही ना? सारी संख्याएँ गयीं, सारे भेद गए। सबसे छोटा भेद है ‘एक’, पर अब वो भी गया।
अगले दो शब्द जो अष्टावक्र ने लिए हैं, बड़े मज़ेदार हैं, पहले तो कहा ‘अनिर्वाच्य स्वभाव’ और फिर कह दिया ‘निःस्वभाव’।
अनिर्वाच्य स्वभाव का अर्थ, जिसके स्वभाव का कुछ ब्यौरा नहीं दिया जा सकता, कोई वचन नहीं किया जा सकता। जब भी कभी स्वभाव होगा, तब बताया जा सकेगा। जो कुछ भी होगा उसका वर्णन किया जा सकता है। आप जिस किसी को भी ‘है’ की, ‘होगा’ की संज्ञा देते हैं तो हमेशा इन्द्रियों और मन के दायरे की बात होती है। यदि कुछ है, तो वह अनिर्वाच्य नहीं हो सकता। अनिर्वाच्य मतलब, वचन वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जो भी समय में है, आकाश में है, वहाँ तक वचन पहुंचेगा, और निश्चित रूप से पहुंचेगा, आप कुछ न कुछ निकाल ही लोगे उसका वर्णन।
अनिर्वाच्य का मतलब, वह स्वभाव कुछ ऐसा है जो संसारी नहीं है, जो नाम रूप के दायरे में नहीं आता, जो मन की पहुँच से बाहर है। इसलिए कहते हैं, निःस्वभाव, वह स्वभाव है ही नहीं। उसमें व्यक्ति-परक कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी आपका है, मेरा है, हमेशा उसके बारे में कहा जा सकता है। जो कुछ भी विचारों में समां जाए, वह शब्दों में भी व्यक्त होकर रहेगा। पर सत्य ही है ऐसा जो न विचारों में समाता है, और न शब्दों में व्यक्त होगा। इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, अनिर्वाच्य है यह। आप जो भी कुछ कहेंगे वह कम पड़ेगा, या आप जो भी कहेंगे उसका विपरीत भी उतना ही सच होगा। आप कहेंगे, ‘वह बड़ा शांत है’, अगले दिन क्रोधित दिख जाएगा। अनिर्वाच्य! अरे, क्या बोलें, जो बोलते हैं झूठ हो जाता है। आप कहें, ‘कम खाता है’, एक दिन जाएँगे, तो खूब खा रहा होगा। आप कोशिश करेंगे उसे बांधने की, वह असीम है। कैसे बांधेंगे उसे?
जोड़ियेगा इस बात को कर्तव्य से। उसके लिए कोई आचरण ही नहीं है। उसका चित्रण कैसे करेंगे आप? किसी चित्र में समाता नहीं है वो, जैसे की पूरे अस्तित्व का चित्र नहीं खींचा जा सकता। आप चित्र खींच सकते हो, एक पहाड़ का, पूरी एक पर्वत श्रंखला का भी खींच सकते हो, पर मैं कहूँ आपसे कि पूरे अस्तित्व का ठीक-ठीक चित्र बनाओ तो आप नहीं बना पाओगे। कैसे बनाओगे, उसके लिए एक और अस्तित्व में आपको जाना पड़ेगा। इतना बड़ा कैनवास कहाँ से लाओगे जिसमें पूरे अस्तित्व को समां सको, इतना बड़ा शब्द कहाँ से लाओगे जिसमें आप सत्य को समां सको। सारे विरोधाभास उसमें आकर मिल जाते हैं और शून्य हो जाते हैं। वह सब कुछ है और कुछ नहीं भी है। कुछ ऐसा नहीं जो उसके लिए वर्जित है, और कुछ ऐसा नहीं है जो उसके लिए करणीय है। तो उसको आप क्या बोलोगे? वो बच्चा जैसा है, और पल ही भर में वो वृद्ध समान हो जाएगा, वो पुरुष भी है और स्त्री भी है। अर्धनारेश्वर याद है ना आपको? वो अष्टावक्र का परमयोगी भी है, वह पुरुष भी है और स्त्री भी। आप उसे क्या बोलोगे? परमपुरुष है वह, और पल भर में पूरी तरह से स्त्री हो जाएगा। प्रकृति के सारे गुण दिखने लगेंगे उसमें, अब क्या करोगे? और यही नहीं कि अभी पुरुष है फिर स्त्री है। महा-दिक्कत तो तब आएगी जब एक ही समय में पुरुष भी हो और स्त्री भी। अब उसका विवरण देना हो, तो कैसे दोगे? बड़ी दिक्कत हो गयी। वो झूठा भी है और सच्चा भी है, सारी माया दिखा देगा वह आपको, और वह सत्य में ही बैठा हुआ है। कैसे पह्चानोगे उसको? कोई चिन्ह नहीं उसका, कोई विशेष चिन्ह ही नहीं। परमबहरूपिया है, सारे रूप हैं उसके क्योंकि उसका अपना कोई रूप नहीं है। पूरा अस्तित्व उसका है, क्योंकि उसकी कोई छोटी सी जगह नहीं है। हर जगह उसका घर है, क्योंकि वह अनिकेत है। कैसे पह्चानोगे, कैसे ढूँढोगे, कैसे बस में करोगे उसे?
अनिर्वाच्य स्वभाव है! ये हम सबके लिए एक पैगाम है। अपने मन में कभी छवि मत बना लीजियेगा, कि योगी ऐसा होता है, कि अच्छा जीवन इस-इस तरह का होता है। कुछ भी हो सकता है, वह अनिर्वाच्य है। वह ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। किन्हीं कर्मों को पकड़ कर मत बैठ जाना कि जो ऐसा-ऐसा कर रहा हो वो योगी है, अन्यथा नहीं। ना !
यह जितनी बड़ी पहेली है, उतनी ही बड़ी मुक्ति भी है। इस बात को सुनकर मन जितना उलझता है कि यह भी नहीं और वह भी नहीं, यह उतनी ही बड़ी मुक्ति भी तो है। यह देख रहे हो ना कि सब चलता है। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। पर पहले तुम योगी हो जाओ, पहले तुम वो स्थितप्रज्ञ बनो, जिसकी प्रज्ञा बैठ गयी है।
श्रोता २: सर खुद को पता लग रहा होता है ना, बाहर वालों को नहीं?
वक्ता: अरे उसके लिए को बाहर वाला है ही नहीं, सब अन्दर वाले हैं। सबको अपनी जेब में रखकर चलता है, कुछ बाहर है ही नहीं। यह सब तो गृहस्त में होता है; घरवाली, बाहरवाली। वो योगी है! क्या अन्दर, क्या बाहर?
ज्ञान सेशन पर आधारित। स्पष्टता हेतु कुछ अंश प्रक्षिप्त हैं ।
