लड़कियां तो पराया धन हैं

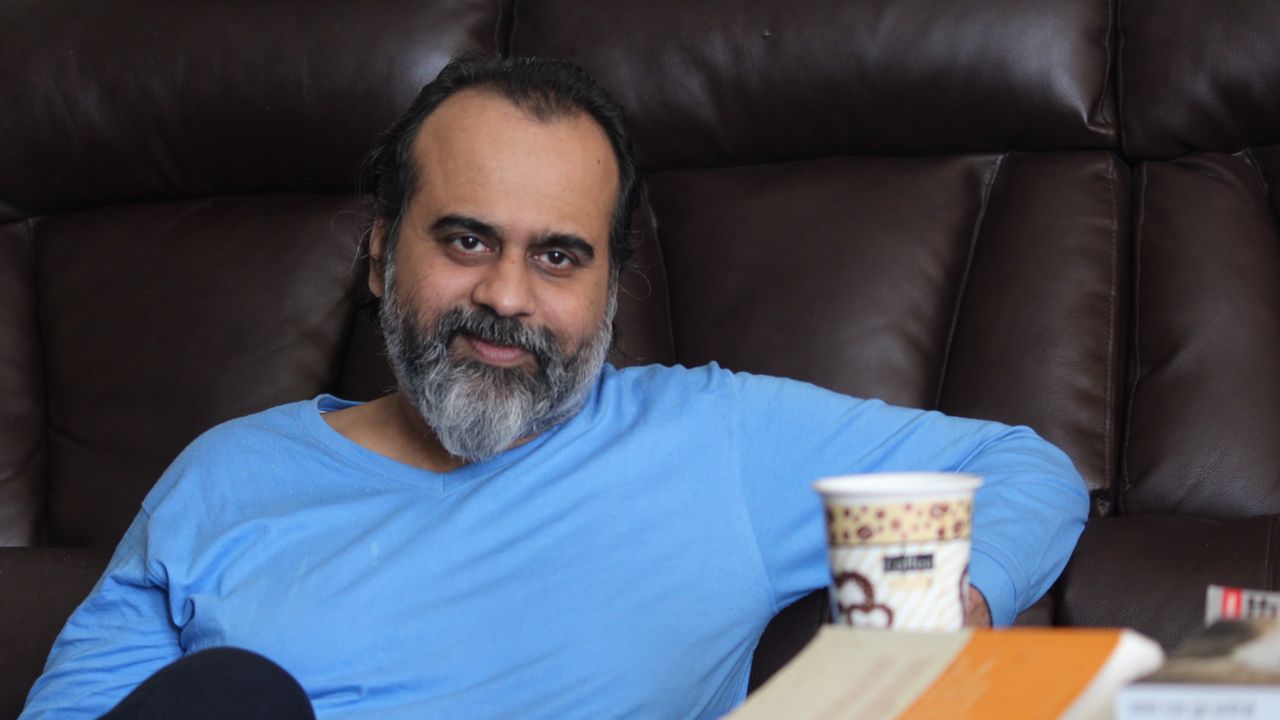
प्रश्नकर्ता: सर, आप फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा वोकल (मुखर) हैं। तो जब हम महिलाओं के लिए बोलते हैं कि इसकी तो शादी हो जाएगी, ये तो ‘पराया धन’ है। ये जो ‘पराया धन’ बोलते हैं, ये बात कहाँ से आई और हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो पराया धन है?
आचार्य प्रशांत: इसमें इतना बड़ा राज़ क्या है, पराया वगैरह तो ठीक है…
प्रश्नकर्ता: वो तो इसी घर में जन्मी है।
आचार्य: हाँ, वो ठीक है ‘पराया’ बोलते हैं, पर देखिए न ‘धन’ बोला। धन माने वो चीज़ जो जड़ होती है।अब ये, (हाथ से माइक उठाते हुए) ये धन है, ये धन है , धन माने जिसकी अपनी कोई चेतना नहीं। धन माने जो सदा किसी और के स्वामित्व में रहेगा, वो धन है। धन कभी बोल नहीं सकता कि मैं अपने हिसाब से खर्च होऊँगा। धन ऐसा बोल सकता है?
प्रश्नकर्ता: नहीं बोल सकता।
आचार्य प्रशांत: धन माने वो जो किसी की प्रॉपर्टी है। और अगर आपको किसी का इस्तेमाल अपने हिसाब से करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी चेतना उससे छीन कर उसे ऐसे ही जड़ बना दो। बात ये नहीं है कि स्त्री पराया धन है, कि अपना धन है — वो धन क्यों है? किसी का धन नहीं है वो, वो एक स्वतंत्र चेतना है, मनुष्य है।
प्रश्नकर्ता: सर, अगर हम ओलंपिक्स की बात करें और हम जब पिछले कई सारे आँकड़ों पर नज़र डालते हैं, कई बार हम ये भी देखते हैं कि महिलाएँ और पुरुषों का कंपैरिज़न (तुलना) चलता रहता है। पर जब हम मेडल्स देखते हैं, अगर मैं युएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका) की खासतौर पर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो मेडल हैं, वो महिलाएँ ही लेकर आती हैं पिछले कई वर्षों से। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में मेडल्स की संख्या महिलाओं की तरफ़ से इतनी कम क्यों रही हैं?
आचार्य प्रशांत: अब बढ़ने लगी है।
प्रश्नकर्ता: अब बढ़ी है। इसमें दो मेडल्स लेकर आई हैं।
आचार्य प्रशांत: अभी तीन में से दो में तो महिला का ही योगदान है। क्यों कम रही है, क्योंकि हमने महिला को कभी ये क्षेत्र दिया ही नहीं कि वो खेल भी सकती है। ओलंपिक्स में क्या होता है वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे गली-मोहल्लों में क्या होता है वो बहुत पास की बात है। जब हमारे घरों में और गलियों में और मोहल्लों में, स्कूलों में ही लड़कियाँ खेल नहीं रही हैं तो ओलंपिक्स में कहाँ पहुँच जाएँगी?
ये बात बहुत दूर की है कि भारत की महिलाएँ ओलंपिक्स से पदक क्यों नहीं लातीं। ये बात बहुत दूर की है कि भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में इतना कम क्यों है, बोर्डरूम्स (कंपनी के अधिकारीयों की बैठक) में इतना कम क्यों है, इकोनॉमी में इतना कम क्यों है…
प्रश्नकर्ता: सैलरीज़ (वेतन) क्यों कम होती हैं।
आचार्य प्रशांत: सैलरीज़ क्यों कम होती हैं, ये बातें तो हमें ऐसा लगता है कहीं और की हैं। ‘अरे वहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, अरे वहाँ भेदभाव हो रहा है।’ वहाँ क्या हो रहा है (छोड़ो), हमारे घरों में क्या हो रहा है? सब कुछ हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से शुरू होता है।
प्रश्नकर्ता: बिलकुल! बिलकुल!
आचार्य प्रशांत: लड़कियों को हम कितना खेलने के लिए प्रेरित करते हैं? लड़कियों को हम उनके को-करिक्यूलर्स (सह-पाठ्यक्रम) विकसित करने के लिए कितना प्रेरित करते हैं? भई, उनका तो जो पूरा योगदान है वो ये माना जाता है कि जाकर के घर सवारों और वंश-वृद्धि में अपना योगदान दे दो। उनकी अपनी कोई अस्मिता है! कि वो महिला बाद में है, मनुष्य पहले हैं! ये बात तो जैसे हमारे भीतर, हमारी संस्कृति में आती ही नहीं है।
प्रश्नकर्ता: सर, इसका एक *एग्ज़ांपल *(उदाहरण) भी मैं देना चाहूँगा। मैंने अपने रेडिओ शो में भी पूछा था कि जो महिला क्रिकेट है, उसको देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों नहीं होती? तो मेरे पास सर कॉल आया एक महिला का, उन्होंने बोला कि मैं फीमेल (महिला) क्रिकेट देख रही थी, मेरी सास ने मुझे बोला कि क्या कर रही है; टीवी बंद कर और जा, रोटी बना। आपकी बात से मुझे याद आ गया कि घर में ही सपोर्ट (समर्थन) नहीं मिलता है तो इतनी बड़े स्तर पर कैसे मिलेगा?
आचार्य प्रशांत: देखिए बल के जितने काम होते हैं; खेल माने बल का, कर्मठता का, पौरुष का, जीवट का, साहस का प्रदर्शन। हम घबराते हैं महिला अगर बल का, पौरुष का, जीवटता का, साहस का प्रदर्शन कर दे तो। हम कहते हैं, ‘ये तो बिलकुल एकदम अब छा जाएगी, पता नहीं क्या करेगी।’ अब लड़कियाँ हैं उनको कई बार घरों से ही बोला जाता है, ‘जिम जाओगी तो शरीर कोमल नहीं रह जाएगा, कंधे चौड़े हो जाएँगे, तुम्हें पसंद कौन करेगा?’ क्योंकि पुरुषों को भी लड़की ऐसी चाहिए जो कोमलांगिणी हो।
प्रश्नकर्ता: हाँ (हँसते हुए), बिलकुल!
आचार्य प्रशांत: ताकि उसपर नियंत्रण रखा जा सके। अगर वो आपके ही समकक्ष बलशाली हो गई तो उसकी नाक में नकेल डालकर कैसे रखोगे? और स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स का तो काम होता है कि आपके भीतर न सिर्फ़ शारीरिक बल्कि मानसिक बल भी विकसित करे। स्पोर्ट्स का काम होता है कि आपको सिखाए कि हारती हुई हालत में भी जीता कैसे जाता है।
अगर महिला ये सब अगर सीख गई तो हमारे घरों में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए हम महिलाओं को प्रेरित ही नहीं करते कि खेलने जाओ। खेलने जाती भी हैं तो हम कहते हैं, ‘लड़कियाँ खेल रही हैं, ये सब कौन देखे, क्या करे।’ हाँ, एक खेल होता है महिलाओं का जो पुरुष बहुत चाव से देखते हैं, वो है स्विमिंग।
प्रश्नकर्ता: सर, इंग्लिश बैकग्राउंड (पृष्ठभूमि) रहा है आपका, लेकिन आपकी जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी संवाद मैंने देखे हैं वो हिंदी में देखें हैं। ये हिंदी को आप प्रमोट (प्रोत्साहन) कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि हिंदी में भावनाएँ ज़्यादा अच्छी व्यक्त होती हैं?
आचार्य प्रशांत: नहीं, मैं अंग्रेज़ी में भी बोलता हूँ। आप हमारे अंग्रेज़ी चैनल पर जाएँगे तो वहाँ भी दो-तीन हज़ार वीडिओ मिलेंगे।
प्रश्नकर्ता: पर ज़्यादातर मैंने हिंदी में ही देखे हैं।
आचार्य प्रशांत: मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि मुझे सब तक पहुँचना है भई! मैं अंग्रेज़ी में बोल सकता हूँ, अभी यहाँ पर हम बात कर लेते, बहुत बार करी भी है, पर ईमानदारी से बताइए कि अभी अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको विशुद्ध अंग्रेज़ी में बोलना शुरू कर दूँ, तो क्या बात उतनी ही सुग्राह्य रह जाएगी जितनी अभी है?
अभी हम अपनी मिट्टी , अपनी ज़मीन की भाषा में बात कर रहें हैं — बात हम आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। यही बात अंग्रेज़ी में होगी तो नहीं पहुँचेगी। इसके अलावा जो और बड़ी मुद्दे की बात है — मुझे सबसे ऊँची बात को बिलकुल आखिरी आदमी तक पहुँचाना है। क्या अध्यात्म पर उनका अधिकार नहीं हैं जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती?
और भारत में आमतौर पर भाषा और आर्थिक स्थिति में बड़ा गहरा संबंध है। मैं अगर अंग्रेज़ी में बोलता रहा तो मैं गरीबों तक कभी नहीं पहुँच सकता। मैं अंग्रेज़ी में ही बोलता रहा तो जितने भी वंचित, दलित, दमित, पिछड़े वर्ग हैं समाज के, मैं उनतक नहीं पहुँच पाउँगा।
और मेरा काम ये नहीं है कि मैं आईआईटी, आईआईएम उस, उस तरफ़ से आ रहा हूँ तो बस मैं उतने ही इलीट (विशिष्ट) ग्रुप में बात करता रहूँ। मुझे उसी इलीट ग्रुप में ही रहना होता तो मैं वहीं बैठा होता, मुझे वहाँ नहीं रहना है। मुझे सबतक जाना है, मैं इसलिए आया हूँ। तो यहाँ मैं वो सब छोड़कर के आऊँ और फिर भी अंग्रेज़ी पकड़े रहूँ? तो ये बात तो बिलकुल बेमेल हो जाएगी।
प्रश्नकर्ता: सर, आपको विश्वभर से प्रेम मिल रहा है। और अगर मैं प्रेम की बात करूँ तो हम कैसे पहचाने कि सामने वाला हमसे प्रेम करता है?
आचार्य प्रशांत: जब तक आपको सामने वाले से प्रेम की बहुत ज़रूरत है आपमें कोई प्रेम नहीं है। प्रेम लेने या माँगने की बात नहीं होती है। प्रेम माँगना एक तरह की सूक्ष्म हिंसा होती है।
प्रेम तो अपनी पूर्णता की अभिव्यक्ति होता है। प्रेम तो ऐसी चीज़ होती है कि मैं दूँगा, प्रेम माँगा थोड़े ही जाता है। तो सामने वाला मुझसे प्रेम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये प्रश्न हमें छोड़ देना चाहिए।
हमें ये देखना चाहिए कि हममें प्रेम है या नहीं है। हम प्रेम के लायक हुए हैं कि नहीं हुए हैं — प्रेम पाने के लायक नहीं, प्रेम देने के लायक हम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। लेकिन हम स्वयं को कभी देखते नहीं, नज़र हमारी हमेशा बाहर को रहती है। तो हम किसी ऐसे को तलाशते रहते हैं जो हमसे प्रेम करता हो।
और जब हम कहते हैं, ‘कोई मुझे मिल जाए जो मुझसे प्यार करता हो।’ तो इससे हमारा आशय क्या होता है? हमारा आशय यही तो होता है कि उससे हम कुछ ले लें, तो ये स्वार्थ की तो अभिव्यक्ति है न?
प्रश्नकर्ता: बिलकुल, स्वार्थ ही हुआ!
आचार्य प्रशांत: स्वार्थ की तो अभिव्यक्ति है। तो असली आदमी वो होता है जो ये प्रश्न पूँछना ही भूल जाए कि कोई मुझसे प्यार करता है, कि नहीं करता है। साहब (अभी) आपने कहा, ‘मुझे दुनियाभर से प्रेम मिलता है।’ जितना प्रेम मिलता है लगभग उतनी ही, शायद उससे ज़्यादा नफ़रत भी मिलती होगी।
प्रश्नकर्ता: बिलकुल।
आचार्य प्रशांत: मै देखना भूल गया कि लोग मुझे क्या दे रहे हैं। देख भी लेता हूँ तो महज़ आँकड़ो के नाते, एक फ़ैक्ट की तरह, कि भई अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ उसका लोगों पर असर क्या पड़ रहा है। लेकिन मैं, लोगों से क्या आ रहा हैं मुझको, इस बात को मैं अपने कर्त्तव्य के रास्ते में नहीं आने देता।
आप मुझे प्रेम दो या नफ़रत दो, मैं आपको वो दूँगा जो मेरे हिसाब से सबसे ऊँची बात है। आप मुझे ताली दो चाहे गाली दो, मैं आपको सच ही दूँगा — ये प्रेम होता है!
प्रश्नकर्ता: सर, एक ज़माना था जब बिना देखे शादी हो जाया करती थी और बुढ़ापे तक टिकाऊ रहती थी। आजकल लोग लिव-इन (बिना शादी के दो वयस्कों का साथ रहना) में भी रहते हैं, घूमते भी हैं और फिर शादी के कुछ वक्त के बाद डाइवोर्स ले लेते हैं। तो ये डायवोर्स केसिस क्यों बढ़ते जा रहा हैं?
आचार्य प्रशांत: देखिए, बढ़ते इसलिए जा रहे हैं, अब बात हो सकता है आपको बहुत प्यारी न लगे, पर आपने इसलिए तो नहीं पूछा कि मैं आपको कुछ दबा, छुपा, ढका हुआ ज़वाब दे दूँ, तो खुली बात बोलता हूँ। बढ़ते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रकृति ने इंसान को ऐसा बनाया नहीं है कि कोई भी दो व्यक्ति ताउम्र एकसाथ चल सकें, चाहे वो दो बच्चे हों, चाहे दो पुरुष हों, दो स्त्रियाँ हों, या फिर स्त्री और पुरुष हो। तो ऐसा कोई प्रकृति में न बंधन है, न व्यवस्था है कि दो लोगों को साथ हमेशा चलना ही है। ठीक है?
पहले चल जाता था, क्योंकि बहुत तरीके के डर होते थे। हो तो ये भी जाता है कि आप किसी को उम्रकैद की सज़ा दे दें तो वो जीवनभर जेल में चल जाए, उसको आप ये थोड़े ही कहेंगे कि बहुत प्यार की बात है।
तो क्यों बढ़ने लगा है? क्योंकि अब लोगों को हक आ गया हैकि वो अलग हो सकते हैं। और लोगों को अधिकार रहेगा कि वो अलग हो सकते हैं, तो अलग होंगे। मैं बिलकुल मानता हूँ और अच्छी तरह मैंने देखा भी है कि जब माँ-बाप अलग होते हैं तो उसका परिवार पर, विशेषकर बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
ये बिलकुल देखा है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उतना ही बुरा असर, और उससे ज़्यादा बुरा असर उन परिवारों में भी पड़ता है जहाँ माँ-बाप में दिन-रात की कलह रहती है। और जहाँ दो ऐसे व्यक्ति, एक स्त्री (और) एक पुरुष साथ रह रहे होते हैं जिनमें आपस में कोई संगती हो ही नहीं सकती, लेकिन ये दोनों ज़बरदस्ती एक-दूसरे के साथ हैं, और ऐसे परिवारों से भी बच्चे बहुत बरबाद निकलते हैं। तो कुछ हद तक संबंध विच्छेद होना कोई आवश्यक रूप से बुरी बात नहीं है।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि जितने लोग हैं सब अपने रिश्ते तोड़ लें। लेकिन अगर, अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोग हैं, अपनी-अपनी कंपनियों में, ऑर्गनाइज़ेशंस (में) सीरियस पदों पर होंगे। आप जो भी निर्णय लेते हो वो सौ प्रतिशत सही निकलता है क्या? आप हायरिंग (नियुक्ति) करते हो, वो सारी फ़ूलप्रूफ़ (विश्वसनीय) होती हैं, या हायरिंग मिस्टेक्स भी होती हैं?
प्रश्नकर्ता: गलतियाँ होती हैं।
आचार्य प्रशांत: आप किसी को प्रमोशन दे देते हो, आपको फिर ऐसा नहीं होता है क्या कि एक साल बाद पता चले एक गलत आदमी को प्रमोशन दे दिया। इंसान हैं न हम, भगवान थोड़े ही हैं कि गलती नहीं कर सकते। जब गलती नहीं कर सकते, तो शादी के लिए भी आप जिसको चुनते हो उसमें भी गलती हो सकती है। और अगर वो गलती हो गई है तो उसका सुधार करो।
सुधार पहले तो ऐसे किया जाता है कि बातचीत करी, रिश्ता बचाने की कोशिश करी, वो भी सुधार का ही एक तरीका है। लेकिन अगर वो तरीका नहीं चलता तो आवश्यक नहीं है कि एक-दूसरे के साथ बंधे रहकर यंत्रणा भोगो जीवनभर।
प्रश्नकर्ता: तब अलग रहना ही सही रहेगा, ऐसा आपका मानना है?
आचार्य प्रशांत: देखिए, मैं आपको एक आँकड़ा बताता हूँ। मेंटल डिज़ीज़ (मानसिक रोग) जो है दुनिया में, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिमागी बीमारी का दुनिया में सबसे बड़ा कारण विवाह है, ये जो बेमेल रिश्ते हैं। ये सिर्फ़ हँसने की बात नहीं है, ये यथार्थ है, ये फ़ैक्ट है।
आप जाएँ अगर किसी साईकोलॉजी (मनोविज्ञान) के ज्ञाता के पास या किसी साइकेट्रिस्ट (मनोचिकित्सक) के पास, तो आपको बताएगा कि ये जितना दिमाग का बिलकुल ज्वालामुखी बनता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने पर विवश होना पड़ रहा है जिसके साथ आपका कोई मेल बैठ ही नहीं सकता।
