क्या हमेशा खुश दिखना ज़रूरी है?

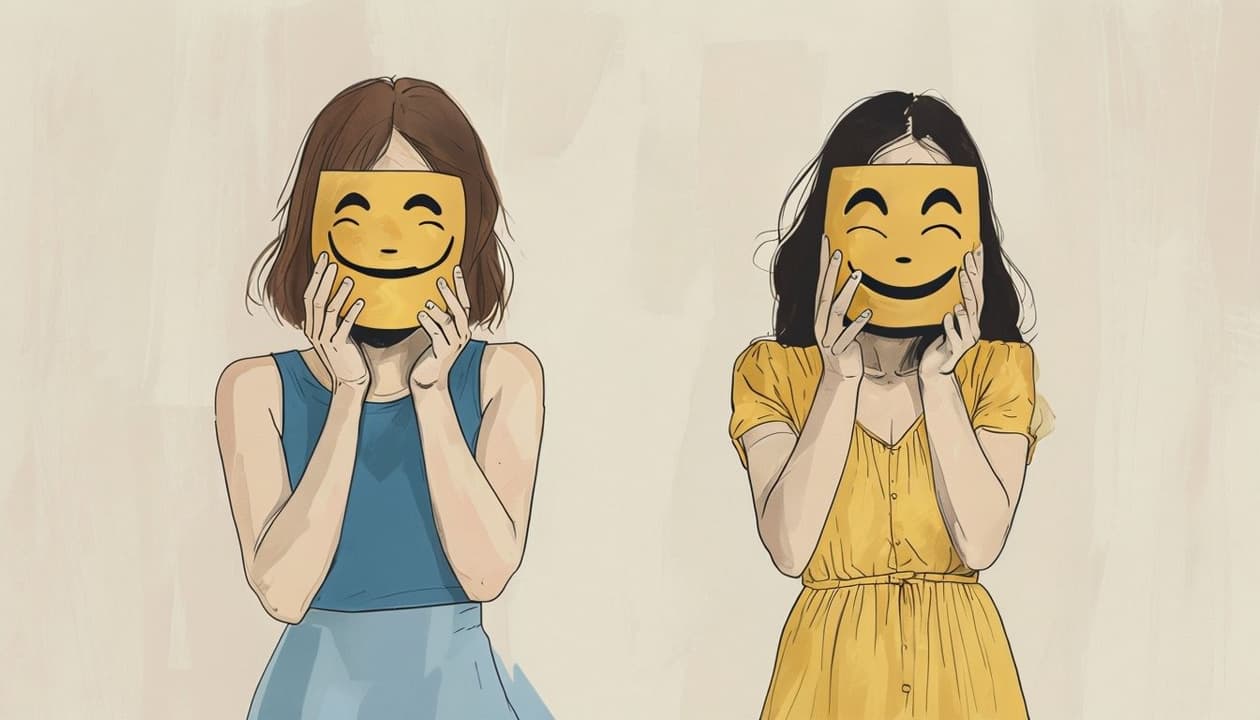
प्रश्नकर्ता: प्रणाम आचार्य जी, मैं अपने भीतर लगातार एक बेचैनी अनुभव करती हूँ और उस बेचैनी के मूल में मैंने एक पैटर्न (ढ़ाँचे) को ऑब्ज़र्व (निरीक्षण) किया है। वह पैटर्न (ढ़ाँचा) इस प्रकार है — मैं चेतन रूप से, कॉन्शियसली, जानबूझकर खुश और अच्छा अनुभव करने की कोशिश करती हूँ जबकि हक़ीक़त में, अवचेतन में, अनकॉन्शियसली, मैं उतनी खुश या अच्छी नहीं हूँ। मैं यह समझना चाहती हूँ कि यह प्रयास मैं सतत-लगातार आखिर क्यों कर रही हूँ?
आचार्य प्रशांत: क्योंकि समाज ने हमको सिखा दिया है कि खुश रहना चाहिए, "हैप्पी फेसबुक फेस"। तो बाहर की इस सीख को हमने इतना सोख लिया है कि ये बात बिल्कुल अंदर तक पैठ गई है। "खुश रहो, हैप्पी रहो," एकदम चेतना की गहराई में पहुँच गई है ये बात। बहुत लोगों ने तो इतना अपने-आपको प्रशिक्षित कर लिया है कि वो सोते समय भी मुस्कुराते रहते हैं। "क्या पता, कोई सोते समय फोटो खींच ले? उसमें कहीं दिख ना जाए कि हम मुस्कुरा नहीं रहे थे। तैयारी पूरी रखो।" कोई पूछे, "क्या हाल है?" तुरंत बोलो, “आई एम हैप्पी” (मैं खुश हूँ)।
और जो जितना प्रकट करे कि वो प्रसन्न है, उसके बारे में जान लीजिएगा कि वो आनंदित तो नहीं ही है, प्रसन्न भी नहीं है। वो वास्तव में भीतर से दुखी है।
प्रसन्नता का मुखौटा और होता क्या है? दुख को ढँकने की एक नाकामयाब साज़िश। ये साज़िश वही करता है जो मन की मूल प्रकृति के बारे में अज्ञानी होता है, जो मन की द्वैतात्मक प्रकृति को समझता नहीं है, जो सुख को दुख से भिन्न जानता है। जो सुख और दुख की हक़ीक़त नहीं जानता वही दूसरों को ये प्रदर्शित करने में लगा रहता है कि "मैं तो सुखी हूँ," और जब वो दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है कि "मैं सुखी हूँ," तो उसके इस प्रदर्शन के भुलावे में, बहकावे में आते भी कौन हैं? उसी के जैसे अज्ञानी लोग जो मन को नहीं जानते। तो एक अज्ञानी दिखा रहा है कि वो खुश है और दूसरा अज्ञानी उसकी खुशी को देखकर माने ले रहा है कि वो पहला व्यक्ति खुश है।
आपने कितने अवतारों को मूर्तियों में हँसते हुए देखा है? ज़रा बताइएगा, बोलिए। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, इनको मुस्कुराता पाते हैं? बोलिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नौदुर्गा की तमाम देवियाँ, गणेश, इनको मूर्तियों में भी क्या पारम्परिक रूप से हँसता-मुस्कुराता प्रदर्शित किया जाता है? अब गुरुओं पर आइए, दत्तात्रेय हों, आचार्य शंकर हों, जहाँ कहीं भी इनको निरूपित किया जाता है, क्या प्रसन्न निरूपित किया जाता है? बोलिए। जटाधारी शिव हैं, उनकी मूर्तियाँ देखी होंगी। वो ध्यानस्थ दिखाई देते हैं या सुखस्थ? ध्यानस्थ, है न? फिर संतों पर आइए, नानक साहब हों, कबीर साहब हों, इनके चित्र भी कभी आपने देखें कि ये हँस रहे हैं? बोलिए।
अब एक काम करिएगा, अपने ही परिवार के पुराने एल्बम खोलिएगा, जिसमें उन्नीस-सौ-सत्तर से पहले के चित्र हों, फोटोग्राफ्स। आपके माताजी-पिताजी के होंगे, अगर आप थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, या आपके दादा-दादी, नाना-नानी के होंगे। देखिएगा कि क्या मुस्कुराते हुए चित्र हैं उनके? मैं आज की पीढ़ी की बात नहीं कर रहा। मैं साठ और सत्तर के दशक के श्वेत-श्याम चित्रों की बात कर रहा हूँ। मुस्कुराते हुए होते थे उनमें? ये चलन कहाँ से आ गया कि तुम्हें हैप्पी (खुश) रहना-ही-रहना है?
अब समझिएगा। प्रकृति में सुख का अर्थ होता है 'भोग'। 'आनंद' तो प्रकृति जानती नहीं। पशु आनंद का अनुभव नहीं करते; हाँ, सुख का अनुभव पशु भी करते हैं। आनंद बस मनुष्यों की ही चीज़ है, पशुओं को उपलब्ध नहीं। पशुओं को सुख मिलता है।
पशु सुख का अनुभव कब करते हैं? भोग के समय। जब वो विश्राम भोग रहे हों, या भोजन भोग रहे हों, या मैथुन भोग रहे हों, तब वो सुख का अनुभव करते हैं और इन्हीं वस्तुओं की, इन्हीं भोगों की अनुपस्थिति में वो दुख का अनुभव करते हैं।
तो प्रसन्नता का संबंध प्रकृति में सदा भोग से है। तो जो आपको सिखा रहे हैं कि हमेशा 'हैप्पी' (खुश) नज़र आओ, वो वही लोग हैं जो आपको भोग की तरफ़ प्रेरित कर रहे हैं।
अब थोड़ी बुद्धि लगाइए, बताइए दुनिया में कौन होगा जो चाहेगा कि आप बार-बार भोग करें? जो चाहेगा कि आप बार-बार भोग करें, वही आपको एक मनोवैज्ञानिक, एक मानसिक छलावे में रखेगा। वो ये सीख देता रहेगा कि "खुश रहा करो न, खुश रहा करो।" मनोवैज्ञानिक-तौर पर वो आपको बार-बार ये सीख देगा कि "खुश रहो," और भौतिक-तौर पर वो आपके सामने क्या रखेगा बार-बार? भोग की सामग्री। आप एक बाज़ार में जा रहे हैं, कौन आपसे बार-बार कहेगा, "आओ ज़रा लड्डू भोगो न, आओ न ज़रा लड्डू खाओ न," ये आपसे कौन कहेगा बाज़ार में? लड्डू बेचने वाला।
तो भोग के लिए आपको वही लोग प्रेरित कर रहे हैं जो भोग की सामग्री के निर्माता और विक्रेता हैं। ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? और चूँकि भोग का संबंध प्रसन्नता से है, इसीलिए वो आपके भीतर ये शिक्षा, ये मूल्य भरे दे रहे हैं कि प्रसन्नता बहुत बड़ी बात है, हमेशा हैप्पी (खुश) रहा करो। क्योंकि उन्हें अपना सामान बेचना है। उन्हें पता है कि उन्हें लड्डू बेचना है, लड्डुओं का संबंध प्रसन्नता से है, तो लड्डू बेचने के लिए वो आपको ये सिखाएँगे, "बी हैप्पी (खुश रहो)"। क्योंकि उन्हें मालूम है कि, "लड्डुओं से हैप्पीनेस (खुशी) मिलनी है, अब अगर इस आदमी को हैप्पी (खुश) होना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे मेरा लड्डू खरीदना पड़ेगा; मेरी जेब भरेगी।"
तो जैसे-जैसे पिछले सौ, डेढ़-सौ सालों में दुनिया में पदार्थों का उत्पादन बढ़ा है, औद्योगीकरण हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से फैक्ट्री आउटपुट आने लगा है, वैसे-वैसे ये आवश्यक हो गया है कि जो माल पैदा हो रहा है उसकी खपत भी तो हो। तभी तो हमें मुनाफ़ा होगा वरना हमने तो बहुत बड़ी फैक्ट्री (कारखाना) डाल दी, जो बहुत सारा उत्पादन करती है, पर उत्पादन-भर करने से क्या होगा? लोग उसको खरीदें और उसका उपभोग करें तब बात बनेगी न? तभी तो माल मिलेगा, मुनाफ़ा मिलेगा।
अब लोग काहे को खरीदें आपका माल, अगर लोग पहले ही संतुष्ट हैं? तो आपका माल बिके इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि लोगों में असंतुष्टि की भावना पैदा की जाए। उन्हें विज्ञापन दिखा-दिखाकर, उनको ग़लत शिक्षा दे-देकर के, उनको ग़लत तरह का साहित्य पढ़ाकर के, ग़लत तरह का मीडिया और फ़िल्में दिखाकर के, उनमें एक असंतुष्टि की भावना भरी जाए और उनको ये बताया जाए कि, "देखो अभी तुम दुखी हो और सुखी होना बहुत ज़रूरी है। जीवन का लक्ष्य ही है हैप्पीनेस (खुशी), और वो हैप्पीनेस (खुशी) तुमको मिलेगी मेरी दुकान का माल खरीदकर।" बात समझ में आ रही है?
यही वजह है कि आज से कुछ दशकों पहले तक, कम-से-कम भारत में, दाँत दिखाने की बहुत परम्परा नहीं थी कि ज़बरदस्ती दाँत फाड़े खड़े हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, "आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, एवरीबडी इज़ हैप्पी" (मैं खुश हूँ, तुम खुश हो, सब खुश हैं)। क्योंकि कुछ दशकों पहले तक भारत में इतना उपभोक्तावाद भी नहीं था। अब जब लोगों के पास पैसा आया है तो तमाम उत्पादनकर्ता भेड़िए खड़े हुए हैं, जिनकी निगाह आपकी जेब पर है, जिनकी निगाह वास्तव में आपके समूचे जीवन पर है। और वो आपसे सीधे-सीधे नहीं कहेंगे कि "आओ, मेरा माल खरीदो," वो कहेंगे आपसे, "आओ मेरे पास, हैप्पीनेस (खुशी) खरीदो।"
क्योंकि अगर वो सीधे कहें कि "आओ, मेरा माल खरीदो," तो आप कहेंगे "क्यों खरीदें? तुम्हारी चीज़ है।" पर जब वो आपसे कहते हैं कि, "हैप्पीनेस (खुशी) बहुत ज़रूरी चीज़ है और आओ, मैं तुम्हें हैप्पीनेस (खुशी) दूँगा," तो आप इस बात के विरुद्ध कोई तर्क नहीं दे पाते, आप कहते हैं "हैप्पीनेस (खुशी) तो ज़रूरी है ही, हमें बचपन से यही बताया गया है, कि खुश रहो, खुश रहो, तो जहाँ भी खुशी मिल रही है, मैं जा रहा हूँ उसे खरीदने।" अब बात समझ रहे हैं?
आम आदमी झूठी खुशी के फेर में पूरी ज़िन्दगी अपनी ख़राब कर लेता है, बर्बाद कर लेता है। एक के बाद एक छोटे-बड़े ग़लत निर्णय लेता ही चला जाता है। उसे समझ में भी नहीं आता कि उसका पूरा जीवन बाज़ार संचालित कर रही है। हमें खुशी के टेम्पलेट (साँचे) दे दिए गए हैं। हमें खुशी की ढर्राबद्ध परिभाषाएँ दे दी गई हैं।
"ऐसा करोगे तो खुश रहोगे, इतना खर्चा करोगे तो इस तल की खुशी मिलेगी। थोड़ी और खुशी चाहिए तो भाई थोड़ा और रोकड़ा निकाल न।" कोई नहीं पूछता कि, "खुशी चाहिए ही क्यों?" क्योंकि किसी को भी सही जीवन-शिक्षा नहीं दी गई है, क्योंकि किसी को भी ये बताया ही नहीं गया है कि जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है। सुख तो भ्रम है, झूठ है। सुख तो दुख का ही और तनाव का ही दूसरा नाम है।
जीवन का उद्देश्य मुक्ति है और आनंद है, और मुक्ति का अर्थ होता है — सुख से मुक्ति, सुख-दुख दोनों से मुक्ति।
चूँकि हमारी जीवन-शिक्षा ग़लत है, इसीलिए हमारी पूरी जीवन-व्यवस्था ही ग़लत हो गई है। और नतीजा उसका निकल रहा है — व्यर्थ जाता जीवन और मनोरोगों में भीषण बढ़ोत्तरी। जितने मनोरोगी आज से पचास वर्ष पहले थे दुनिया में, आज उससे दस-गुने से भी ज़्यादा हैं। तनाव का, और चिंता का, एंग्जाइटी का स्तर आज के आम आदमी में करीब-करीब उतना हो गया है जितना एक शताब्दी पहले के विक्षिप्त आदमी में होता था।
आज का आम आदमी वैसा है मानसिक तल पर जैसा आज से सौ साल पहले का पागल आदमी होता था। जाकर के मनोवैज्ञानिकों की राय ले लीजिए, वो इस बारे में आपको और बहुत सारी जानकारी देंगे, या सायकोलॉजी (मनोविज्ञान) के जो प्रामाणिक और प्रतिष्ठित जर्नल (पत्रिका) हैं उनको पढ़ लीजिए।
ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे हैप्पी (खुश) रहना है! जो जितना हैप्पी (खुश) रहना चाहेगा, वो उतना ज़्यादा पागलपन की ओर बढ़ेगा। और इस पागलपन का इलाज सिर्फ़ एक है — सीधा सरल अध्यात्म। और उसको तो हमने मान लिया कि अब तो ये पुरानी चीज़ हो गई न। हमने कह दिया, ये सब ऋषियों-ज्ञानियों-संतों ने जो बातें बोली, ये तो ऑउटडेटेड हो गईं, तिथिबाह्य हो गईं। लोग निकल आए जो क्या कहते है? "देखो, आजकल के ज्ञानी तो यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) के रिसर्चर्स (शोधकर्ता) और प्रोफेसर्स (प्राध्यापक) हैं, उनकी बात सुनो न।"
ये अलग बात है कि ये जिन नए-नए ज्ञानियों की आप बात कर रहे हो उसमें से आधे ख़ुद विक्षिप्त हैं। यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) के डिपार्टमेंट्स (विभाग) में मनोरोगियों का अनुपात साधारण जनता में मनोरोगियों के अनुपात से कुछ कम नहीं होता है। जितने विक्षिप्त बाहर हैं उतने ही विश्वविद्यालयों के अंदर भी हैं। भले ही वो मनोविज्ञान-विभाग ही क्यों न हो विश्वविद्यालय का। सायकोलॉजी डिपार्टमेंट (मनोविज्ञान-विभाग) में सायको (विक्षिप्त) बैठे हुए हैं।
पर नहीं साहब, "पुराने लोग तो बेकार की बात बोलते थे। अरे, हटाओ न ये सब। आओ, तुम्हें नई-नई बातें बताएँगे, नया-नया ज्ञान देंगे।" आजकल नया-नया अध्यात्म भी कढ़ाई से ताज़ा छानकर निकाला जा रहा है। माइंडफुलनेस (सचेतनता), लिविंग इन द प्रेजेंट (वर्तमान में जीना), हैप्पी थॉट्स (प्रसन्न विचार), यू कैन डु इट ( तुम ये कर सकते हो), ट्राई, ट्राई एन्ड ट्राई अगेन ( बार-बार प्रयास करते रहो), यू आर आलरेडी लिबरेटेड (तुम मुक्त ही हो)। एक बार जाँच तो लो कि क्या जानने वालों ने भी तुम्हें यही सब बातें बताई हैं, या बस फँसे जा रहे हो इन आधुनिक जुमलों में।
(एक श्रोता को सम्बोधित करते हुए) अभी भी मुस्कुरा रहे हो। ऐसा घोर प्रशिक्षण हो गया है कि क्या कहें! मैं नहीं कह रहा हूँ कि दुख भरा चेहरा बनाएँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उदास होकर चेहरा लटकाए-लटकाए घूमें।
पर समझिए कि जिसको आप प्रसन्नता कहते हैं वो भी एक तरह का तनाव ही है। मनुष्य की, मन की सहज स्थिति का नाम प्रसन्नता नहीं है। सहजता बहुत दूसरी और बहुत ऊँची बात है।
आप चौबीस घण्टे सहज रह सकते हैं; आप चौबीस घण्टे हँस सकते हैं क्या? आप चौबीस मिनट लगातार हँसकर दिखाइएगा, एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाएगी। पर चौबीस घण्टे सहज रहा जा सकता है। चौबीस घण्टे एक झीना-सूक्ष्म आनंद जीया जा सकता है। चौबीस घण्टे प्रसन्नता नहीं झेल पाएँगे आप, मर जाएँगे।
एक उत्तेजना है प्रसन्नता, एक तरह का तनाव है प्रसन्नता जो आपसे बावली हरकतें करवाए जाती है। बचिए, ये जो कल्ट ऑफ़ हैप्पीनेस (खुशी का पंथ) है इससे बचिए। कल्ट ऑफ़ हैप्पीनेस (खुशी का पंथ) से अगर बच लिए तो सैडनेस (दुख) का निवारण अपने-आप हो जाएगा। और जहाँ ना हैप्पीनेस (खुशी) है ना सैडनेस (दुख) है, ना सुख है ना दुख है, वहाँ अनुपम आनंद है, मुक्ति है, मुक्ति मात्र है।
