अहम् के तादात्म्य

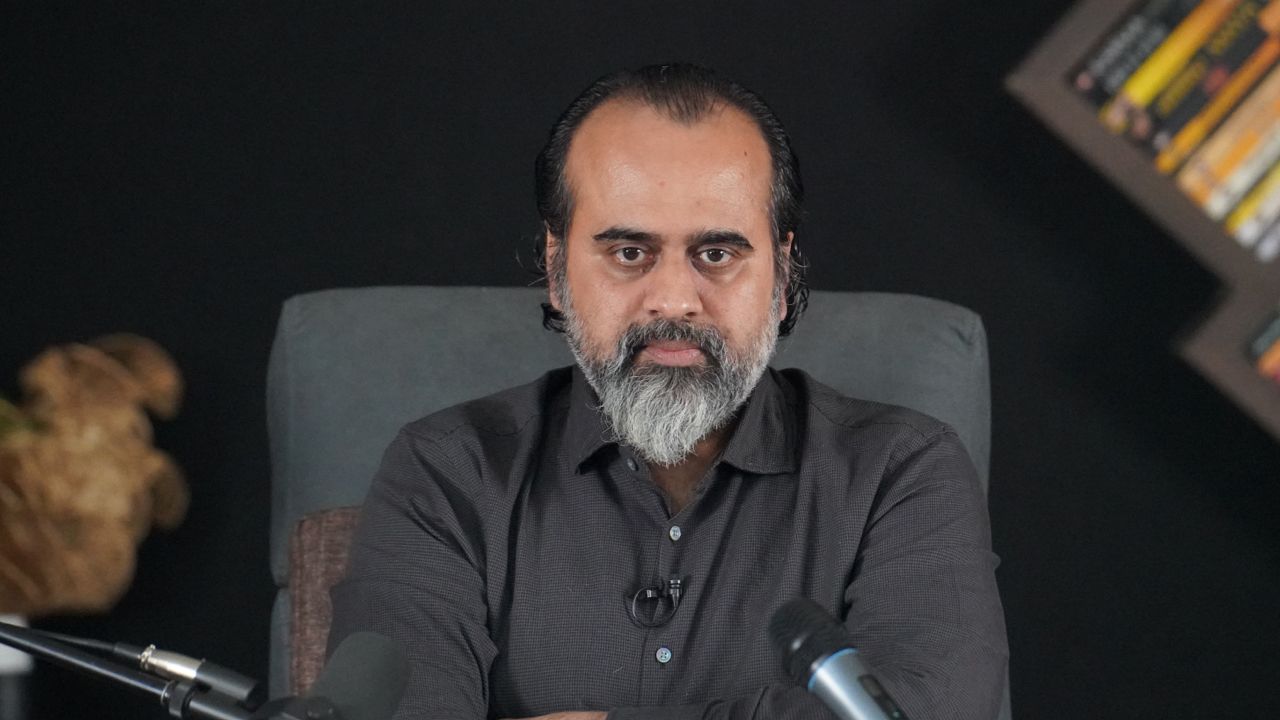
प्रश्नकर्ता: जब मैं कमरे में था कुछ देर पहले और जैसी चीज़ें, दुनिया थी मेरी, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो फिर मैं कौन हूँ और चीज़ें क्या हैं?
आचार्य प्रशांत: क्या नहीं बदला, वही हो तुम। जो तुम अभी अपने कमरे में थे वो तो मिट गया, जो अभी तुम यहाँ हो वो भी मिट जाएगा। क्या है जो नहीं बदलता, भले ही तुम अपने कमरे में हो, सो रहे हो, जग रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, सुन रहे हो। क्या है जो नहीं बदलता? वही हो तुम। बाकी सब तो अवस्थाएँ मात्र हैं। जब कमरे में थे तो पूर्णतया संतुष्ट थे? अभी भी बैठे विचार कर रहे हो, पूर्णतया संतुष्ट हो? एक असंतुष्ट वृत्ति हो तुम जिसको अपनी असंतुष्टि के अलग-अलग कारण मिलते रहते हैं, पल-दर-पल। वो कारण बदलते रहते हैं, उन कारणों से जुड़ी हुई फिर अवस्थाएँ बदलती रहती हैं। जो एक चीज़ नहीं बदलती, वो क्या है? असंतुष्टि। उसी को मैं बार-बार बोला करता हूँ अपने-आपको अतृप्त चेतना जानो।
प्रश्नकर्ता: ये बात भी सुनी है, ये भी बदल जाएगी।
आचार्य प्रशांत: इसी बात से असंतुष्ट हो न? तो कारण एक और मिल गया असंतुष्टि का। गहरी नींद में भी होते हो तो भी क्या मिट जाते हो? कुछ खोज रहे होते हो, इस कारण जगने को तैयार रहते हो। असंतुष्टि तो गहरी नींद में भी नहीं मिट रही। उसी असंतुष्टि का नाम जीवात्मा है।
प्रश्नकर्ता: प्रणाम, आचार्य जी। पिछले अध्याय में आपने कहा कि अर्जुन हम सब हैं पर कृष्ण नहीं हैं सब के पास। साथ-ही-साथ ये भी आभास हुआ कि यदि जीवन की तड़प कृष्ण के ही माध्यम से मिटेगी तो फिर कृष्ण के पास जाने का चुनाव क्यों करना पड़ता है कुछ लोगों को? ये मैंडेटरी (अनिवार्य) क्यों नहीं हो सकता? ये चॉइस (चुनाव) क्यों बनी रहती है? और जो लोग कृष्ण को नहीं चुनते हैं वो संतुष्ट जीवन कैसे बिता लेते हैं? उनको उनकी बेचैनी कैसे स्वीकार हो जाती है?
आचार्य प्रशांत: नहीं, बेचैनी स्वीकार नहीं हो जाती। बेचैनी मिटाने के लिए नए-नए उपाय आज़माते रहते हैं। स्वीकार नहीं कर लेते हैं कि ‘हम बेचैन हैं और ये स्थिति ठीक है, हमने स्वीकार करी’। तो फिर अपनी बेचैनी मिटाने के लिए और तरह-तरह की आज़माइशें करते हैं। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, और सब कुछ विफल हो गया तो फिर कोई और तरीका आज़मा लो। जीवन भर प्रयोग करते रहो, इधर से उधर अनुभव लेते रहो, ये सब चलता रहता है।
दूसरी बात बोली कि ‘अनिवार्य क्यों नहीं किया जाता?’ कौन करेगा? तुम्हारे लिए अनिवार्य थोड़े ही था ये प्रश्न पूछना! देखो, जिस दिन हम पैदा होते हैं न, हमें एक बहुत घातक चीज़ मिल जाती है। ये आज के सत्र में भी मैंने बोला, क्या? चुनाव का विकल्प। कोई यहाँ किसी के लिए कुछ अनिवार्य नहीं कर सकता। अनिवार्यता को तो ये मतलब होता है कि विकल्प अब शेष नहीं है। अनिवार्य माने जिसका कोई निवारण नहीं है, जिससे तुम बच नहीं सकते, वो अनिवार्य है।
अनिवार्य इस अस्तित्व में कुछ है ही नहीं। साँस लेना तक अनिवार्य नहीं। यहाँ तुम कुछ भी कर लो कोई तुम्हें रोकने आने वाला नहीं। कर्मफल मिलता है, वो अपनी जगह है। लेकिन अनिवार्य यहाँ कुछ भी नहीं। हर पल में, हर कर्म में, आपके पास चुनाव का अधिकार रहता ही है। यही आपका सौभाग्य है और यही बड़े-से-बड़ा दुर्भाग्य है। और देखिए कि ये बात कितनी ज़्यादा सशक्तिकरण की है। अब उस शक्ति का किस दिशा में आप प्रयोग करते हो, वो आप जानो।
वेदांत आपको कठपुतली नहीं बना देता दैवीय ताक़तों के हाथ की। वेदांत भाग्यवादी नहीं है। वेदांत ये नहीं कहता है कि हम तो मोहरे हैं बस और चालें शतरंज की, चल कोई और रहा है। ना! भारतीय समाज में और दुनिया में अन्य जगहों पर भी, धर्म के क्षेत्र में ऐसी धारणा बहुत पायी जाती है कि धर्म का मतलब है किसी ईश्वर पर विश्वास, और वो ईश्वर कौन है? जिसकी रज़ा के बग़ैर पंछी पर नहीं मारता और पत्ता भी नहीं खड़कता। है न? ऐसी बातें आपने खूब सुनी होंगी। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसी बातें सुनी हैं न? दुनिया-भर में ऐसी बातें मानी जाती हैं। सब धार्मिक धाराओं में इस तरह की बातें होती हैं कि कोई ईश्वर है जो हमारे सब कर्मों का संचालन कर रहा है, ईश्वर है जो सब कुछ तय करता है।
वेदांत में कोई ईश्वर नहीं होता। वेदांत में आप हैं और आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा या तो सत्यमुखी हो सकती है, या सत्य विपरीत हो सकती है। और सत्य की ओर जाना है या सत्य विमुख हो जाना है, ये आपका चुनाव है। वेदांत आपको बड़ी शक्ति देता है। आपके हाथों में आपकी क़िस्मत रख दी है, अब जो करना है करो। और रख दी है माने ऐसा कोई नहीं कि ऊपर से कोई भविष्यवाणी हुई है या फ़रमान आया है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने आपके हाथ में रखी है। तथ्य बताया है कि ऐसा ही है।
ये जीवन है, जैसा जीना चाहो तुम्हारी इच्छा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो भी कुछ करते हो, वो कुछ बनकर करते हो और जब ग़लत करते हो तो ग़लत बनकर करते हो, और ग़लत होने का परिणाम अच्छा तो नहीं हो सकता। पर वेदांत तो परिणाम को भी भविष्य में नहीं रखता। वेदांत कहता है, परिणाम भी अभी है, अभी है क्योंकि जो तुमने ग़लत करा वो ग़लत बनकर करा। लो मिल गया न परिणाम। क्या मिल गया परिणाम? तुम ग़लत बन गए, यही तो परिणाम है।
तो आपके पास पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है। जो चाहिए आप करिए लेकिन परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। बल्कि वो परिणाम भी नहीं है। परिणाम से तो ऐसा लगता है कि कर्म के बाद परिणाम आता है। वो परिणाम से बहुत पहले की कोई बात है। हाँ, बताने वालों ने, ऋषियों ने इतना ज़रूर बताया है कि ‘देखिए नियति तो आपकी यही है कि आप शांति की ओर बढ़ें, नियति तो यही है कि सत्य की ओर बढ़ें। तो हम आपको सलाह दे सकते हैं कि आप सही चुनाव करें।‘ सलाह दे सकते हैं, अनिवार्य तो नहीं बना सकते।
देखो, किसी को सलाह देना और किसी के लिए कुछ, जैसा आपने कहा, मैंडेटरी कर देना इन दोनों बातों में अंतर है न? तो ऋषि सलाह देते हैं, वो नियम नहीं बनाते। क्योंकि नियम बना भी दें तो नियम चलेगा नहीं। आदमी का अहंकार इतना उच्छृंखल होता है कि वो कौन सा नियम मानता है? इतने धर्मो ने इतने नियम बना दिए, लोग मानते हैं क्या नियमों को? नियम आप बनाते रहो पर आपके भीतर जो बंदर बैठा है वो सारे नियमों को तोड़ देगा। तो ऋषि नियम बनाते ही नहीं। वो कहते हैं, ‘कौन अपना ही अपमान कराए नियम बना कर? नियम हम बनाएँगे ही नहीं! हम नियम बनाएँगे, लोग तोड़ देंगे।‘
तो सलाह देते हैं, वो आपको बस सच्चाई बता देते हैं। फिर कहते हैं ‘देखो आगे अब आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप एक वयस्क हो, आप स्वयं एक सक्षम चेतना हो, अब आप स्वयं चुनाव कर लो। हमने आपको बता दिया कि ये जो सामने चीज़ रखी है इसमें ज़हर है। अब इसको खाना है या नहीं खाना है, ये आपका चुनाव। हाँ, ये हम आपको साफ़-साफ़ बता देंगे कि इसमें ज़हर है और अगर आप और पूछना चाहोगे तो हम ये भी बता देंगे कि ज़हर खाने से क्या-क्या आप पर आफ़ते आती हैं। ये सब भी बता देंगे, जितना चाहोगे बता देंगे, लेकिन खाना है या नहीं खाना है ज़हर, इसका निर्णय तो अंततः आप ही करोगे।‘
प्रश्नकर्ता: भगवान श्री नमन! अभी आपने जैसे चर्चा की कि अर्जुन, कृष्ण और संसार, ये त्रिभुज ही समय है। मैं अपने को देखता हूँ, तो मैं हूँ और मेरे साथ हर समय चुनाव के दो विकल्प हैं। तो मेरे लिए समय है। मेरे लिए समयातीत होने का मतलब है कि विकल्प हट जाएगा तब समय गया या मैं ही चला जाऊँगा तब समय जाएगा?
आचार्य प्रशांत: वो एक ही बात है दोनों। 'मैं' विकल्प के बिना जीता नहीं। जिस 'मैं' को हम जानते हैं न, वो विकल्प की ही ख़ुराक पर ज़िंदा रहता है। उसको विकल्प चाहिए तभी तो निर्विकल्पता, चॉइसलेसनेस उसके अंत के समान होती है। तो ये जो 'मैं' है, ये लगातार एक खोज में रहेगा, तलाश में रहेगा और इसके विकल्प ही इसका अस्तित्व हैं। इससे आप एक बात और समझिएगा। विकल्पों का होना तभी तक है जब एक सही विकल्प और एक ग़लत विकल्प हो। एक ही विकल्प बचे तो फिर कोई विकल्प नहीं बचता।
विकल्प तभी तक कुछ अर्थ रखते हैं जब तक एक सही विकल्प हो, और एक ग़लत विकल्प हो। अगर एक ही विकल्प बचा, माने कि सही वाला, तो फिर हमारे लिए कोई विकल्प नहीं बचा। विकल्प कम-से-कम दो होना चाहिए, द्वैत। और हमने कहा 'मैं' के अस्तित्व के लिए विकल्पों का होना ज़रूरी है। विकल्प होंगे कम-से-कम दो, तो माने ‘मैं’ के अस्तित्व के लिए ग़लत विकल्प का भी होना ज़रूरी है। माने ‘मैं’ अपने बचे रहने के लिए जो ग़लत चीज़ है उसको अपने जीवन से कभी जाने देगा नहीं क्योंकि ग़लत विकल्प भी अगर चला गया तो ‘मैं’ मिट जाएगा। ‘मैं’ अपने बचे रहने के लिए सही विकल्प को भी अपने जीवन से कभी जाने देगा नहीं क्योंकि सही भी अगर चला गया तो ‘मैं’ मिट जाएगा।
तो ‘मैं’ का काम है सही-ग़लत की खिचड़ी पकाते रहना। कुछ ग़लत चाहिए, कुछ सही चाहिए और उनका द्वंद चलता रहे। उसमें ‘मैं’ जीवित रहता है, उसको खुराक मिलती रहती है। जैसे सिनेमा के पर्दे के सामने ‘मैं’ बैठ गया है। उसमें एक नायक है और एक खलनायक है। वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उसमें मज़ा कौन ले रहा है? ‘मैं’। वो बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा है। तो वो दो जो हैं, जब तक सामने पर्दे पर लड़ रहे हैं तब तक ‘मैं’ रसमग्न है। ऐसी कोई आपने आज तक देखी है पिक्चर जिसमें खलनायक ना हो या जिसमें कोई नायक जैसा ना हो?
एक द्वंद चाहिए होता है 'मैं' को जीवित रहने के लिए, तभी तो मज़ा आता है। कभी धूप, कभी छाँव; दोनों को बनाए रखता है। और आप जानते हैं कि पिक्चर चलने के लिए एक अच्छा खलनायक कितना ज़रूरी है। अगर खलनायक एकदम फिसड्डी हो तो पिक्चर पिट जाती है। पिक्चर में मज़ा तभी है जब एक ज़बरदस्त खलनायक को हम बनाए रखें। उस खलनायक में 'मैं' का निवेश है। ‘मैं’ ही उस खलनायक को पोषण देकर, सहारा देकर, बनाए रखता है ताकि पिक्चर मज़ेदार रहे।
प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, अभी आपने एक चीज़ बतायी कि सच रह गया तो भी अहम् चला जाएगा। अगर झूठ रह गया तो भी अहम् चला जाएगा। उस स्थिति में झूठ कैसे रहेगा, झूठ तो है ही नहीं?
आचार्य प्रशांत: अहम् क्या बोल कर रहता है, मैं कौन हूँ?
प्रश्नकर्ता: मैं हूँ।
आचार्य प्रशांत: ‘मैं हूँ’ माने मेरा होना सच है न, तभी तो हूँ। अब सच अगर नहीं रहा तो अहम् क्या बोलेगा बेचारा? ‘मैं नहीं हूँ’, तो मिट गया न फिर। ‘मैं हूँ’ माने होता है, मैं सचमुच हूँ। ‘मैं हूँ’ माने मैं सचमुच हूँ। अब सच तो रहा नहीं तो फिर अहम् को क्या बोलना पड़ेगा? ‘मैं झूठ हूँ, मैं नहीं हूँ’ तो मिट गया न?
